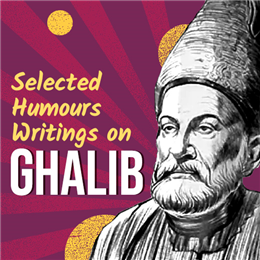ग़ालिब और शरीक-ए-ग़ालिब
इधर कई महीनों से मकान की तलाश में शह्र के बहुत से हिस्सों और गोशों की ख़ाक छानने और कई महल्लों की आब-ओ-हवा को नमूने के तौर पर चखने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो पता चला कि जिस तरह हर गली के लिए कम से कम एक कम तौल पंसारी, एक घर का शेर कुत्ता, एक लड़ाका सास, एक बद-ज़बान बहू, एक नसीहत करने वाले बुज़ुर्ग, एक फ़ज़ीहत पी जाने वाला रिंद और हवाइज-ए-ज़रूरी से फ़ारिग़ होते हुए बहुत से बच्चों का होना लाज़िमी होता है। उसी तरह किसी न किसी भेस में एक माहिर-ए-ग़ालिबयात का होना भी लाज़िमी होता है और बग़ैर उसके गिर्द-ओ-पेश का जुग़राफ़िया कुछ अधूरा रह जाता है।
अच्छा भला एक मकान मिल गया था लेकिन अभी उसमें मिनजुमला अस्बाब-ए-वीरानी मेरा लिपटा हुआ बिस्तर भी ठीक से खुल नहीं पाया था कि महल्ले के माहिर-ए-ग़ालिबयात ने नहीं मालूम कैसे सूँघ लिया कि मैं सुख़न-फ़हम न सही ग़ालिब का तरफ़दार ज़रूर हूँ और मुझे अपनी ग़ालिबाना गिरफ़्त में एक सैद-ए-ज़बूँ की तरह जकड़ लिया।
आते ही आते उन्होंने ग़ालिब के मुताल्लिक़ दो-चार हैरत-अंगेज़ इन्किशाफ़ात के बाद मुझे फाँसने के लिए एक-आध हल्के-फुल्के सवालात कर दिए। अब मेरी हिमाक़त मुलाहिज़ा हो... कि दिल ही दिल में अपने आपको बहुत बड़ा ग़ालिब फ़हम समझता... मैंने उनको नरम चारा समझ कर उन पर दो-चार मुँह मार दिए या यूँ समझ लीजिए उनकी दुम पर पैर रख दिया यानी उनके सामने ग़ालिब को अपने मख़सूस ज़ाविया-ए-निगाह से पेश करने की ‘सई-ए-ला-हासिल’ कर बैठा। मुझे क्या ख़बर थी कि मैं किसी बारूद के खज़ाने के क़रीब दियासलाई जलाने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर क्या था, “आप ग़ालिब को ग़लत समझे हैं” चीख़ कर माहिर-ए-ग़ालिबयात फूट तो पड़े मुझ पर और मेरी मालूमात में इज़ाफ़ा करने के लिए फ़न-ए-ग़ालिबयात की ऐसी-ऐसी तोपों और आतिश-फ़िशानों के दहाने खोल दिए कि मैं सरासीमा, मबहूत और शश्दर हो कर हमेशा के लिए अह्द कर बैठा कि अब आइन्दा किसी अजनबी बुज़ुर्ग के सामने हज़रत-ए-ग़ालिब का नाम अपनी ज़बान-ए-बेलगाम से हरगिज़-हरगिज़ निकलने न दूँगा।
दूसरे ही दिन से माहिर-ए-ग़ालिबयात ने, “आप ग़ालिब को ग़लत समझे हैं।” के उनवान से मेरी बाक़ायदा तालीम शुरू कर दी। सवेरे मैं बिस्तर ही पर होता कि वो ‘लज़्ज़त-ए-ख़्वाब-ए-सहर’ पर धावा बोलते आ पहुँचते और पहले ग़ालिब के कुछ इंतिहाई संगलाख़ अशआर पढ़ कर उनके मअनी मुझसे पूछते, गोया मेरा आमोख़्ता सुनते और फिर क़ब्ल इसके कि मैं एक लफ़्ज़ भी अपनी ज़बान से निकाल पाऊँ, वो “आप ग़ालिब को ग़लत समझे हैं।” फ़रमाकर उनके मअनी और मतालिब ख़ुद बयान करना शुरू कर देते और फिर अपनी ‘गुल-अफ़्शानी-ए-गुफ़तार’ से जिद्दत आफ़रीनी, हुस्न-ए-तख़य्युल, लुत्फ़ बयान, शिकवा-ए-अलफ़ाज़, बलंदी-ए-परवाज़ी, नुदरत-ए-कलाम बल्कि फाँस को बाँस और राई को पहाड़ बनाने के ऐसे-ऐसे ‘गुल कुतरते’ कि मेरे लिए ‘साइक़ा-ओ-शोला-ओ-सीमाब’ का आलम हो जाता और वो ख़ुद इस शे’र की मुजस्सम तफ़सीर बन कर रह जाते,
आगही दाम-ए-शुनीदन जिस क़दर चाहे बिछाए
मुद्दआ अनक़ा है अपने आलम-ए-तक़रीर का
और फिर नौबत यहाँ तक पहुँचती कि मैं दाढ़ी बना रहा हूँ और वो ग़ालिब का फ़लसफ़ा-ए-हुस्न समझा रहे हैं। मैं कंघा कर रहा हूँ और वो आराइश-ए-जमाल से फ़ारिग़ नहीं हनूज़, में मसअला-ए-इर्तिक़ा को परवान चढ़ते देख रहे हैं। मैं कपड़े बदल रहा हूँ और वो हयूला बर्क़-ए-ख़िर्मन का है ख़ून-ए-गर्म दहक़ाँ का, पढ़-पढ़ कर और गाहे-ब-गाहे इन्क़लाब ज़िंदाबाद का नारा लगा लगा कर ग़ालिब को हिन्दोस्तान का सबसे पहला इन्क़लाबी साबित कर रहे हैं।
मैं जूते की डोरियाँ बाँध रहा हूँ और वो ‘बनेंगे और सितारे अब आसमाँ के लिए’ वाले मिसरे से फ़ज़ा-ए-आसमानी पर स्प्टिंग छोड़ रहे हैं। मैं नाश्ता कर रहा हूँ और वो ‘मै है ये मगस की क़ै नहीं है’ दोहरा-दोहरा कर ग़ालिब के इल्म-उल-ग़िज़ा पर कुछ इस अंदाज़ से रौशनी डाल रहे हैं कि मेरे मुँह का निवाला हलक़ में जाने से इनकार कर बैठता है।
मैं दफ़्तर जाने के लिए साईकल निकाल रहा हूँ और वो ग़ालिब का फ़लसफ़-ए-इमरानियात बयान कर रहे हैं। मैं साईकल पर बैठ चुका हूँ और वो शाम को दफ़्तर से मेरी वापसी पर ग़ालिब और ज़ब्त-ए-तौलीद के मौज़ू पर अपने ताज़ा-तरीन इलहामात को मुझ पर नाज़िल करने की धमकियाँ दे रहे हैं।
शाम को ज़ुहूर पज़ीर होते तो ग़ालिब और दूसरे शोअरा का मुवाज़ना शुरू फ़रमा देते और ग़ालिब के मुँह लगने वाले दीगर तमाम शोअरा को क़ाबिल-ए-गर्दनज़दनी क़रार देकर भी जब तसल्ली न होती तो ग़ालिब के मुख़्तलिफ़ शारहीन का पहले सर्कस फिर कुश्ती शुरू करा देते और काफ़ी धर पटख़ के बाद जब हर शारेह काफ़ी पस्त हो चुकता तो ख़ुद भी अखाड़े में कूद पड़ते और फ़र्दन-फ़र्दन हर शारेह को पछाड़ते और फिर हर शे’र के मुताल्लिक़ अपनी एक अनोखी, अछूती और अजूबा-ए-रोज़गार शरह का आग़ाज़ कर देते जिसका अंजाम ग़ालिबन उस वक़्त तक न होता जब तक मैं अपने होश-ओ-हवास की क़ैद-ओ-बंद से निजात पाकर वहाँ न पहुँच जाता जहाँ से ख़ुद मुझको मेरी ख़बर न आती, यानी बिलकुल ही बेसुध हो कर अपने बिस्तर पर गिर न जाता।
मैं अक्सर ख़्वाब में देखता कि हज़रत-ए-ग़ालिब अपना दीवान बग़ल में दबाए बेतहाशा चीख़ते हुए भाग रहे हैं, “बचाओ बचाओ, मुझे मेरे शारेहीन और माहिरीन से बचाओ।” और उनके पीछे शारेहीन, माहिरीन और परस्तारों का एक ग़ोल-ए-बियाबानी उनका तआक़ुब कर रहा है जिसकी क़यादत एक डंडा लिए मेरे महल्ले के माहिर-ए-ग़ालिबयात कर रहे हैं और अपने साथ मुझे भी एक ज़ंजीर में बाँधे घसीट रहे हैं।
कई मर्तबा तकल्लुफ़-बर-तरफ़ करके मिन्नत-समाजत की, हाथ जोड़े, दाढ़ी में हाथ दिया, कान पकड़ कर उठा बैठा और हर्फ़-ए-मतलब यूँ ज़बान पर लाया कि “ऐ माहिर-ए-ग़ालिबयात, आपको आपके हज़रत-ए-ग़ालिब मुबारक, मुझ मग़्लूब को मेरे ही हाल पर छोड़ दीजिए तो आपकी ग़ालिबियत में कौन सा बट्टा लग जाएगा?
“मैं एक गदा-ए-बेनवा हूँ, अहमक़, जाहिल और हैचमदाँ हूँ। मेरे ऐसे ज़र्रा-ए-नाचीज़ को ग़ालिब ऐसे आफ़ताब-ए-आलम-ए-ताब से क्या निसबत? मैं हज़रत-ए-ग़ालिब का सिर्फ़ इस क़दर गुनहगार हूँ कि आलम-ए-तुफ़ूलियत में एक मौलवी साहब ने स्कूल में कोर्स की किताब से उनकी चंद ग़ज़लें ज़बरदस्ती पढ़ा दी थीं। इसके अलावा मुझसे क़सम ले लीजिए जो मैंने कभी उन्हें हाथ भी लगाया हो और हाथ लगाता भी ख़ाक, हाथ आएं तो लगाए न बने।
ग़ालिब को मैं क्या मेरी सात पुश्तें भी नहीं समझ सकतीं। मैं न उन्हें समझा हूँ न समझने की अहलियत रखता हूँ। आप बेकार मेरे होश-ओ-हवास पर चाँद मारी... गोया बंजर ज़मीन पर तुख़्म-रेज़ी और आबयारी करते हैं। नतीजा इसका ये होगा कि मैं पागल हो जाऊँगा और मेरे बीवी और बच्चे आपको और मिर्ज़ा ग़ालिब को कोसते फिरेंगे।”
लेकिन माहिर-ए-ग़ालिबयात भला कब मानने वाले थे? मेरे इज़हार-ए-बेचारगी से उनकी हमादानी में और भी चार चाँद लग जाते और फ़ख़्र-ओ-तमकिनत से उनके गले की रगें पहले से भी ज़्यादा फूलने लगतीं,
“होगा कोई ऐसा भी जो ग़ालिब को न जाने?
दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान और
आप ग़ालिब को ग़लत समझे हैं
ऐ द़रीग़ा वोह रिंद-ए-शाहिद बाज़!”
और ये फ़रमाने के बाद वो ग़ालिब के मुताल्लिक़ अपनी तहक़ीक़ और दरयाफ़्त की गोला-बारी मुझ पर कुछ और तेज़ कर देते। मुझे कभी अगर ऊँघता या हवास बाख़्ता देखते तो चौकन्ना करने के लिए मुझ पर दो-चार इंतिहाई ज़लज़ला-ख़ेज़ सवालात दाग़ देते, “ग़ालिब के नज़रिया-ए-फ़लकिय्यात के मुताल्लिक़ आपका क्या ख़्याल है और इसके मातहत, मह-ए-नख़शब, के साथ 'दस्त-ए-क़ज़ा' ने क्या बरताव किया था?
ग़ालिब ने क़ुदरती मुनाज़िर से जो नफ़सियाती मूशिगाफ़ियाँ की हैं, उससे उनके तहत-उश-शुऊर की किस बुलंदी का पता चलता है?”
“ग़ालिब के समाजी शुऊर में सियासी और इक़तिसादी बग़िययत कब और कैसे पैदा हुई?” वग़ैरा वग़ैरा, मैं भला इन सवालात का जवाब क्या देता? मैं मजबूरन माहिर-ए-ग़ालिबयात की तमानियत-ए-क़ल्ब के लिए आँखें फाड़ कर मुँह खोल देता और उनकी ख़्वाहिश के मुताबिक़ उन्हें अपने हैरत-ज़दा होने का पूरा-पूरा यक़ीन दिला देता, लेकिन दिल ही दिल में सोचता कि अगर मैं अपनी समाजी बलूग़ियत को काम में लाते हुए अपना वज़नी क़लम-दान माहिर-ए-ग़ालिबयात के तहत-उश-शुऊर पर पूरी क़ुव्वत से पटख़ दूँ तो यक़ीनन उन पर फ़लकियात के बहुत से तबक़ रौशन हो जाएँगे।
बस क्या अर्ज़ किया जाये कि किस तरह आजिज़ और परेशान कर रखा था उन माहिर-ए-ग़ालिबयात ने। उन से जान छुड़ाने के लिए बीसियों तरकीबें कीं। महल्ले के बाअसर लोगों का दबाव डलवाया, गुमनाम ख़ुतूत लिखे, एक इंस्पेक्टर पुलिस से उनके ख़िलाफ़ कोई फ़र्ज़ी मुक़द्दमा चलाने की फ़र्माइश की, बीमारी का ढोंग बनाया, बहरे बने (तो इलतिफ़ात) दूना हो गया।
दोस्तों के घर जाकर पनाह ली, घर के दरवाज़े बंद कराए, नौकर को हिदायत की कि “हर चंद कहें कि है नहीं है!” लेकिन अजी तौबा कीजिए। ‘अह्ल-ए-तदबीर की वामांदगियाँ’ माहिर-ए-ग़ालिबयात मुझे न पाते तो घंटों ग़ालिब का कोई शे’र और उससे मुताल्लिक़ एक नई दास्तान-ए-होश-रुबा अपने ऊपर तारी किए हुए मेरे दरवाज़े के सामने गली में टहला करते और जब तक मुझे घर से निकलते गिरफ़्तार करके मुझ पर ये शे’र सादिक़ न कर देते दम ही न लेते।
भागे थे हम बहुत सो उसी की सज़ा है ये
हो कर असीर दाबते हैं राहज़न के पाँव
इन हालात में इसे चाहे मेरी बदज़ाती कहिए चाहे इक़दाम-ए-क़त्ल से गुरेज़ कि जैसे ही मुझे एक दूसरा मकान मिला जो अगरचे मेरे पहले मकान का सिर्फ़ निस्फ़ बेहतर मालूम होता, मैं रस्सियाँ तुड़ा कर भागा। माहिर-ए-ग़ालिबयात से मैंने कह दिया कि मैं शह्र क्या सूबा छोड़ रहा हूँ और वो मुझे आबदीदा हो कर रुख़सत करने आए तो बड़े रिक़्क़त अंगेज़ लहजे में फ़रमाया, “आप ग़ालिब को ग़लत समझे हैं।”
और अगर मैं “शर्म तुमको मगर नहीं आती।” न चीख़ता और ग़लती से ताँगे वाला उसका मुख़ातब अपने आपको समझ कर फ़ौरन ताँगा हाँक न देता तो यक़ीनन माहिर-ए-ग़ालिबयात मुझे एक फ़िलबदीह अलविदाई जुलाब दिए बग़ैर हरगिज़ न मानते।
अपने इन जान लेवा माहिर-ए-ग़ालिबयात से छुटकारा पाकर मुझे जो मुसर्रत-ए-बेपायाँ हासिल हुई उसका इज़हार ग़ालिबन गै़र ज़रूरी है।
मुज़्दा ए मुर्ग़ कि गुलज़ार में सय्याद नहीं
***
मकान तबदील करने के सिलसिले में अपने एक मकान से इंतिहाई बदहवास और सरा सीमगी से बाँधा हुआ सामान जब दूसरे मकान में खोला जाता है तो कहीं से लूट कर लाए हुए माल-ए-ग़नीमत का लुत्फ़ आ जाता है और उसमें से ऐसे-ऐसे हैरत-अंगेज़ इन्किशाफ़ात नमूदार होने लगते हैं कि नातिक़ा सर ब-गरेबाँ हो कर रह जाता है।
मेरा वो आईना जिसको मैंने यक़ीनन किसी बहुत महफ़ूज़ जगह बड़ी एहतियात से छिपा दिया था कि सनद रहे और वक़्त-ए-ज़रूरत पर काम आए, अनथक तलाश और जुस्तजू के बाद भी हाथ नहीं लगता है लेकिन निगार का वो जूता जिसके मुताल्लिक़ यक़ीन-ए-कामिल था कि दो महीने हुए खो चुका है, चुनांचे उसके जोड़ीदार को मैंने चलते-चलाते माहिर-ए-ग़ालिबयात के मकान की तरफ़ उछाल दिया था, एक डिब्बे से बेसाख़्ता निकल पड़ता है।
मैं अपने सामान से कुश्ती लड़-लड़ कर इस क़िस्म के हवादिस से दो-चार था कि दफ़अतन किसी ने बाहर का दरवाज़ा भड़भड़ाना शुरू कर दिया। मुझे उस वक़्त सच पूछिए तो मलक-उल-मौत तक से मिलने की फ़ुर्सत न थी लेकिन तौअन-ओ-करहन लाहौल पढ़ता हुआ लपका और दरवाज़ा खोल दिया।
दाढ़ी चढ़ाए और सिर्फ़ बनियाइन और तहमद पहने एक बुज़ुर्ग नमूदार हुए और बड़ी बे-तकल्लुफ़ी से “सलाम अलैकुम” कहते हुए बैठके में दाख़िल हो कर एक कुर्सी घसीटी और उस पर उकड़ूँ बैठ गए और कुछ झूम कर ये शे’र पढ़ा,
“हम पुकारें और खुले, यूँ कौन जाये?
यार का दरवाज़ा पाएं गर खुला”
“मुझे मजबूरन “वाअलैकुम अस्सलाम” कह कर एक मोंढे पर पनाह लेना पड़ी।
“इस मकान के नए किराएदार आप ही हैं? कोई वीरानी सी वीरानी है? मतलब ये कि, आवे न क्यों पसंद कि ठंडा मकान है।”
मिर्ज़ा ग़ालिब का ताबड़तोड़ कलाम सुनने के बाद और ग़ुस्से के ख़ौफ़ से मेरे कान ख़ुद-ब-ख़ुद हिलने लगे और बड़ी मुश्किल से मेरे मुँह से फ़क़त एक “जी” निकल सकी।
“अभी-अभी मिर्ज़ा कब्बन साहिब से मालूम हुआ कि यहाँ तशरीफ़ लाने से क़ब्ल आप दिल्ली में रहते थे।
क्यों न दिल्ली में हर इक नाचीज़ नवाबी करे?”
“जी हाँ दो तीन माह दिल्ली भी रहा हूँ। क्या मेरे ख़िलाफ़ खु़फ़िया पुलिस की कोई तहक़ीक़ात आपके सपुर्द हुई है?”
मुस्कराकर चीख़ उठे, “है है ख़ुदा-ना-ख़्वास्ता वो और दुश्मनी
ऐ शौक़-ए-मुनफ़इल ये तुझे क्या ख़्याल है”
मैंने हिम्मत करके दबी ज़बान से अर्ज़ किया, “आपने अभी तक मुझे ख़ुद अपने आपसे मुतआरिफ़ होने का शरफ़ नहीं बख़्शा।”
अपने सर के बाल नोचते हुए बोले, “पूछते हैं वो कि ग़ालिब कौन है। कोई बतलाओ कि हम बतलाएँ क्या?”
अब मेरी बदहवासी मुकम्मल हो चुकी थी, “जी, आप? हज़रत-ए-ग़ालिब।”
“जी हाँ हज़रत-ए-ग़ालिब।
हमपेशा-ओ-हममशरब-ओ-हमराज़ है मेरा
मैं इस वक़्त सिर्फ़ ये पूछने हाज़िर हुआ था कि आप दिल्ली में रहे हैं तो शहनशाह-ए-अक़लीम-ए-सुख़न, हज़रत-ए-ग़ालिब से तो ज़रूर ही वाक़िफ़ होंगे।”
मुझे झुर-झुरी सी महसूस होने लगी और मैंने बड़ी बे-एतिनाई से जवाब दिया, “जी हाँ, सुना है कि इस नाम के एक बुज़ुर्ग का मज़ार दिल्ली ही में है।” अपना सर पीटते हुए बोले, “माफ़ कीजिएगा आपने भी बेरहमी की हद कर दी, सुना है कि इस नाम के एक बुज़ुर्ग का मज़ार दिल्ली ही में है।
जलवा-गुल के सिवा गर्द अपने मदफ़न में नहीं। अजी आपको ये भी तौफ़ीक़ नहीं हुई कि आप उस बारगाह-ए-फ़लक मंज़िलत पर। रुत्बे में मह्र-ओ-माह से कमतर नहीं हूँ मैं। सर-ए-अक़ीदत ख़म करके कम से कम शरफ़-ए-क़दम बोसी तो हासिल कर ही लेते। वही मिस्ल बारह बरस दिल्ली में रहे और, सर जाये यार है न रहें पर कहे बग़ैर। भाड़ ही झोंकते रहे?”
मैंने भी कुछ इस जलबलाहट से जवाब दिया जैसे अगर मेरा बस चलता तो ग़ालिब को उनकी ख़्वाहिश के मुताबिक़ ग़र्क़-ए-दरिया हो जाने देता और कुछ नहीं तो दिल्ली में तो उनका मज़ार हरगिज़ बनने न देता। “मैं मज़ार पर हाज़िर भी होता तो मरहूम तो क़ब्र के अंदर थे न कि ऊपर, मैं शरफ़-ए-क़दम-बोसी कैसे हासिल कर पाता?”
कलेजा पकड़ कर बोले, “हे हे... रखता है ज़िद से खींच के बाहर लगन के पाँव। अजी आपको क्या ख़बर... पस अज़ मर्दन भी दीवाना ज़यारत गाह-ए-तिफ़्लाँ है। शरार-ए-संग ने तुर्बत पे मेरी गुलफ़िशानी की।”
मैं ख़ामोश रहा, चंद लम्हों की ख़ामोशी के बाद फिर गोया हुए, “कम से कम अज़ राह़-ए-ताज़ियत आपको मरहूम के बीवी-बच्चों के पास तो चले ही जाना चाहिए था। बच्चों का भी देखा न तमाशा कोई दिन और।”
“अब किसी रोज़ आपको साथ लेकर चला जाऊँगा”
मेरे जवाब को सुना अन-सुना करके अचानक बड़बड़ाए और मेरी किताबों के गट्ठर पर जो अभी मेज़ पर बड़ी बेतर्तीबी से रखा हुआ था झपटे, और सबसे ऊपर की किताब जो इत्तिफ़ाक़ से दीवान-ए-ग़ालिब थी उठाकर “जोश-ए-बहार-ए-जलवा” बनते हुए बोले, “ये सहीफ़ा आपको कहाँ से दस्तयाब हुआ? यादगार-ए-नाला इक दीवान-ए-बेशीराज़ा था। मुद्दत के बाद आज एक मुसल्लम दीवान-ए-ग़ालिब हाथ आया है जो किसी तरह भी मुझे मुर्ग़-ए-मुसल्लम से कम अज़ीज़ नहीं। कहते हैं कि ग़ालिब का है अंदाज़ बयान और।”
“बाज़ार से।”
“बाज़ार से? और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया? क्या बाज़ार में इस क़िस्म का भी कलाम बिकता है? ख़ुदा झूट न बुलवाए तो सतरह अठारह साल हुए मेरे पास भी एक मुसल्लम दीवान-ए-ग़ालिब था जो मेरे एक रिश्ते के नाना मेरे घर पर भूल गए थे। कभी फ़ितराक में तेरे कोई नख़चीर भी था, लेकिन ख़ुश क़िस्मती से एक रोज़ बरखु़र्दार जुम्मन की वालिदा जो आग जलाने बैठीं कि लगाए न लगे और बुझाए न बने, तो उस सहीफ़ा-ए-ज़र्रीं को कुछ इस तरह फाड़ा कि बस। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। यानी दीवान का क़रीब-क़रीब हर मिसरा-ए-ऊला अपने मिसरा-ए-सानी से जुदा हो गया। वो तो कहिए कि बरवक़्त मेरी नज़र पड़ गई वर्ना, आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया, का मज़मून दरपेश आ जाता। क्यों साहब... ये लफ़्ज़ ख़ुश क़िस्मती पर आप चौंके क्यों? जी हाँ, इसमें कुछ शाइबा-ए-ख़ूबी-ए-तक़दीर भी था।”
मैंने अपना पेट पकड़ते और मुँह बनाते हुए अर्ज़ किया, “इस वक़्त पेट में कुछ दर्द हो रहा है। अगर ये गुफ़्तगु आप किसी दूसरे वक़्त के लिए मुल्तवी कर दें...” नादिर शाही हुक्म दिया, “ए मर्गे नागहाँ तुझे क्या इंतज़ार है। मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ।
जी हाँ तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब जो वालिदा मुहतरमा मतलब ये कि जुम्मन की वालिदा मुहतरमा उन औराक़-ए-परीशाँ को जो किसी आशिक़ का गिरेबां हो चुके थे, जोड़ने बैठीं तो उनको कुछ ऐसा जोड़ दिया कि फ़न-ए-ग़ालिबयात में एक नए दौर का आग़ाज़ बल्कि इज़ाफ़ा हो गया और जिस पर नाचीज़ अपनी उम्र-ए-अज़ीज़ के बारह साल सर्फ़ कर चुका है और अब बहुत जल्द दीवान-ए-ग़ालिब हस्ब-ए-तर्तीब-ए-बालिग़ मंज़र-ए-आम पर जल्वा-अफ़रोज़ हो कर मुश्ताक़ान-ए-ग़ालिब और क़दर शनासाँ बालिग़ के लिए जन्नत-ए-निगाह और फ़िरदौस-ए-गोश बनने वाला है।
महज़ मिसरों की थोड़ी सी उलट-पलट से कलाम की लताफ़त, ज़राफ़त और सदाक़त नहीं मालूम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और यक़ीनन अब मिर्ज़ा ग़ालिब को ये फ़रमाने का... ‘न सही गर मेरे अशआर में मअनी न सही’ कोई हक़ बाक़ी नहीं रहता। काश कि वो ख़ुद उसको देखते तो अश-अश करके कफ-ए-अफ़सोस मलते कि हाय ख़ुद मुझे ये क्यों न सूझी और बिला इमदाद-ए-बालिग़ मैंने ये पहेली क्यों न बूझी।”
सिलसिला-ए-कलाम-ए-यक-तरफ़ा को जारी रखते हुए फ़रमाया, “नमूने के तौर पर सिर्फ़ चंद अशआर मुलाहिज़ा हों... देखिए किस तरह दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है?
एक रोज़ मजनूँ स्कूल से रोता हुआ लौटा तो उसने अपने गार्जियन मिर्ज़ा ग़ालिब से शिकायत की कि उसको मास्टर ने बेक़ुसूर मारा है। मिर्ज़ा ग़ालिब का अफ़्रिसयाबी ख़ून जोश में आ गया और वो मास्टर के ‘पुर्जे़ उड़ाने’ स्कूल पहुँचे तो ऐन मौक़ा-ए-वारदात पर शायर मिल गया और उन्हें समझाता है कि मास्टर ने बरख़ुर्दार मजनूँ को जो सज़ा दी, वो बिल्कुल हक़-ब-जानिब थी क्योंकि ये साहबज़ादे कोयले से स्कूल की दीवार ख़राब करते हुए पकड़े गए थे....
‘‘न लड़ नासेह से ग़ालिब क्या हुआ गर उसने शिद्दत की
कि मजनूँ लाम अलिफ़ लिखता था दीवार-ए-दबिस्ताँ पर’’
ज़रा ख़ुदा-लगती कहिएगा कि अब शे’र की अख़लाक़ी हैसियत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? आशिक़ की इज़्ज़त-ए-नफ़्स के मुताल्लिक़ ग़ालिब ने बहुत से अशआर कहे हैं लेकिन ज़रा इस शे’र के तेवर मुलाहिज़ा फ़रमाईए। एक दफ़्तर में क्लर्क हो जाने के बाद आशिक़ के लहजे में कैसी ख़ुद-एतिमादी आ जाती है।
दाइम पड़ा हुआ तिरे दर पर नहीं हूँ मैं
वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं
मुलाहिज़ा हो कि क़र्ज़ की शराब पी कर मिर्ज़ा ग़ालिब साक़ी की धर पटख़ से बचने के लिए उसको किस तरह का पुचकारा देते हैं...
क़र्ज़ की पीते थे मै और कहते थे कि हाँ
धौल-धप्पा उस सरापा-नाज़ का शेवा नहीं
कौन कहता है कि मिर्ज़ा साहिब ना-आक़िबत-अँदेश थे। देखिए किस तरह अपने छोटे भाई असद को मश्वरा लेने के बहाने नसीहत करते हैं...
ले तो लूँ सोते में उसके पाँव का बोसा मगर
फ़ायदा क्या सोच आख़िर तू भी दाना है असद
और ग़ालिबन ये आपके मज़ाक़ का शे’र हो। ज़रा माशूक़ की जल्द-बाज़ी तो मुलाहिज़ा हो...
ज़ुल्फ़ से बढ़कर निक़ाब उस शोख़ के मुँह पर खुला
जितने अर्से में मिरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला
और माशूक़ की तेज़ रफ़्तारी तो ग़ालिबन इससे बेहतर कभी बयान ही नहीं की जा सकी...
थान से वो ग़ैरत-ए-सर सर खुला
किस ने खोला, कब खुला, क्योंकर खुला
और ग़ालिबन ये शे’र तो दाद से मुस्तसना है। साक़ी इससे बढ़कर मिर्ज़ा साहिब पर और एहसान ही क्या कर सकता था।
मैं और हज़-ए-वस्ल ख़ुदा-साज़ बात है
साक़ी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में
और फिर माशूक़ के बुढ़ापे की, जब वो कई बच्चों की माँ बन कर अपने शौहर यानी ग़ालिब के पुराने रक़ीब के साथ ‘सब ख़ैरीयत है’ क़िस्म की ज़िंदगी बसर कर रही है, क्या ख़ूब तस्वीर खींच कर रख दी है।
यक़ीन है हमको भी लेकिन अब इसमें दम क्या है
रक़ीब पर है अगर लुत्फ़, तो सितम क्या है
देखिए, ‘ज़ुल्म है गर न दो सुख़न की दाद…’ ये सब मिसरे हज़रत-ए-ग़ालिब ही के हैं और मैंने उनमें किसी क़िस्म की कोई तहरीफ़ नहीं की है सिर्फ़ ज़रा चाबुकदस्ती से उनकी तर्तीब में थोड़ी सी उलट-पलट कर दी है।”
मैं नक़्श-ए-हैरत बना ये सब सुन रहा था लेकिन नहीं मालूम मेरे हाथों में एक ख़ास क़िस्म की तशनुज्जी कैफ़ियत क्यों पैदा हो रही थी। बालिग़ साहिब की रवानी-ए-तबा कुछ और तेज़ हो चली।
“देखिए मिर्ज़ा साहब माशूक़ को बहला फुसला कर उसे छुप कर मिलने के कैसे-कैसे मुक़ामात बताते हैं... गुर्ग-ए-बाराँ दीदा थे कि बातें...
मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो
मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई ख़ानक़ाह हो
और जिगर थाम कर ज़रा ये शे’र तो मुलाहिज़ा फ़रमाईए...
दिल साहिब-ए-औलाद से इंसाफ़-तलब है। आपने बहुत से माशूक़ देखे होंगे लेकिन ऐसा आशिक़ मार माशूक़ भी कभी आपके पल्ले पड़ा है...
उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक
जी में कहते हैं कि “मुफ़्त आए तो माल अच्छा है”
और ये शे’र तो हासिल-ए-दीवान हो कर रह गया है। पहले शे’र सुन लीजिए फिर मैं उसके तफ़सीलात ज़रा तफ़सील से बयान करना चाहता हूँ।
ग़ैर से रात क्या बनी ये जो कहा तो देखिए
मौज-ए-मुहीत-ए-आब में मारे हैं दस्त-ओ-पा कि यूँ
***
इसके बाद क्या हुआ? तफ़सीलात बर-तरफ़। एक तहमद और एक बनियाइन की कुछ धज्जियाँ मेरे हिस्से में आईं और मेरा रफ़ीक़ दीवान-ए-ग़ालिब मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। फ़िलहाल मैं अस्पताल में हूँ और बीवी-बच्चे होटल में। अलॉटमेंट ऑफ़िसर को दरख़्वास्त दे रखी है कि मुझे कोई ऐसा मकान अलॉट कीजिए जिसमें चाहे रौशनदान, नाबदान बल्कि छतें और दीवारें तक न हों लेकिन उससे एक मील के क़तर में कोई माहिर-ए-ग़ालिबयात न पाया जाता हो। अभी तक एक भी ऐसा कोई मकान मिल नहीं पाया है।
वाज़ेह रहे कि ग़ालिब अब भी मेरा महबूब तरीन शायर है बल्कि माहिरीन और शारेहीन के हाथों उसकी दुर्गत बनते देखकर वो मुझे पहले से भी कहीं ज़्यादा अज़ीज़ हो गया है। ब-हम्द-ओ-लिल्लाह मैंने दीवान-ए-ग़ालिब का एक दूसरा नुस्ख़ा ख़रीद लिया है और ग़ुस्ल-ख़ाने में जब भी पानी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होता है तो मैं उसके और सिर्फ़ उसके अशआर गुनगुनाता हूँ और अक्सर उसकी मज़लूमियत का तसव्वुर करके ये मिसरा भी पढ़ लेता हूँ...
शायर तो वो अच्छा है प बदनाम बहुत है
स्रोत:

Ghaalib Se Mazarat Ke Sath (Pg. 86)
- लेखक: अहमद जमाल पाशा
-
- प्रकाशक: नसीम बुक डिपो, लखनऊ
- प्रकाशन वर्ष: 1964
यह पाठ नीचे दिए गये संग्रह में भी शामिल है
COMMENT
COMMENTS
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.