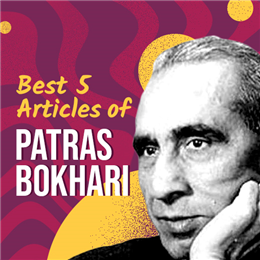मैं एक मियाँ हूँ
मैं एक मियाँ हूँ। मुती-व-फ़रमां-बरदार। अपनी बीवी रौशन आरा को अपनी ज़िंदगी की हर एक बात से आगाह रखना उसूल-ए-ज़िंदगी समझता हूँ और हमेशा से इस पर कार-बन्द रहा हूँ। ख़ुदा मेरा अंजाम बख़ैर करे।
चुनांचे मेरी अहलिया मेरे दोस्तों की तमाम आदात-व-ख़साएल से वाक़िफ़ हैं जिसका नतीजा ये है कि मेरे दोस्त जितने मुझ को अज़ीज़ हैं उतने ही रौशन आरा को बुरे लगते हैं। मेरे अहबाब की जिन अदाओं ने मुझे मस्हूर कर रखा है उन्हें मेरी अहलिया एक शरीफ़ इंसान के लिए बाइस-ए-ज़िल्लत समझती है।
आप कहीं ये न समझ लें कि ख़ुदा-नख़्वास्ता वो कोई ऐसे आदमी हैं जिनका ज़िक्र किसी मुअज़्ज़ मज्मे में ना किया जा सके। कुछ अपने हुनर के तुफ़ैल और कुछ ख़ाकसार की सोहबत की बदौलत सब के सब ही सफेदपोश हैं। लेकिन इस बात को क्या करूँ कि उनकी दोस्ती मेरे घर के अमन में इस क़दर ख़लल अंदाज़ होती है कि कुछ कह नहीं सकता।
मसलन मिर्ज़ा साहब ही को लीजिए। अच्छे ख़ासे और भले आदमी हैं। गो महक्मा-ए-जंगलात में एक मा’क़ूल ओ’हदे पर मुमताज़ हैं लेकिन शक्ल-व-सूरत ऐसी पाकीज़ा पाई है कि इमाम-ए-मस्जिद मा’लूम होते हैं। जुवा वह नहीं खेलते, गिल्ली-डंडे का उनको शौक़ नहीं, जेब कतरते हुए कभी वो नहीं पकड़े गये। अलबत्ता कबूतर पाल रखे हैं। उन्हीं से जी बहलाते हैं। हमारी अहलिया की ये कैफ़ियत है कि मुहल्ले का कोई बदमाश जुए में क़ैद हो जाये तो उसकी माँ के पास मातम-पुर्सी तक को चली जाती हैं। गिल्ली-डंडे में किसी की आँख फूट जाये तो मरहम पट्टी करती रहती हैं। कोई जेब-कतरा पकड़ा जाये तो घंटों आँसू बहाती रहती हैं लेकिन वो बुज़ुर्ग जिनको दुनिया भर की ज़बान मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा साहब कहते थकती नहीं, हमारे घर में मूऐ कबूतर -बाज़ के नाम से याद किए जाते हैं। कभी भूले से भी में आसमान की तरफ़ नज़र उठा कर किसी चील, कव्वे, गिद्ध, शुक्रे को देखने लग जाऊं तो रौशन आरा को फ़ौरन ख़्याल हो जाता है कि बस अब ये भी कबूतर-बाज़ बनने लगा।
इसके बाद मिर्ज़ा साहब की शान में एक क़सीदा शुरू होजाता है। बीच में मेरी जानिब गुरेज़। कभी लंबी बहर में कभी छोटी बहर में।
एक दिन जब ये वाक़या पेश आया तो मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस मिर्ज़ा कम्बख़्त को कभी पास न फटकने दूँगा। आख़िर घर सब से मुक़द्दम है। मियाँ-बीवी के बाहमी इख़लास के मुक़ाबले में दोस्तों की ख़ुशनूदी क्या चीज़ है? चुनांचे हम ग़ुस्से में भरे हुए मिर्ज़ा साहब के घर गये। दरवाज़ा खटखटाया। कहने लगे, “अंदर आ जाओ।” हम ने कहा, “नहीं आते। तुम बाहर आओ।” ख़ैर अंदर गया। बदन पर तेल मल कर एक कबूतर की चोंच मुँह में लिए धूप में बैठे थे। कहने लगे, “बैठ जाओ।” हम ने कहा, “बैठेंगे नहीं।” आख़िर बैठ गये। मा’लूम होता है हमारे तेवर कुछ बिगड़े हुए थे। मिर्ज़ा बोले, “क्यूँ भई! ख़ैर बाशद!” मैंने कहा’ “कुछ नहीं।” कहने लगे, “इस वक़्त कैसे आना हुआ?”
अब मेरे दिल में फ़िक़रे खौलने शुरू हुए। पहले इरादा किया कि एक दम ही सब कुछ कह डालो और चल दो। फिर सोचा कि मज़ाक़ समझेगा, इसलिए किसी ढंग से बात शुरू करो लेकिन समझ में न आया कि पहले क्या कहें। आख़िर हम ने कहा,
“मिर्ज़ा! भई कबूतर बहुत महंगे होते हैं।”
ये सुनते ही मिर्ज़ा साहिब ने चीन से लेकर अमरीका तक के तमाम कबूतरों को एक-एक कर के गिनवाना शुरू किया। इसके बाद दाने की महंगाई के मुता’ल्लिक़ गुल-अफ़्शानी करते रहे और फिर महज़ महंगाई पर तक़रीर करने लगे। उस दिन तो हम यूँ ही चले आये लेकिन अभी खट-पट का इरादा दिल में बाक़ी था। ख़ुदा का करना क्या हुआ कि शाम को घर में हमारी सुलह हो गई। हम ने कहा, “चलो अब मिर्ज़ा के साथ बिगाड़ने से क्या हासिल? चुनांचे दूसरे दिन मिर्ज़ा से भी सुलह-सफ़ाई हो गई।
लेकिन मेरी ज़िंदगी तल्ख़ करने के लिए एक न एक दोस्त हमेशा कार आमद होता है। ऐसा मा’लूम होता है कि फ़ितरत ने मेरी तबीयत में क़ुबूलियत और सलाहियत कूट-कूट कर भर दी है क्योंकि हमारी अहलिया को हममें हर वक़्त किसी न किसी दोस्त की आदात की झलक नज़र आती रहती है, यहां तक कि मेरी अपनी ज़ाती शख़्सी सीरत बिल्कुल ही ना-पैद हो चुकी है।
शादी से पहले हम कभी-कभी दस बजे उठा करते थे वर्ना ग्यारह बजे। अब कितने बजे उठते हैं? इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिन के घर नाशता ज़बरदस्ती सुबह के सात बजे करा दिया जाता है और अगर हम कभी बश्री कमज़ोरी के तक़ाज़े से मुर्गों की तरह तड़के उठने में कोताही करें तो फ़ौरन कह दिया जाता है कि ये इस निखट्टू नसीम की सोहबत का नतीजा है। एक दिन सुबह-सुबह हम नहा रहे थे। सर्दी का मौसम, हाथ पांव काँप रहे थे। साबुन सर पर मलते थे तो नाक में घुसता था कि इतने में हमने ख़ुदा जाने किस पुर-असरार जज़्बे के मा-तहत ग़ुस्ल-ख़ाने में अलापना शुरू किया और फिर गाने लगे कि “तोरी छल-बल है न्यारी...” इसको हमारी इंतिहाई बद-मज़ाक़ी समझा गया और इस बद-मज़ाक़ी का अस्ल मम्बा हमारे दोस्त पण्डित जी को ठहराया गया।
लेकिन हाल ही में मुझ पर एक ऐसा सानिहा गुज़रा है कि मैंने तमाम दोस्तों को तर्क कर देने की क़सम खा ली है।
तीन चार दिन का ज़िक्र है कि सुबह के वक़्त रौशन आरा ने मुझ से मायके जाने की इजाज़त मांगी। जब से हमारी शादी हुई है रौशन आरा सिर्फ़ दो दफ़ा मायके गयी है और फिर उसने कुछ इस सादगी और इज्ज़ से कहा कि मैं इनकार न कर सका। कहने लगी, “तो फिर मैं डेढ़ बजे की गाड़ी से चली जाऊं।” मैंने कहा, “और क्या?”
वह झट तैयारी में मशग़ूल हो गयी और मेरे दिमाग़ में आज़ादी के ख़्यालात ने चक्कर लगाने शुरू किए। या’नी अब बेशक दोस्त आयें, बेशक उधम मचाएं, मैं बेशक गाउँ, बेशक जब चाहूँ उठूँ। बेशक थिएटर जाऊँ। मैंने कहा,
“रौशन आरा जल्दी करो। नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी।”
साथ स्टेशन पर गया। जब गाड़ी में सवार करा चुका तो कहने लगी, “ख़त ज़रूर लिखते रहिए!” मैंने कहा, “हर रोज़। और तुम भी!”
“खाना वक़्त पे खा लिया कीजिए और हाँ धुली हुई जुराबें और रूमाल अलमारी के निचले ख़ाने में पड़े हैं।”
इसके बाद हम दोनों ख़ामोश हो गये और एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे। उस की आँखों में आँसू भर आये। मेरा दिल भी बेताब होने लगा और जब गाड़ी रवाना हुई तो मैं देर तक मबहूत प्लेट-फार्म पर खड़ा रहा।
आख़िर आहिस्ता-आहिस्ता क़दम उठाता हुआ किताबों की दुकान तक आया और रिसालों के वरक़ पलट-पलट कर तस्वीरें देखता रहा। एक अख़बार ख़रीदा। तह करके जेब में डाला और आदत के मुताबिक़ घर का इरादा कर लिया।
फिर ख़्याल आया कि अब घर जाना ज़रूरी नहीं। अब जहां चाहूँ जाऊँ,चाहूँ तो घंटों स्टेशन पर ही टहलता रहूँ। दिल चाहता था क़ुला-बाज़ियां खाऊं।
कहते हैं, जब अफ़्रीक़ा के वहशियों को किसी तहज़ीब याफ़्ता मुल्क में कुछ अ’र्से के लिए रखा जाता है तो वह वहां की शान-व-शौकत से बहुत मुतास्सिर होते हैं। लेकिन जब वापस जंगलों में पहुंचते हैं तो ख़ुशी के मारे चीख़ें मारते हैं। कुछ ऐसी ही कैफ़ियत मेरे दिल की भी हो रही थी। भागता हुआ स्टेशन से आज़ादाना बाहर निकला। आज़ादी के लहजे में तांगे वाले को बुलाया और कूद कर तांगे में सवार हो गया सिगरेट सुलगा लिया, टांगें सीट पर फैला दीं और क्लब को रवाना हो गया।
रस्ते में एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। ताँगा मोड़ कर घर की तरफ़ पल्टा। बाहर ही से नौकर को आवाज़ दी।
“अमजद!”
“हुज़ूर!”
“देखो, हज्जाम को जा कर कह दो कि कल ग्यारह बजे आय।”
“बहुत अच्छा।”
“ग्यारह बजे। सुन लिया ना? कहीं रोज़ की तरह फिर छः बजे वारिद न हो जाये।”
“बहुत अच्छा हुज़ूर।”
“और अगर ग्यारह बजे से पहले आये, तो धक्के दे कर बाहर निकाल दो।”
यहां से क्लब पहुंचे। आज तक कभी दिन के दो बजे क्लब ना गया था। अंदर दाख़िल हुआ तो सुनसान, आदमी का नाम-व-निशान तक नहीं। सब कमरे देख डाले। बिलियर्ड का कमरा ख़ाली, शतरंज का कमरा ख़ाली। ताश का कमरा ख़ाली। सिर्फ़ खाने के कमरे में एक मुलाज़िम छुरियां तेज़ कर रहा था। उससे पूछा “क्यूँ बे आज कोई नहीं आया?”
कहने लगा, “हुज़ूर! आप तो जानते ही हैं। इस वक़्त भला कौन आता है?”
बहुत मायूस हुआ। बाहर निकल कर सोचने लगा कि अब क्या करूं? और कुछ ना सूझा तो वहां से मिर्ज़ा साहब के घर पहुंचा। मालूम हुआ अभी दफ़्तर से वापस नहीं आये। दफ़्तर पहुंचा, देख कर बहुत हैरान हुये। मैंने सब हाल बयान किया। कहने लगे, “तुम बाहर के कमरे में ठहरो, थोड़ा सा काम रह गया है। बस अभी भुग्ता के तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाम का प्रोग्राम क्या है?”
मैंने कहा, “थिएटर!”
कहने लगे, बस बहुत ठीक है, तुम बाहर बैठो। मैं अभी आया।”
बाहर के कमरे में एक छोटी सी कुर्सी पड़ी थी। उस पर बैठ कर इंतज़ार करने लगा और जेब से अख़बार निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू से आख़िर तक सब पढ़ डाला और अभी चार बजने में एक घंटा बाक़ी था। फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। सब इश्तिहार पढ़ डाले और फिर सब इश्तिहारों को दुबारा पढ़ डाला।
आख़िर कार अख़बार फेंक कर बगै़र किसी तकल्लुफ़ या लिहाज़ के जमाइयाँ लेने लगा। जमाई पे जमाई, जमाई पे जमाई। हत्ता कि जबड़ों में दर्द होने लगा। उसके बाद टांगें हिलाना शुरू किया लेकिन इस से भी थक गया। फिर मेज़ पर तबले की गतैं बजाता रहा। बहुत तंग आ गया तो दरवाज़ा खोल कर मिर्ज़ा से कहा, “अबे यार! अब चलता भी है कि मुझे इंतज़ार ही में मार डालेगा, मर्दूद कहीं का। सारा दिन मेरा ज़ाया कर दिया।”
वहां से उठ कर मिर्ज़ा के घर गये। शाम बड़े लुत्फ़ में कटी। खाना क्लब में खाया और वहां से दोस्तों को साथ लिए थिएटर गये। रात के ढाई बजे घर लौटे। तकिए पर सर रखा ही था कि नींद ने बे-होश कर दिया।
सुबह आँख खुली तो कमरे में धूप लहरें मार रही थी। घड़ी को देखा तो पौने ग्यारा बजे थे। हाथ बढ़ा कर मेज़ पर से एक सिगरेट उठाया और सुलगा कर तश्तरी में रख दिया और फिर ऊँघने लगा।
ग्यारह बजे अमजद कमरे में दाख़िल हुआ कहने लगा, “हुज़ूर! हज्जाम आया है।”
हम ने कहा, “यहीं बुला लाओ।” ये ऐश मुद्दत के बाद नसीब हुआ कि बिस्तर में लेटे लेटे हजामत बनवा लें। इत्मिनान से उठे और नहा धो कर बाहर जाने के लिए तैयार हुए लेकिन तबीयत में वो शगुफ़्तगी न थी जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे। चलते वक़्त अलमारी से रुमाल निकाला तो ख़ुदा जाने क्या ख़्याल दिल में आया। वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सौदाईयों की तरह उस रूमाल को तकता रहा। अलमारी का एक और ख़ाना खोला तो सुरमई रंग का एक रेशमी दुपट्टा नज़र आया। बाहर निकाला। हल्की हल्की अतर की ख़ुशबू आरही थी। बहुत देर तक उस पर हाथ फेरता रहा। दिल भर आया। घर सूना मालूम होने लगा। बहुतेरा अपने आप को संभाला लेकिन आँसू टपक ही पड़े। आँसूओं का गिरना था कि बेताब हो गया और सच-मुच रोने लगा। सब जोड़े बारी-बारी निकाल कर देखे लेकिन न मा’लूम क्या-क्या याद आया कि और भी बेक़रार होता गया।
आख़िर न रहा गया, बाहर निकला और सीधा तार-घर पहुंचा। वहां से तार दिया कि, “मैं बहुत उदास हूँ तुम फ़ौरन आ जाओ!”
तार देने के बाद दिल को इत्मिनान हुआ। यक़ीन था कि रौशन आरा अब जिस क़दर जल्द हो सकेगा आ जाएगी। इससे कुछ ढारस बंध गई और दिल पर से जैसे एक बोझ हट गया।
दूसरे दिन दोपहर को मिर्ज़ा के मकान पर ताश का मार्का गर्म होना था। वहां पहुंचे तो मा’लूम हुआ कि मिर्ज़ा के वालिद से कुछ लोग मिलने आये हैं। इसलिए तजवीज़ ये ठहरी कि यहां से किसी और जगह सरक चलो। हमारा मकान तो ख़ाली था ही। सब यार लोग वहीं जमा हुए। अमजद से कह दिया गया कि हुक्के में अगर ज़रा भी ख़लल वाक़े हुआ तो तुम्हारी ख़ैर नहीं और पान इस तरह से मुतवातिर पहुंचते रहें कि बस तांता लग जाये।
अब उसके बाद के वाक़ियात को कुछ मर्द ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। शुरू शुरू में तो ताश बाक़ायदा और बाज़ाब्ता होता रहा। जो खेल भी खेला गया बहुत माक़ूल तरीक़े से, क़वायद-व-ज़वाबित के मुताबिक़ और मतानत-व-संजीदगी के साथ लेकिन एक दो घंटे के बाद कुछ ख़ुश-तबई शुरू हुई। यार लोगों ने एक दूसरे के पत्ते देखने शुरू कर दिये। ये हालत थी कि आँख बची नहीं और एक आध काम का पत्ता उड़ा नहीं और साथ ही क़हक़हे पर क़हक़हे उड़ने लगे। तीन घंटे के बाद ये हालत थी कि कोई घुटना हिला-हिला कर गा रहा है, कोई फ़र्श पर बाज़ू टेके सीटी बजा रहा है, कोई थिएटर का एक आध मज़ाक़िया फ़िकरा लाखों दफ़ा दोहरा रहा है लेकिन ताश बराबर हो रहा है। थोड़ी देर के बाद धौल-धप्पा शुरू हो गया। इन ख़ुश-फ़े’लियों के दौरान में एक मसख़रे ने एक ऐसा खेल तजवीज़ कर दिया जिसके आख़िर में एक आदमी बादशाह बन जाता है, दूसरा वज़ीर, तीसरा कोतवाल और जो सब से हार जाये वह चोर। सब ने कहा, “वाह! वा क्या बात कही है।” एक बोला, “फिर आज जो चोर बना, उसकी शामत आ जायेगी।” दूसरे ने कहा, “और नहीं तो क्या। भला कोई ऐसा वैसा खेल है। सल़्तनतों के मामले हैं, सल़्तनतों के!”
खेल शुरू हुआ। बद-क़िस्मती से हम चोर बन गये। तरह तरह की सज़ाएं तजवीज़ होने लगीं। कोई कहे, “नंगे पांव भागता हुआ जाये और हलवाई की दुकान से मिठाई ख़रीद के लाय।” कोई कहे, “नहीं हुज़ूर! सब के पांव पड़े और हर एक से दो दो चाँटे खाये।” दूसरे ने कहा, “नहीं साहब, एक पांव पर खड़ा हो कर हमारे सामने नाचे।” आख़िर में बादशाह सलामत बोले, “हम हुक्म देते हैं कि चोर को काग़ज़ की एक लंबोतरी नोक-दार टोपी पहनाई जाये और उसके चेहरे पर स्याही मल दी जाये और ये इसी हालत में जाकर अंदर से हुक़्क़े की चिलिम भर कर लाये।” सब ने कहा, “क्या दिमाग़ पाया है हुज़ूर ने! क्या सज़ा तजवीज़ की है। वाह वा।”
हम भी मज़े में आये हुए थे। हमने कहा, “तो हुआ क्या? आज हम हैं कल किसी और की बारी आ जाएगी।” निहायत ख़ंदा पेशानी से अपने चेहरे को पेश किया। हंस हंस कर वो बेहूदा सी टोपी पहनी। एक शान-ए-इस्तिग़ना के साथ चिलम उठाई और ज़नाने का दरवाज़ा खोल कर बावर्ची-ख़ाने को चल दिये और हमारे पीछे कमरा क़हक़हों से गूँज रहा था।
सहन में पहुंचे ही थे कि बाहर का दरवाज़ा खुला और एक बुर्क़ा-पोश ख़ातून अंदर दाख़िल हुई। मुँह से बुर्क़ा उल्टा तो रौशन आरा!
दम ख़ुश्क हो गया। बदन पर एक लर्ज़ा सा तारी हो गया। ज़बान बंद हो गई। सामने वो रौशन आरा जिस को मैंने तार दे कर बुलाया था कि, “तुम फ़ौरन आ जाओ। मैं बहुत उदास हूँ।” और अपनी ये हालत कि मुँह पर स्याही मली है, सर पर वो लंबोतरी सी काग़ज़ की टोपी पहन रखी है और हाथ में चिलम उठाए खड़े हैं और मर्दाने कमरे से क़हक़हों का शोर बराबर आ रहा है।
रूह मुंजमिद हो गई और तमाम हवास ने जवाब दे दिया। रौशन आरा कुछ देर तक चुपकी खड़ी देखती रही और फिर कहने लगी... बस मैं क्या बताऊं कि क्या कहने लगी? उसकी आवाज़ तो मेरे कानों तक जैसे बेहोशी के आ’लम में पहुंच रही थी।
अब तक आप इतना तो जान ही गये होंगे कि मैं बज़ात-ए-ख़ुद अज़ हद शरीफ़ वाक़े हुआ हूँ। जहां तक मैं मैं हूँ। मुझसे बेहतर मियाँ दुनिया पैदा नहीं कर सकती। मेरी ससुराल में सब की यही राय है और मेरा अपना ईमान भी यही है लेकिन इन दोस्तों ने मुझे रुसवा कर दिया है। इसलिए मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि अब या घर में रहूँगा या काम पर जाया करूँगा। न किसी से मिलूँगा और न किसी को अपने घर आने दूँगा सिवाए डाकिए या हज्जाम के, और उनसे भी निहायत मुख़्तसर बातें करूंगा।
“ख़त है?”
“जी हाँ।”
“दे जाओ। चले जाओ।”
“नाख़ुन तराश दो।”
“भाग जाओ।”
बस इससे ज़्यादा कलाम न करूंगा। आप देखिए तो सही!
स्रोत:
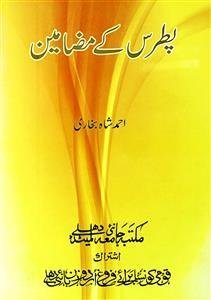
Patras Ke Mazameen (Pg. 70)
- लेखक: पतरस बुख़ारी
-
- प्रकाशक: डायरेक्टर क़ौमी कौंसिल बरा-ए-फ़रोग़-ए-उर्दू ज़बान, नई दिल्ली
- प्रकाशन वर्ष: 2011
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.