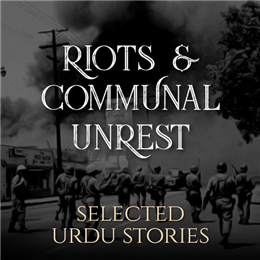उनकी ईद
स्टोरीलाइन
यह कहानी बाबरी विध्वंस के दौरान हुए दंगों में अपने प्रियजनों और अपनी संपत्ति को खो देने वाले एक मुस्लिम परिवार को आधार बनाकर लिखी गई है। मुंबई में उनके पास अपना एक अच्छा सा घर था और चलता हुआ कारोबार भी। उन्होंने अपने एक-दो रिश्तेदारों को भी अपने पास बुला लिया था। फिर शहर में दंगा भड़क उठा और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। वे वापस गाँव लौट आए, मायूस और बदहाल। गाँव में यह उनकी दूसरी ईद थी, पर दिलों में पहली ईद से कहीं ज़्यादा दुख था।
मुनीर मियां ने हस्ब-ए-दस्तूर मशीनी अंदाज़ में वुज़ू किया और घुटनों पर हाथ रखकर उठे। जिस्म जैसे गीला आटा हो रहा था, जिधर झुको उधर ढलक जाये। “आता हूँ नेक-बख़्त” उन्होंने बीवी से कहा, जो पिछले दो साल में बीस बरस का सफ़र तै कर चुकी थीं। हाथों में रअशा और नज़र कमज़ोर। वो भी घुटनों पर हाथ रखकर शौहर के पीछे किवाड़ बंद करने को उठीं।
मुनीर मियां मुहल्ले की मस्जिद की तरफ़ निकल गए। बरामदे में लोहे के हुक से टँगे पिंजरे में क़ैद मिट्ठू चिल्लाया, “दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो।” फिर बड़ी मीठी आवाज़ में बोला, “अम्मां आँ।”
काँपते हाथों से साजिदा बेगम ने दरवाज़ा बंद किया। काफ़ी दिन के इलाज के बाद अब बदन की कपकपाहट कम हो गई थी, लेकिन उंगलियां फिर भी क़ाबू में नहीं रहती थीं। खासतौर से जब मुनीर मियां बाहर जाते और वो पीछे से किवाड़ लगातीं। क्या बंद दरवाज़े तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी हैं? वो किवाड़ तोड़ न देंगे? वो, जो किवाड़ तोड़ देते हैं।
“अम्मां...आँ।' ये तो मिट्ठू है, सिर्फ़ मिट्ठू। फिर वो क्यों चौंकें? जैसे जैसे मासूम बच्चा माँ की छाती मुँह में लिये लिये चौंक जाये। किवाड़ बंद हैं। नमाज़ी नमाज़ में मसरूफ़ हैं। फ़िज़ा ख़ामोश है। दसवीं रमज़ान के चाँद में चमक बढ़ चली है। सब तरफ़ ख़ैरियत है, उनके दिल में भी और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
“अब की ईद देखिए, तीन को पड़ती है या चार को।” बासित, शाम को इफ़तार पर चला आया था।
क्या फ़र्क़ पड़ता है, कभी पड़े। हर रोज़ रोज़ आशूर है। फरात के किनारे ठाटें मारते पानी से चंद क़दम दूर अल-अतश, अल-अतश की सदाएँ। सुना है ज़ख़्म खाने वाले पानी मांगते हैं। ज़ख़्म लगें तो प्यास भी लगती है। उसके सारे जिस्म पर ज़ख़्म ही ज़ख़्म थे। उसे किसी ने पानी दिया था?
मुनीर मियां ने बासित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई, “लो मियां रोज़ा खोलो।” उन्होंने क़दरे शर्मिंदगी के साथ प्लेट उसकी तरफ़ बढ़ाई। चंद खजूरें थीं और एक तश्तरी में उबले हुए काबुली चने। सूजी का हलवा अलबत्ता कटोरा भरकर था, जो बासित के आ निकलने पर जल्दी जल्दी तैयार कर लिया गया था। ऐसे ही मौक़ों के लिए साजिदा चची कुछ जल्द तैयार होजाने वाली चीज़ों का इंतज़ाम रखती थीं कि शायद कोई आ निकले।
“बेटा, हम लोग खजूर से रोज़ा खोल कर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सीधे ही खाना खा लेते हैं। तुम ज़रा पहले आते तो इफ़्तारी तैयार होजाती। अब नमाज़ पढ़ आओ, फिर खाना ख़ाके ही जाना। जो भी है दाल दलिया। बेटा, अब कुछ खाने को जी चाहता है न पकाने को।'
“हलवा बहुत सा है चची।” बासित ने जल्दी से कहा, “मज़ेदार भी है और खाना तो मैं तरावीह के बाद खाता हूँ, इसलिए आप खाने की फ़िक्र न करें। आप लोग अपने मामूल के मुताबिक़ खा लीजिएगा।”
दोनों ख़ामोशी से बासित के हलवा ख़त्म करने का इंतज़ार करने लगे थे।
“चचा, थोड़ा सा आप भी तो लीजिए।” बासित ने प्याला मुनीर मियां की तरफ़ बढ़ाया। ऐसा लगा जैसे वो मेज़बान है और मुनीर मियां मेहमान।
“नहीं बेटा, नहीं हज़म होगा।” उन्होंने मुख़्तसर-सा जवाब दिया।
बासित ख़ामोशी से मुँह चलाता रहा। सिर्फ़ तीन साल पहले लाँबे, मज़बूत मुनीर चचा कटोरा भर तर तराता हलवा खाकर एक बड़ा गिलास दूध पिया करते थे और अपनी उम्र से दस बरस कम नज़र आते थे। मगर अब किसी पुरानी हवेली की दीवारों की तरह ढय गए हैं मुनीर चचा। बासित बम्बई गया था तो उन लोगों का मेहमान बना था। बड़ी ख़ैर हुई जो वो फ़सादात से पहले वापस आगया था। लेकिन ज़फ़र मामूं इतने ख़ुशक़िस्मत नहीं थे। ज़फ़र मामूं जो बासित के सगे मामूं होते थे और साजिदा चची के ख़ालाज़ाद भाई। हँसमुख, मेहनती। उनकी परचून की दुकान थी। मज़े में खा-कमा रहे थे। मौत ने चुपके से कान में कहा, दुकान में रेडीमेड कपड़ों का काउंटर भी खोल लो। बहुत मुनाफ़ा होगा। वो मश्वरा मान कर मुनीर चचा के पास पहुँच गए बम्बई। उधर फ़िज़ा गर्म होने लगी थी और धूल उठ रही थी। छः दिसंबर को सूरमाओं ने अपना ग़ुस्सा ईंट पत्थर की बेजान पाँच सौ साला पुरानी इमारत पर उतारा। फिर ज़फ़र मामूं, अजोध्या से सैकड़ों मील दूर रोज़ी रोटी की तलाश में निकले हुए ज़फ़र मामूं, दो जवान होती हुई बेटियों और दो बढ़ते बेटों के बाप, वालिदैन की धुँदलाती आँखों के तारे, निहत्ते और बेक़सूर ज़ब्ह कर दिए गए।
ज़फ़र किस की राह में ज़ब्ह किया गया? वो किसी पैग़ंबर का बेटा नहीं था कि उसकी क़ुर्बानी अल्लाह को मंज़ूर होती। ज़फ़र किसी फ़ौज में नहीं लड़ रहा था कि दुश्मन के सिपाही उसे क़त्ल करते। ज़फ़र किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं था कि क़ानून उसे मौत की सज़ा सुनाता। ज़फ़र किसी के ख़ून का क़िसास भी नहीं था। ज़फ़र का मीर बाक़ी से कोई रिश्ता था या उसके ख़ानदान का कोई शख़्स बाहर से ताल्लुक़ रखता था, उसके इमकानात भी नहीं थे। लेकिन साजिदा चची बहुत पढ़ी लिखी नहीं थीं और मीर बाक़ी का तो उन्होंने नाम तक नहीं सुना था। कुछ अर्से पहले तक तो वो बाबरी मस्जिद को भी नहीं जानती थीं। इसलिए वो इतने सारे अलफ़ाज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती थीं।
वो तो सिर्फ़ हैरान-ओ-परेशान खड़ी कफ़-ए-अफ़सोस मिलती रहीं और भाई के ग़म में उनका कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। अब वो भावज से किस मुँह से मिलेंगी। सुबह तक तो ज़फ़र बिल्कुल ठीक था। हट्टा कट्टा, ख़ुश मिज़ाज और सेहतमंद। हाँ, मस्जिद टूटने की बात आम हुई तो उसकी आँखों में एक सुलगी सुलगी सी कैफ़ियत ज़रूर बेदार हुई थी। उसने बाज़ू पर स्याह पट्टी बाँधी थी बस। लेकिन क्या अपने किसी नुक़्सान पर रंज के इज़हार की सज़ा मौत हुआ करती है? कौन से क़ानून के मुताबिक़? किस जंगल का क़ानून था ये और किस ने अशरफ़-उल-मख़लूक़ात को ये क़ानून सिखाया था? साजिदा बेगम को नहीं मालूम था कि जंगल के ज़्यादा बेरहम क़ानून अभी उनके मुंतज़िर हैं।
“बेटा, उठो, मग़रिब की नमाज़ का वक़्त बड़ा मुख़्तसर होता है।” मुनीर चचा ने बासित से कहा।
“और ज़िंदगी का भी, सिर्फ़ दुखों की काली रात तवील होती है।” बासित ने जल्दी से हलवे का आख़िरी चमचा मुँह में डाला।
साजिदा चची ने धीमी आँच पर चाय का पानी रख दिया और ख़ुद भी नमाज़ के लिए सर पर दुपट्टा दुरुस्त करने लगीं। दोनों नमाज़ पढ़ कर आएंगे तो वो चाय की कश्ती हाज़िर करेंगी। बस एक चाय थी जो बरक़रार रह गई थी। बाक़ी सारे शौक़ मियां-बीवी ने तर्क कर दिए थे। साजिदा चची ने पान तक छोड़ दिया था।
मुनीर मियां और बासित लप-झप मस्जिद की तरफ़ चले जो बिल्कुल क़रीब ही थी। सलाम फेरते वक़्त दोनों की निगाहें चार हुईं। बासित इसीलिए उनके यहाँ आने से कतराता था। जब भी मिलो ऐसा गहरा इ इज़्मेह्लाल तारी होजाता था कि दो-चार दिन किसी काम में जी न लगे। ऐसी बेचारगी थी मुनीर मियां के चेहरे पर। बासित के दिल में होलनाक ख़्यालात उठने लगे। ख़ुदा के हुज़ूर में झुके ये सर क्या सिर्फ़ इसलिए तह-ए-तेग़ कर दिए जाऐंगे कि वो एक मख़सूस सिम्त की तरफ़ मुँह कर के ख़ुदाए वाहिद की इबादत करते हैं? चौड़े शानों वाला, महबूब आलम घड़ीसाज़, ज़रदोज़ी का छोटा सा कारख़ाना चलाने वाला सिराज, अठारह साला खलन्डरा बिब्बी... क्या ये सब मार दिए जाएंगे? क्या उनके चेहरे पत्थरों से कुचल दिए जाएंगे कि उनकी शनाख़्त न हो सके, जैसे फ़सादात के दूसरे दौर में ज़ीशान...
लाहौल वलाकूव, बासित, तुमने तो फ़साद झेला भी नहीं। ज़िंदा सलामत हो। तब भी तुम्हारा दिमाग़ यूं ख़राब हो रहा है। ख़ामोश कलजिब्भे, क्यों काली बातें सोच रहे हो? रात काली है। दिन में सूरज छुपा छुपा सा रहता है और तातारियों के ग़ोल हरकत में हैं। इन सबको अच्छा रखियो अल्लाह ताला... बासित ने लरज़ कर सोचा और दुआ की, और बनी नौअ इंसान को अक़्ल दीजियो अल्लाह ताला, जो तुमने आज तक न दी, अगरचे उसे अशरफ़-उल-मख़लूक़ात का दर्जा दिया।
मुनीर चचा की पेशानी पर सियह गट्टा चमक रहा था। उन्होंने दुआ के लिए हाथ फैला दिए थे और हिल हिल कर क़ल्ब की इंतिहाई गहराइयों से दुआ मांग रहे थे। लेकिन अब उन्हें क्या माँगना था अल्लाह से? क्या ज़ीशान और नूरैन की मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे थे वो? जिस लड़के को घर से घसीट कर बाहर निकाला जाये और फिर पत्थरों से कुचल कुचल कर हलाक कर दिया जाये, क्या उसके किसी गुनाह की सज़ा बाक़ी रह जाती है जो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाये? और नूरैन... बासित तेज़ हवा में किसी लुंड मुंड दरख़्त पर लगे वाहिद पत्ते की तरह काँपा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आँतें मुँह को आरही हैं और उसका खाया पिया सब वहीं बाहर आजाएगा। नूरैन को वो उठाले गए थे।
“अल्लाह!” मुनीर चचा घुटनों पर हाथ रखकर उठे। अल्लाह पर मुनीर चचा का यक़ीन कैसे बाक़ी है? नमक की डली की तरह घुलने वाले मुनीर चचा ये सोच कर कि वो क्यों ज़िंदा बचे, पल पल मरने वाले मुनीर चचा। उन्होंने बासित के कंधों पर हाथ रखा, “चलो बेटा, चाय पी लो। और फिर वापस अपने घर जाना। तुम्हारी चची चाय लेकर बैठी होंगी।”
बासित ख़ामोशी से साथ चलने लगा।
“बच्चों के कपड़े लत्ते बनवा लिये?” मुनीर चचा ने सवाल किया।
“जी।” कहते हुए बासित को जैसे गुनाह का एहसास हुआ। वो क्यों ख़ुश है? ख़ुशियों पर उसका क्या हक़ है?
“शमशाद को हम लोगों ने उसकी ख़ाला के घर भेज दिया है। वहाँ उसकी उम्र के बच्चे हैं।” मुनीर मियां ने कमज़ोर आवाज़ में कहा।
“मालूम है चचा।” बासित ने मुख़्तसर सा जवाब दिया।
शमशाद मुनीर चचा का दस साला पोता है। ज़ीशान और नूरैन का बच्चा, बल्कि बचा हुआ बच्चा। उसने अपने बाप को बलवाइयों के हाथों घसीटे जाते देखा। अपनी नौजवान माँ की कर्बनाक चीख़ें सुनीं। अपने सोलह साला भाई को पुलिस के हाथों इंतिहाई बेरहमी से पिटते देखा। फिर ये तीनों कभी वापस नहीं आए। ज़िंदगी ने धूल, मिट्टी, आग, धुएं और ख़ून में लोट लगाई और जब वो पलटी तो उसका चेहरा मुख़्तलिफ़ हो चुका था। किसी दीवानी चुड़ैल का चेहरा या क़ब्रिस्तान का चेहरा जहाँ सन्नाटा होता है, और वहशत और इबरत होती है और ईद मुहर्रम का समां पेश करती है।
अल-अतश, अल-अतश, ये गला क्यों सूखता है इतना? क्या बदले की आग से जो सीनों में दहक रही है? मुस्तक़बिल के ख़ौफ़ से जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जगाता है?
मुनीर चचा ने अपनी छोटी सी बेकरी बेच दी थी। वो अब वहाँ रहना नहीं चाहते थे। उन ख़ौफ़नाक यादों के बीच और फिर उन धमकियों के दरमियान जो फ़साद होजाने के बहुत बाद तक उन्हें मिलती रही थीं। कोई मुसलमान वो बेकरी ख़रीदने को तैयार नहीं था, इसलिए कि वो ग़ैर मुस्लिम इलाक़े में थी। और वो जो पहले क़तई बेज़रर थे, अब सारे के सारे ज़रर की अलामत बन चुके थे और दिलों में ख़ौफ़ जगाने लगे थे। वो अपने ही जैसे इंसानों में ख़ौफ़ जगाने लगे थे, अगरचे ज़िंदगी उन सबके लिए यकसाँ सुख दुख से इबारत थी। यकसाँ सुख दुख और यकसाँ सूद-ओ-ज़ियाँ। और उन सबकी रगों में बहने वाला लहू भी एक जैसा ही था। फिर भी उनमें से कुछ, दूसरों के लिए ज़रर की अलामत थे। और जो कुछ हो रहा था या हुआ था, होना नहीं चाहिए था।
बेकरी निहायत औने-पौने फ़रोख़्त हुई। अपने वतन वापस आकर मुनीर मियां ने ये टूटा फूटा बेरौनक़ मकान ख़रीदा। इससे बेहतर की न उनकी इस्तिताअत थी, न ख़्वाहिश। बाक़ी रूपों से उन्होंने छोटी सी परचून की दुकान खोली। शमशाद उनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा था। उसे परवान चढ़ाना था। जब तक ज़िंदा थे, पेट में कुछ डालना था और ज़फ़र के कुन्बे को भी देखना था। बरसहाबरस से रोशनियों और कंक्रीट के इस देवक़ामत शहर में रहने की आदत के बावजूद वो बग़ैर किसी परेशानी के अपने आबाई क़स्बे में रहने लगे थे।
“रहते तो बेटा हम अपने जिस्म की क़ब्र में हैं और हम कहीं नहीं रहते।” मुनीर चचा ने सादगी से कहा था, “और अगर जिस्म क़ब्र बन जाये तो बम्बई क्या और ये गाँव नुमा क़स्बा क्या।”
पिछली ईद पर, जो यहाँ मुनीर मियां की पहली ईद थी, सारे अज़ीज़ उनके घर ज़रूर आए थे, और किसी के घर गए हों या न गए हों। सबके दिल उदास हो गए थे। दोनों मियां बीवी के सपाट चेहरे ऐसे थे जैसे किसी घर के मुक़फ़्फ़ल किवाड़। ‘हमारा दुख तुम्हारे साथ बांटने लायक़ नहीं है, उन मुक़फ़्फ़ल किवाड़ों पर लटकी तख़्ती पर लिखा था, उसे अंदर ही रहने दो, वरना ये तुम्हें सैल-ए-बला की तरह बहा ले जाएगा।’ उन्होंने दिल के किवाड़ मुक़फ़्फ़ल रखे, फिर भी लोग उदास हुए और मुनव्वर आपा तो साजिदा चची से लिपट कर इतना रोईं कि बेहोश हो गईं। दरअसल उनका जवान दामाद उनही दिनों काफ़ी अरसा बीमार रह कर मर गया था। बड़ा ही नेक और बीवी-बच्चों से मुहब्बत करने वाला इंसान था। घरेलू और मेहनती। अच्छा कमाता था और दिल खोल कर ख़र्च करता था। मुबारक हैं वो जो चैन से मरते हैं। बंद किवाड़ों के अंदर से बाहर ले जाये जाकर, बेख़ता, बेक़सूर संगसार नहीं किए जाते। मगर साजिदा चची ने कहा कुछ नहीं, ख़ामोश रहीं। उनका दुख समुंद्र था जो दूसरों के दुख की नदियों को अपने अंदर ख़ामोशी से समेट लेता था। समुंद्र गहरा होता है और समुंद्र में कभी सैलाब नहीं आता। सिर्फ अंदर ही अंदर धारे चलते हैं, सर्द भी और गर्म भी।
बासित को उन लोगों से बेहद हमदर्दी थी, लेकिन वो ईद के दिन वहाँ नहीं आना चाहता था। घर पर हू का आलम। एक क़ब्ल अज़ वक़्त बूढ़ा होजाने वाला मर्द और एक क़ब्ल अज़ वक़्त बूढ़ी होजाने वाली औरत, जिसके चेहरे पर बेचारगी पुती हुई थी और आँखें लबालब कटोरे। बरामदे की खपरैल से लटका मिट्ठू का पिंजरा।
“अम्मां... आँ...!”
किसने पुकारा? ज़ीशान ने या सआदतमंद ख़ुश शक्ल, रुनझुन पायल बजाती बहू ने? (या मज़लूम ज़फ़र ने जिसका इस इफ़रियत नुमा शहर से कोई वास्ता या मतलब ही न था। वो वहाँ सिर्फ़ मरने आया था या खट्टे मीठे तज्रिबों से गुज़रती उनकी साबिक़ा ख़ुश-ओ-ख़ुर्रम ज़िंदगी ने...
किसी ने भी नहीं, ये तो मिट्ठू है जो बे सोचे समझे बोलता है।
साजिदा चची ने फिर भी साफ़ धुला हुआ दस्तरख़्वान बिछाया था।
“चची!” बासित और साथ आए हुए दो और अज़ीज़ों के मुँह से बैक वक़्त निकला था।
“ईद है बेटा।” उन्होंने रसान से कहा था, “मुँह मीठा करो, त्योहार के दिन तुम क्यों बद शगुनों से गुज़रो।”
फिर वो दो प्यालियों में सेवइयां लाईं, सादी बिल्कुल। उबाल कर सिर्फ़ दूध, चीनी डाली हुई और सिर्फ़ सेवइयां। ज़िंदगी की तरह उनका भरा पुरा दस्तरख़्वान भी सिमट चुका था। लोगों ने चुपचाप सेवइयां खालीं कि चची की दिल शिकनी ना हो। फिर वो घुटनों पर हाथ रखकर उठीं, ताक़ पर से टटोल कर सौंफ की तश्तरी उठाई, “लो सौंफ लो।” उन लोगों ने ख़ामोशी से सौंफ भी ले ली। थोड़ी देर यूँही बैठे रह कर उन्होंने कहा,
“अब चलते हैं चची।”
“अच्छा बेटा।” चची ने जवाब दिया।
बासित और वो अज़ीज़ रुख़्सत हो गए। उनके बाहर निकलने पर किवाड़ खुला तो कुंडी देर तक खड़कती रही।
“कौन है, कौन है?” मिट्ठू ने पिंजरे में चक फेरीयां लगाईं, फिर ख़ुद ही बोला, “कोई नहीं, कोई नहीं।”
सारे अज़ीज़ नमाज़ के बाद ही एक एक दो दो करके आके मिल गए थे। अब अपने बे-ख़्वाब किवाड़ों को मुक़फ़्फ़ल करलो। ज़ीशान कभी नहीं आएगा। नूरैन का दला हुआ, कटा फटा जिस्म तक नहीं मिलेगा और उनके बड़े बेटे नौशाद का भी नहीं। और ज़फ़र भी वहीं गया है। वो भी नहीं आएगा। मगर तुम क्यों रंजीदा होते हो? मुनीर मियां, वो तो बहुत से थे जो यूं मारे गए। ईद तुम अकेले की तो नहीं, इन सारे घरों में ऐसी ही ईद है। मेहंदी, इत्र, पान, सेवइयों, मिठास और मसर्रतों से आरी, बेरंग-ओ-नूर।
धूप छोटे से कच्चे आँगन में लगे अमरूद के दरख़्त की फुँग से होती हुई दीवार पर चढ़ चुकी थी। पाँच बज रहे होंगे। साजिदा बीबी ने अस्र की नमाज़ के लिए वुज़ू करना शुरू कर दिया था। सुबह नूरैन के रिश्ते के ख़ालू वसी अहमद भी आए थे, साथ में बच्चे भी थे। कह गए थे कि उनकी अम्मां नहीं आ सकीं, कल आएंगी, आज फ़ुर्सत नहीं मिलेगी।
“त्योहार के दिन औरतों को कहाँ फ़ुर्सत?” साजिदा बीबी ने सिदक़ दिली से कहा। ख़ुदा न करे जो किसी को ईद के दिन ऐसी फ़ुर्सत मिले। उन्होंने मस्ह के लिए बालों में उंगलियां फेरीं, वुज़ू मुकम्मल किया और झुकी झुकी सी उठने लगीं, अल्लाह... फिर उन्होंने अस्र के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ी और फिर इशा की। ईद ख़त्म हुई। किसी भी आम दिन की तरह वो ईद का दिन था। फिर भी इसमें कोई ख़ास बात नहीं हो सकी थी। वो वैसा ही दिन था जैसा अब गुज़रने वाला कोई भी दिन। बेकरां, उदास और बेहिसाब उजाड़। दिल के रेगिस्तान में आग बरसाती हवाएं चकराती फिरती थीं और चेहरे के किवाड़ मुक़फ़्फ़ल थे।
मुनीर चचा के साथ चलता हुआ बासित सोच रहा था कि इस बार ईद पर उनके यहाँ लोग शायद पिछली बार से कम आएं। पिछली बार उनकी पहली ईद थी। ख़ुद बासित दो बार रमज़ान में आचुका है। आज उनके साथ इफ़्तार भी कर लिया है। अगर ईद में न आसका तो ऐसी कोई शिकायत की बात नहीं होगी। वो बेरहमी नहीं बरत रहा है, न ही तोता-चश्मी। वो अपने अंदर की उस बेकली से बचना चाहता है जो उनकी ईद में शरीक हो कर उसे मिलती है। ईद जो जाड़ों में हल्के बादलों से छन कर आती उदास, मरियल धूप की तरह उनके आँगन में उतरती है और शाम होने से पहले दबे-पाँव रुख़्सत होजाती है और रात को सोने से पहले वो दुआ करते हैं कि सुबह को उनकी आँखें न खुलीं तो कितना अच्छा हो। दुनिया का क्या है, दुनिया तो यूँही रवाँ-दवाँ रहेगी।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.