बन्दर का घाव
स्टोरीलाइन
मध्यम वर्ग की एक लड़की की कहानी है। यौवनावस्था में वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने पड़ोस में रहने वाले एक छात्र की मुहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और उससे मिलने की ख़ातिर रात में अपनी छत पर चढ़ती है लेकिन डर की वजह से वो सीढ़ियों से लुढ़क जाती है। उसके इस कर्म से घर वाले जाग जाते हैं और फिर बाप और भाई की ग़ैरत जोश में आ जाती है और वो उसे अध मुआ करके सिसक सिसक कर ज़िंदा रहने के लिए छोड़ देते हैं।
वो बरामदे में झिलंगी खाट पर नई दुल्हन की तरह गठरी बनी पड़ी थी। गर्मी की भरी दोपहर, उस पर ठैरा हुआ बुख़ार... जी बौलाया जा रहा था। कमरे में घर के सब अफ़राद दरवाज़े बंद किए आराम से हँस बोल रहे थे। कई बार उसका जी चाहा कि वो भी सूरज की तपिश से पनाह लेने के लिए कमरे में जा पड़े। लेकिन उसको डर था कि कहीं उसे देखते ही कड़वी नसीहतों की बोतलें न खुल जाएँ। इसलिए वो सूरज की तपिश और बुख़ार की हालत में भी इस थोड़ी सी तन्हाई को ग़नीमत समझ रही थी।
तेज़-धूप और तेज़ बुख़ार। उसे रह-रह के ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियों का गूदा पिघल गया है और उसमें उसकी नस-नस तली जा रही है और उसकी कमानों की तरह उभरी हुई पसलियों को एक मज़बूत हाथ झाड़ू की सींकों की तरह तोड़-मरोड़ देना चाहता है। इस अजीब एहसास से उसे खाँसी आने लगी। वही खाँसी... इस तरह जैसे कोई लकड़ी के घुने हुए ख़ाली संदूक़ को धप धपाए, खाँसते-खाँसते उसके हलक़ से कोई चीज़ उमड़ आई और उसने लेटे लेटे खाट के ढीले बानों को सरका कर थूका। जमे हुए ख़ून का एक छोटा सा लोथड़ा चप से ज़मीन पर चिपक गया और इससे पहले कि वो ख़ून को देखकर कुछ सोचती, बंदरों के खोखियाने की आवाज़ सुनकर बेहिस-ओ-हरकत पड़ गई। क्योंकि उसे बंदरों से बहुत ख़ौफ़ मालूम होता था। उसने बग़ैर गर्दन मोड़े आँखें घुमा कर उस तरफ़ देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी।
हाय अल्लाह... उसके पपड़ियाए हुए होंटों को और भी झुलसाता हुआ निकला ओफ़ो, कितने बहुत से बंदर बावर्ची-ख़ाने के पिछवाड़े वाली नीम से धपा-धप छत पर उल्टी सीधी छलाँगें लगा रहे थे। उसका दिल एक दम चाहा कि वो भाग कर कमरे में घुस जाये। लेकिन इस डर के मारे वो हरकत न कर सकी कि कहीं ये सब बंदर उस पर टूट न पड़ें।
काई से काली मुंडेर पर एक मरझल्ला सा बंदर पड़ा सिसक रहा था और उसके इर्द-गिर्द कई मोटे मोटे बंदर बैठे उसकी पीठ के स्याह घिनौने घाव को अपने तेज़ नाख़ुनों से कुरेद रहे थे। बंदर का मकरूह घाव देखकर उसे फुरेरियाँ आने लगीं। और बंदर थे कि ज़ख़्म के मुआइने में पूरी तरह मुनहमिक, अभी एक घाव में हाथ घंघोल रहा है और दूसरा खीसें निकालता, पपोटे पीटता, वही अमल शुरू कर देता। गोया एक ज़ख़्मी और सैंकड़ों जर्राह। और वो बेचारा मरझल्ला बंदर था कि मारे तकलीफ़ के सर ढ़लकाए देता। ऐसा मालूम होता कि बस अब मरा, अब मरा। वो सोचने लगी कि ये कम्बख़्त यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता? भला इस तरह अपने घाव का मुआइना कराते-कराते जान देने से हासिल? लेकिन बे-अक़्ल जानवर, फिर भी उसे उस मज़लूम की बेकसी पर बड़ा रहम आ रहा था।
उसका जी चाहा कि वो किसी तरह उन धौं के धौं बंदरों से उसका पीछा छुड़ा दे जो हमदर्दी के बहाने तमाशा देख रहे हैं लेकिन... लेकिन यक-लख़्त उसकी पसलियों पर कोई मज़बूत हाथ ज़ोर-आज़माई करने लगा। खाँसी और सीने से लेकर हलक़ तक गुदगुदी। उसका मुँह इस तरह भर गया जैसे उसने बैक वक़्त पान की कई गिलौरियों की पीक इकट्ठी कर ली हो, उसने घबरा कर थूका। ही ई ई... सुर्ख़-सुर्ख़ जीता हुआ ख़ून, हाथ-पाँव ढीले पड़ गए और वो अपना धमकता हुआ सर फाँसों भरी खाट पर रगड़ने लगी।
बंदर ख़ोखिया रहे थे और कमरे में घर के लोग उसके यूँ अलग-थलग रहने पर बातें बना रहे थे। उसने बेज़ार हो कर ढ़ीली-ढ़ीली टाँगें पसार कर पट्टी से अड़ा लीं और दोनों हाथ सीने पर रख लिए। उसके कानों में घर वालों के बड़बड़ाने और बंदरों के खोखियाने की आवाज़ें लोहे की गर्म-गर्म सलाख़ों की मानिंद उतरती मालूम हो रही थीं। बंदर और घर वाले कितने हम-आहंग हैं। उसे ख़्याल आया और उसे अपने सारे जिस्म में नब्ज़ों की फड़क महसूस होने लगी। मअन जैसे उससे किसी ने कह दिया हो कि तू भी उस मरझल्ले बंदर की तरह है जो जानते बूझते मोहलिक बीमारियों का शिकार हो रही है और फिर बतौर दलील उसके धमकते हुए दिमाग़ पर कुछ ज़माना-ए-क़ब्ल की कई अनमिट तस्वीरें उभर आईं।
“तेईस-चौबीस बरस की जवान पुच्छती, आँखों में नहीं समाती अब तो।” माँ कुछ जल कर फ़िक्र-मंद लहजे में कह उठती और उसे अपने पहाड़ जैसे कंवार-पने का बहुत एहसास होने लगता। उसके ख़ानदान की हम-उम्र लड़कियाँ बल्कि उससे भी कम्सिन लड़कियाँ कितने ही साल हुए ब्याही जा चुकी थीं। कई के चार-चार, पाँच-पाँच बच्चे भी हो चुके थे। कई अपने शौहरों की नज़र में पुराना घिसा हुआ माल हो कर मैके में पड़ी तावीज़ों और पीर साहिबान के अमलियात के ज़रिए अपनी फटी-पुरानी जवानियाँ रफ़ू करा रही थीं। लेकिन एक वही न जाने कैसी क़िस्मत लेकर आई थी कि अब तक इस अछूती बेरी पर किसी ने ढे़ला फेंकने की ज़हमत न गवारा फ़रमाई। सूरत शक्ल की कहो तो ऐसी बुरी भी न थी। बड़ी सुघड़ और बे-मुँह की लड़की थी। इसके बावजूद उसकी शादी का कहीं बंद-ओ-बस्त हो ही न पाता था।
इतनी बात ज़रूर थी कि सिवाए उसके और उसकी माँ के किसी और को इतनी फ़िक्र भी न थी। बाप था तो उसको सिर्फ पड़े-पड़े हुक़्क़ा पीने और हर दूसरे साल एक अदद बच्चे के इज़ाफ़ा पर फ़ख़्र करने के अलावा तीसरा काम न था। बड़ा भाई सो अपनी फ़िक्र में मगन। आज धोबिन पर आशिक़ तो कल मेहतरानी पर फ़िदा और चुपके-चुपके भी नहीं। खुल्लम-खुल्ला, जवान बहन के सामने आहें भरने, चटख़ारे लेने और जा व बेजा खुजाने से भी न चूकता।
तो वो कुछ ऐसे माहौल में साँस ले रही थी। माँ ने उसकी भरपूर जवानी को ख़ानादारी की सिल के नीचे बहुत दबाना चाहा लेकिन तौबा एक वक़्त हुआ करता है। जब सूप का उलारा सूप में नहीं रहता। आपने कभी चूल्हे पर पकती हुई दाल तो देखी ही होगी और ये भी देखा होगा कि जिस वक़्त उबाल आता है तो हंडिया देखने वाला जल्दी से पतीली का ढ़कना हटा देता है। इस तरह उबाल में कुछ कमी आ जाती है ना? और अगर ग़लती से ढ़कना न हटाया जाये तो उबाल उसे ख़ुद-ब-ख़ुद उछाल कर अपने लिए राह पैदा कर लेता है। ग़लत तो नहीं? हाँ तो उसकी ज़िंदगी में भी उबाल की सी कैफ़ियत पैदा हो गई। हया के बोझ से झुकी हुई आँखें कुछ ढ़ूँढ़ने के लिए इधर-उधर उठने लगीं। वैसे तो पड़ोसन का मकान अर्से से ख़ाली पड़ा था लेकिन इधर सुना कि कोई तालिब-ए-इल्म आकर रहा है।
बस क्या था? ज़मीन के पेट में पेच-ओ-ताब खाते हुए लावे को फूट पड़ने के लिए ज़मीन की कमज़ोर परत मिल गई। काम-काज करते करते उसकी नज़रें इस दीवार की तरफ़ उठ जातीं जिसके पीछे कोई चलता फिरता हुआ रहता होगा। उसकी ख़ुद फ़रामोशियों पर माँ गालियाँ कोसने दे रही होती। लेकिन उसके कानों के पर्दे वो भारी सी अजनबी आवाज़ अपने में जज़्ब करने के लिए फड़फड़ाते रहते। घर में माँ-बाप आपस में झगड़ते होते और वो ख़्याल ही ख़्याल में दीवार पार के किसी के पहलू से जा लगती, लावा जो था... बस अंदर ही अंदर जोश खा रहा था।
“कोठे पर क्यों जा रही है ?” बड़ा भाई था बड़ा माहिर-ए-नफ़सियात। उसके हाथ में रंगा हुआ गीला दुपट्टा भिंच कर रह गया।
“दुपट्टा सुखाने।” उसकी तेवरी पर बल आगए। भूके के सामने से थाली सरकाई जाये और उसे ग़ुस्सा न आए।
“क्या यहाँ धूप नहीं है जो ऊपर जाने की ज़रूरत हुई?” उसने एक बा-गै़रत भाई की तरह उसे जलती हुई नज़रों से घूरा और फिर एक घटिया क़िस्म की सिगरेट सुलगाई। वो बुदबुदाती हुई दुपट्टा पलंग पर फेंक कर बैठ रही। भाई मुतमइन हो कर गुनगुनाने लगा... नैनों में नैना डाले, हो बाँके नैना वाले... और वो चिड़ कर दिल में कोसने देने लगी।
इधर देखा, उधर देखा। कोई भी उसके शौक़ में हारिज न था। ओफ़्फ़ोह, कितने दिन से वो इस सुराख़ से झाँकने की मुतमन्नी थी। उसने मौक़ा पाकर जल्दी से अपनी आँख उस नन्हे से सुराख़ से लगा दी। थोड़ी ही देर बाद एक गोरा चिट्टा सा चेहरा सामने आया और झप से गुज़र गया। एक झलक सिर्फ़ एक, उसका इज़्तिराब और बढ़ गया। काश, एक बार वो और सामने आ जाये... वो अपनी आँख सुराख़ से लगाए रही। कम्बख़्त सुराख़ भी तो ऐसी जगह था कि न तो पूरी तरह बैठ कर झाँका जा सकता था और न बिल्कुल खड़े ही हो कर। बस उस पर बिल्कुल रुकू की सी कैफ़ियत तारी थी। दोनों हाथ घुटनों पर, आँख सुराख़ पर और कान कमरे के दरवाज़ों पर। झुके झुके कमर दुख गई, हाथ सुन्न पड़ गए और कई बार तो पलकों की रगड़ से दीवार की मिट्टी झड़कर आँख में घुस गई लेकिन वो उसी तरह उस सुराख़ से चिम्टी रही और उससे अजीब अजीब उमंगें लिपटी रहीं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन... महीनों उस नन्हे से सुराख़ से इस नज़र के साथ साथ जिस्म ने भी पार हो जाना चाहा। लेकिन थक कर उसे यक़ीन आ गया कि ये ना-मुम्किन बात है।
“अम्माँ!” उसका छोटा भाई धमाधम ज़ीने से उतर रहा था, “साले ने मेरी पतंग काट ली।”
“ऐ किसने बेटा?” माँ के छक्के छूट गए। यानी अभी कल ही तो उन्होंने उसे चार पैसे की पतंग मंगा कर दी थी और वो भी कट गई।
“वही जो उधर आकर आ रहा है... कह रहा था कोठे पर पतंग न उड़ाया करो। गिर पड़ोगे नीचे।” वो मारे ग़ुस्से के पाँव पटख़े जा रहा था।
“तो क्या बुरा कहा?” आटा गूँधते-गूँधते रुक कर बोली।
“चल तू चुपकी बैठी रह।” माँ ने उसे फटकार दी, “वो बड़ा आया नसीहत करने... बच्चा कोठे पर न उड़ाए तो क्या उसकी मय्या के सीने पर उड़ाए? हाँ तो बेटा फिर उसने पतंग किस बात पर काटी?”
“मैंने कहा, तुम कौन होते हो मना करने वाले? ख़ूब उड़ाएंगे पतंग, तुम्हारा इजारा नहीं। बस इस पर उसने लंगर डाल कर पतंग काट ली।”
साहबज़ादे ने मज़े में आकर दो-चार मोटी मोटी गालियाँ बक डालीं और उसके जैसे मिर्चें ही लग गईं। जी चाहा कि आटा छोड़कर लगाए दो तीन, और ये अम्माँ? मना भी नहीं करतीं उसे... बालिशत भर का लौंडा और ये गालियाँ, वो इतनी बड़ी हो गई थी फिर भी जब उसने एक बार सिर्फ यूँही एक घरेलू गाली ग़ुस्से में आकर बक दी तो अम्माँ फुँकनी लेकर मारने खड़ी हो गई थीं मगर...
“हे हे, क़ुर्बान करूँ ऐसे ख़ुदाई फ़ौजदार को... तो बेटा जब वो छत पर ना हुआ करे तो उड़ाया कर पतंग... कमीनों के मुँह नहीं लगते और फिर तेरे अब्बा हैं ज़ालिम। कहीं सुन पाया तो अपनी उसकी जान एक कर देंगे।
“की न हो एक जान!” वो फिर बुदबुदाई, “भला ये भी कोई बात थी कि जिसके लिए वो इतने दिन से सूख रही थी, उसे कोई गालियाँ दे?”
“हुआ किया न करे? वो तो शाम से डटा रहता है छत पर। पलंग-वलंग भी वहीं डाल रखा है और शायद सोता भी वहीं है। मरे ख़ुदा करे, जनाज़ा निकले।” भाई कोसने देकर अपना दिल ठंडा कर रहा था। लेकिन वो आप ही आप मुस्कुरा रही थी। जैसे वो ये कोसने सुन ही न रही थी, और वाक़ई वो तो उस वक़्त कुछ सोच रही थी, एक बड़े मज़े की बात।
“पिंजरे का पंछी उड़ान के लिए पर तौल रहा था।”
रात को माँ ने पलंग पर लेटते ही चाबियों का गुच्छा कमरबंद से खोल कर देते हुए कहा, “लो ये... और कोठरी का ताला खोल कर ज़ीने के दरवाज़े में डाल दो। आज तो बच्चे की पतंग पर नीयत ख़राब की। कल को घर का सफ़ाया कर देगा, ए हाँ निगोड़ा!” और फिर अपना घड़ा जैसा चमकता हुआ पेट खोल कर इत्मीनान से टाँगें पसार दीं। अपने भर वो हिफ़ाज़त कर चुकी थीं। लेकिन उधर शुरू हो गया काट पेच। वो कोठरी का ताला खोलते हुए सोच रही थी, “छत से छत तो मिली हुई है। आज इससे वो सब कुछ क्यों न कह डालूँ जो होश सँभालने के बाद से अब तक दिल में भरा हुआ है।” ज़ीने का दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल कर दिया गया। लेकिन गुच्छे से उसकी चाबी ग़ायब हो कर तकिए के नीचे पहुँच गई।
चौकी के घंटे ने टन-टन दो बजाये। घर में सब बेख़बर सो रहे थे। वो तकिए के नीचे से चाबी निकाल कर नंगे पाँव उठ खड़ी हुई। हवा का एक भीगा सा झोंका आया और उसकी जवानी को हिल्कोरा दे गया। किसी ने सोते सोते पाँव पटख़ा और वो दबे क़दमों पानी की घड़ौंची के क़रीब जा खड़ी हुई। वो थोड़ी देर तक तारों की रोशनी में सबको घूरती रही कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर इत्मीनान करके उसने चुपके चुपके ताला खोला। अब दरवाज़ा खोलने की मुहिम थी। लेकिन वो भी बग़ैर चीं-चपड़ किए इस तरह वा हो गया जैसे कोई भूकी भिकारन चँद टकों की ख़ातिर लोथ पड़ जाये। कितने ज़ोर से उसका दिल धड़क रहा था। जैसे अब वो पसलियों को तोड़ कर रहेगा। ज़ीने के घुप-अँधेरे में उसकी जलती हुई आँखों के सामने वो सब तारे नाच रहे थे, जो उसने सर-ए-शाम से उस वक़्त तक गिने थे। और उसकी कनपटियां शिद्दत-ए-जज़्बात से धड़-धड़ कर रही थीं। इस पर भर्राए हुए मच्छरों की भुन-भुन और कचोके। जाने किस मुश्किल से आधे ज़ीने तै किए। उस वक़्त तो वाक़ई उसे अपना जिस्म पहाड़ मालूम हो रहा था। शौक़, ख़ौफ़ और अंधेरा। सांस रोकने से उसका सर चकराने लगा और फिर आँखों के सामने रंग-बिरंगे धब्बे फैल गए।
गदा गद... वो जवान पुच्छती, गेंद की तरह ज़ीनों पर गिरती-उछलती बाप के पलंग के पाए से जा टकराई।
हो हो... हाय... चोर... अल्लाह चीख़ें सुनकर उसकी आँखों के सामने के रंग-बिरंगे धब्बे सिकुड़ गए। लालटेन की बत्ती ऊँची की गई।
“हे हे ये।” माँ ने एक दोहत्तड़ अपने मुतज़लज़ल सीने पर रसीद किया, “अरे मैं तो पहले ही इस रंडी के गुन देख रही थी। हाय तू मर क्यों न गई।” ग़रीब माँ को तो जैसे ग़श आने लगा।
“ज़ब्ह कर दूँगा उसे, बस कोई रोके न मुझे... कहे देता हूँ। ऊपर से हो कर आई है मुर्दार।” बाप की हालत मारे ग़ैरत के ग़ैर हो गई। लेकिन शाबाश है कि आपे से बाहर तो था लेकिन कह रहा था सब चुपके चुपके... अरे हाँ, कोई और मुहल्ले वाले सुन लें तो... तो...
बड़ा भाई शायद अपनी नई माशूक़ा का ख़्वाब देखते देखते चौंका था। इसलिए उसकी जो हालत थी बस बयान से बाहर। दूसरे वो कितनी ही बार इशारों ही इशारों में उसे समझा भी चुका था कि “देखो ये कुँआ है इसमें किसी बहन को नहीं गिरना चाहिए।” इस पर भी न मानी तो ये ले... बस चोटी पकड़ी और देना शुरू किए झटके। बाप की ग़ैरत अंदर ही अंदर पेच-ओ-ताब खा रही थी। अब जो इतना आसान तरीक़ा देखा तो ख़ुद भी जुट गया। लेकिन माँ चूँकि बारहवीं उम्मीद से थी, इसलिए मेहनत से गुरेज़ कर गईं। वैसे जितनी भी ख़ास क़िस्म की गालियाँ याद थीं, हिर-फिर कर दुहराई जा रही थीं। लेकिन वो बेइंतिहा तकलीफ़ महसूस करते हुए भी चीख़ न सकती थी। इरादे की नाकामी इंसान को बुज़दिल बना देती है और बुज़दिल ही दुनिया से ख़ौफ़ खाता है। उसमें इतनी हिम्मत ही न थी कि इन मुजरिम मुंसिफ़ों के ख़िलाफ़ ज़बान हिला सके।
कितने ही महीने गुज़र गए इस वाक़िए को। वो समझती थी कि जिस तरह बड़े भाई अय्याशियाँ “सियाना है, ये उम्र ही ऐसी होती है” कह कर भुला दी जाती हैं, उसी तरह उसके अज़्म गुनाह को भी फ़रामोश कर दिया जाएगा, लेकिन पगली, औरत की हैसियत को भूल गई। औरत एक कठ-पुतली है जिसकी डोर समाज के कोढ़ी हाथों में है और उन कोढ़ी हाथों में जब चल होने लगती है तो डोर के झटकों से ये कठपुतली नचाई जाती है। लेकिन अगर उस कठपुतली में जान पड़ जाये और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ हरकत करने लगे तो समाज का लूथ पड़ा हुआ सड़ांध जिस्म... किससे दिलचस्पी ले? वो सोचती थी कि जिस तरह उसके घर वाले उसकी जवानी के तक़ाज़ों की तरफ़ से कान बहरे करके बैठ रहे, उसी तरह इस वाक़िए को भूल कर अपनी ग़लती को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन ये महज़ उसका ख़्याल था। उसके फ़रिश्ता-सिफ़त सरपरस्तों की नज़र में उसकी ज़िंदगी पर गुनाह की जो ख़राश आ गई थी, भला वो कभी मुंदमिल भी हो सकती थी।
“बदमाश...” उसका बदमाश भाई ज़रा सी बात पर कह उठता।
“अरी...” माँ उसकी उतरी सूरत ही देखकर एक साँस में घनी घनी गालियाँ सुना डालती।
मामूली ख़राश लॉन तान के ज़हरीले नाख़ुनों से कुरेदी जा रही थी। यहाँ तक कि वो ख़राश एक बड़ा सा घाव बना दी गई। ऐसा घाव जो अंदर ही अंदर सड़ कर ज़हरीला हो जाए और फिर उसका ज़हर ज़िंदगी पर सकरात तारी कर दे। लेकिन ख़ौफ़नाक नाख़ुन भर भी चैन नहीं लेते।
“यहाँ क्यों पड़ी है? निगोड़ी को बुख़ार वैसे ही रहता है। इस पर ये दीवार और धूप, मगर मैं जानती हूँ कि सब के संग बैठ कर काहे को दिल लगेगा। बातचीत होगी और बीवी बननो का ध्यान भटकेगा।” माँ खाँसती हुई लोटा ले पाख़ाने में जा घुसी।
उसने निढाल हो कर अपनी टांगें समेट लीं। बावर्चीख़ाने की छत पर मुस्टंडे बंदर अपने हिसाब ज़ख़्मी बंदर का इलाज कर रहे थे। उसके सीने में दर्द फिर अँगड़ाइयाँ लेने लगा। हलक़ से सीने तक सरसराहाट और फिर वही हड्डियों का पिघला हुआ गूदा उसे अंदर ही अंदर तलने लगा।
“अल्लाह!” उसने ललक कर पुकारा और फिर अपनी फ़रियादी नज़रें नीले आसमान की तरफ़ उठाईं जो एक वसीअ ढकने की तरह दुनिया पर रखा हुआ था। नज़रें देर तक ढकने के उस पार जाने की कोशिश करती रहीं। जहाँ उसके ख़्याल से इन्साफ़-ओ-रहम की दुनिया बसी थी। लेकिन फ़रियादी नज़रें नाकाम रहीं। थक कर उसे ख़्याल आया कि अल्लाह मियाँ अपनी दुनिया को आसमान के ढकने से ढक कर मुतमइन हो गए हैं। जिस तरह वो एक दिन कटोरे में बची-खुची दाल रख, ढक कर मुतमइन हो गई थी। लेकिन जब एक गर्म दोपहर गुज़रने के बाद उसे दाल का ख़्याल आया तो देखा दाल सड़ कर बजबजा रही थी।
स्रोत:
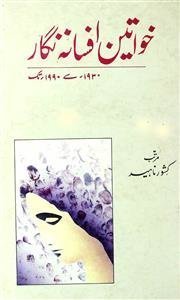
ख़्वातीन अफ़्साना निगार (Pg. 49)
-
- प्रकाशक: नियाज़ अहमद
- प्रकाशन वर्ष: 1996
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.

