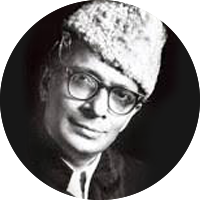डाची
पी सिकन्दर के मुसलमान जाट बाक़र को अपने माल की तरफ़ हरीसाना निगाहों से ताकते देखकर उकान्हा के घने दरख़्त से पीठ लगाए, नीम ग़ुनूदगी की सी हालत में बैठा चौधरी नंदू अपनी ऊंची घरघराती आवाज़ में ललकार उठा... रे रे उठे के करे है? (अरे यहां क्या कर रहा है?) और उस का छः फुट लंबा लहीम-शहीम जिस्म तन गया और बटन टूट जाने की वजह से मोटी खादी के कुरते से उस का चौड़ा चकला सीना और मज़बूत कंधे साफ़ दिखाई देने लगे।
बाक़र ज़रा नज़दीक आ गया। गर्द से भरी हुई नुकीली दाढ़ी और शरई मूंछों के ऊपर गढ़ों में धंसी हुई दो आँखों में एक लम्हे के लिए चमक पैदा हुई और ज़रा मुस्कुरा कर उसने कहा... डाची देख रहा था चौधरी। कैसी ख़ूबसूरत और जवान है। देखकर भूक मिटती है।
अपने माल की तारीफ़ सुनकर चौधरी नंदू का तनाव कुछ कम हुआ। ख़ुश हो कर बोला... कसी सांड? (कौन सी डाची?)
वो, परली से चौथी! बाक़र ने इशारा करते हुए कहा।
उकान्हा के एक घने पेड़ के साये में आठ दस ऊंट बंधे थे। उन्ही में वो जवान सांडनी अपनी लंबी, ख़ूबसूरत और सुडौल गर्दन बढाए पत्तों में मुँह मार रही थी। माल मंडी में दूर जहाँ तक नज़र काम करती थी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंटों, ख़ूबसूरत सांडनियों, काली मोटी बेडौल भैंसों और गायों के सिवा कुछ नज़र न आता था। गधे भी थे पर न होने के बराबर। ज़्यादातर तो ऊंट ही थे। बहावल नगर के रेगिस्तानी इलाक़े में उनकी कसरत है भी क़ुदरती। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है। इस तपते रेतीले इलाक़ा में आमद-व-रफ़्त, खेती बाड़ी और बार-बरदारी का काम उसी से होता है। पुराने वक़्तों में, जब गायें दस दस और बैल पंद्रह पंद्रह रुपये में मिल जाते थे, तब भी अच्छा ऊंट पच्चास से कम में हाथ न आता था और अब भी, जब इस इलाक़े में नहर आ गई है और पानी की इतनी क़िल्लत नहीं रही ऊंट की वक़त कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी ही है। सवारी के ऊंट दो-दो सौ से तीन-तीन सौ तक पा जाते हैं और बाही और बार बरदारी के भी अस्सी, सौ से कम में हाथ नहीं आते।
ज़रा और आगे बढ़कर बाक़र ने कहा, सच कहता हूँ चौधरी, उस जैसी ख़ूबसूरत सांडनी मुझे सारी मंडी में दिखाई नहीं दी।
मसर्रत से नंदू का सीना दुगना हो गया। बोला, आ एक ही के, ईहा तो सगली फोटड़ी हैं। हूँ तो उन्हें चारा फलोनसी नेरीया करूँ! (ये एक ही क्या? ये तो सभी ख़ूबसूरत हैं। मैं तो उन्हें चारा और फलोसी देता हूँ)
आहिस्ते से बाक़र ने पूछा, बेचोगे इसे?
अठई बेचने लई तो लाया हूँ! (यहां बेचने के लिए तो लाया हूँ) नंदू ने ज़रा तुर्शी से कहा।
तो फिर बताओ कितने को दोगे? बाक़र ने पूछा।
नंदू ने बाक़र पर सर से पांव तक एक निगाह डाली और हंसते हुए बोला, तने चाही जे, का तेरे धनी बी मोल लेसी? (तुझे चाहिए या अपने मालिक के लिए मोल लेगा)
मुझे चाहिए, बाक़र ने ज़रा सख़्ती से कहा।
नंदू ने बेपर्वाई से सर हिलाया। इस मज़दूर की ये बिसात कि ऐसी ख़ूबसूरत डाची मोल ले। बोला, तोल की लेसी? (तो क्या लेगा?)
बाक़र की जेब में पड़े हुए डेढ़ सौ के नोट जैसे बाहर उछल पड़ने को बेक़रार हो उठे। ज़रा जोश से उसने कहा, तुम्हें इससे क्या, कोई ले। तुम्हें तो अपनी क़ीमत से ग़रज़ है, तुम मोल बताओ?
नंदू ने इस के बोसीदा-कपड़ों, घुटनों से उठे हुए ता बंद और जैसे नूह के वक़्त से भी पुराने जूते को देखते हुए टालने की ग़रज़ से कहा, जा-जा तू अशि वशी मोल ले आई, एंहगो मोल तो आठ बीसी सूँ घाट के नहीं। (जा-जा तू कोई ऐसी वैसी डाची ले लेना उस की क़ीमत तो 160 से कम नहीं)
एक लम्हे के लिए बाक़र के थके हुए जिस्म में मसर्रत की लहर दौड़ गई। उसे डर था कि चौधरी कहीं इतना मोल न बता दे जो उस की बिसात से बाहर हो। लेकिन अब जब अपनी ज़बान ही से उसने एक सौ साठ बताए तो उसकी ख़ुशी का ठिकाना न रहा। 150 तो उसके पास थे ही। अगर इतने पर भी चौधरी न माना तो दस रुपये का इससे उधार कर लेगा। भाव-ताव करना तो उसे आता न था। झट से डेढ़ सौ के नोट निकाले और नंदू के आगे फेंक दिए। बोला, गिन लो, इनसे ज़्यादा मेरे पास एक पाई नहीं। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी!
नंदू ने बादिल-ए-नाख़्वास्ता नोट गिनने शुरू किये। लेकिन गिनती ख़त्म होते ही उसकी आँखें चमक उठीं। उसने तो बाक़र को टालने की ग़रज़ से मोल 160 बताया था। नहीं इस सांडनी के तो 140 पाने का ख़याल भी उसे ख़्वाब में नहीं था। लेकिन दिल की ख़ुशी को दिल ही में दबा कर और जैसे बाक़र पर एहसान का बोझ लादते हुए नंदू बोला, सांड तो मेरी दो से की है। पन जा, सगी मोल मियां तने दस छांडया। (सांडनी तो मेरी दो सौ की है, पर जाओ तुम्हें सारी क़ीमत में से दस रुपए छोड़ दिए) और ये कहते कहते उसने उठकर सांडनी की रस्सी बाक़र के हाथ में दे दी।
एक लम्हे के लिए उस वहशी सिफ़त इन्सान का दिल भी भर आया। ये सांडनी उसके यहां ही पैदा हुई और पली थी। आज पाल पोस कर उसे दूसरे के हाथ में सौंपते हुए उसके दिल की कुछ ऐसी ही हालत हुई जो लड़की को ससुराल भेजते वक़्त बाप की होती है। आवाज़ और लहजे को ज़रा नर्म कर के उसने कहा, आ सांड सोहरी रहेड़ी है। तू इन्हें रीहड़ ही में ना गेर दिये, (ये सांडनी अच्छी तरह पली है तो इसकी मिट्टी ख़राब न कर देना) ऐसे ही जैसे ख़ुसर दामाद से कह रहा हो, मेरी लरकी लाडों पली है। देखना उसे तकलीफ़ न हो।
ख़ुशी के परों पर उड़ते हुए बाक़र ने कहा, तुम फ़िक्र न करो, जान देकर पालूँगा!
नंदू ने नोट अंटी में सँभालते हुए जैसे सूखे हुए गले को ज़रा तर करने के लिए घड़े से मिट्टी का प्याला भरा। मंडी में चारों तरफ़ धूल उड़ रही थी। शहरों की माल मंडियों में भी, जहां बीसियों आरिज़ी नलके लग जाते हैं और सारा सारा दिन छिड़काव होता रहता है धूल की कमी नहीं होती। फिर उस रेगिस्तान की मंडी में धूल ही की सल्तन थी। गन्ने वाले की गंडेरों पर, हलवाई के हलवे, जलेबियों पर और ख़्वांचे वाले के दही पकौड़ी पर। ग़रज़ सब जगह धूल ही धूल नज़र आती थी। घड़े का पानी टांचियों के ज़रिये नहर से लाया गया था। पर यहां आते आते कीचड़ जैसा गदला हो गया था। नंदू का ख़याल था, निथरने पर पिएगा पर गला कुछ सूख रहा था। एक ही घूँट में प्याले को ख़त्म कर के नंदू ने उससे भी पीने के लिया कहा। बाक़र आया था तो उसे ग़ज़ब की प्यास लगी हुई थी, पर अब उसे पानी पीने की फ़ुर्सत कहाँ? रात होने से पहले पहले वो अपने गांव में पहुंच जाना चाहता था, डाची की रस्सी पकड़े हुए, गर्द-ओ-ग़ुबार को जैसे चीरता हुआ वो चल पड़ा।
बाक़र के दिल में बड़ी देर से एक ख़ूबसूरत और जवान डाची ख़रीदने की आरज़ू थी। ज़ात से वो कमीन था। उसके आबा-ओ-अजदाद कहारों का काम करते थे। लेकिन उसके बाप ने अपना क़दीम पेशा छोड़कर मज़दूरी से अपना पेट पालना शुरू कर दिया था और बाक़र भी उसी पेशे को इख़्तियार किये हुए था। मज़दूरी वो ज़्यादा करता हो, ये बात न थी। काम से हमेशा उसने जी चुराया था और चुराता भी क्यों न? जब उसकी बीवी उससे दुगना काम कर के उसके बोझ को बटाने और उसे आराम पहुंचाने के लिये मौजूद थी। कुम्बा बड़ा था नहीं। एक वो, एक उसकी बीवी और एक नन्ही सी बच्ची। फिर किस लिये वो जी हलकान करता? लेकिन ये फ़लक बे पीर... उसने उसे सुख से न बैठने दिया। इस नींद से बेदार करके उसे अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया। उसे बता दिया कि ज़िंदगी में सुख ही नहीं, आराम ही नहीं, दुख भी है। मेहनत और मशक़्क़त भी है!
पाँच साल हुए उसकी वही आराम देने वाली अज़ीज़ बीवी गुड़िया सी एक लड़की को छोड़कर इस जहान से रहलत कर गई। मरते वक़्त अपने सब सोज़ को अपनी फीकी और उदास आँखों में भर उसने बाक़र से कहा था, मेरी रज़िया अब तुम्हारे हवाले है, उसे तकलीफ़ न होने देना। और उसी एक फ़िक़रे ने बाक़र की तमाम ज़िंदगी के रुख को पलट दिया था। अपनी शरीक-ए-हयात की वफ़ात के बाद वो अपनी बेवा बहन को उसके गांव से ले आया था और अपनी आलस और ग़फ़लत को छोड़कर अपनी मरहूम बीवी की आख़िरी आरज़ू को पूरा करने में जी जान से मुनहमिक हो गया था।
ये मुम्किन भी कैसे था कि अपनी बीवी की, अपनी उस बीवी की जिसे वो रूह की गहराईयों के साथ मुहब्बत करता था, जिसकी मौत का ग़म उसके दिल के नामालूम पर्दों तक छा गया था, जिसके बाद उम्र होने पर भी, मज़हब की इजाज़त होने पर भी, रिश्तेदारों के मजबूर करने पर भी उसने दूसरी शादी न की थी... अपनी उसी बीवी की आख़िरी ख़्वाहिश को भुला देता।
वो दिन-रात जी तोड़ कर काम करता था। ताकि अपनी मरहूम बीवी की इस अमानत को, अपनी इस नन्ही सी गुड़िया को तरह तरह की चीज़ें लाकर दे सके। जब भी कभी वो मंडी से आता नन्ही रज़िया उसकी टांगों से लिपट जाती और अपनी बड़ी बड़ी आँखें उसके गर्द से अटे हुए चेहरे पर जमा कर पूछती, अब्बा, मेरे लिए क्या लाए हो! तो वो उसे अपनी गोद में ले लेता और कभी मिठाई और कभी खिलौनों से उसकी झोली भर देता। तब रज़िया उसकी गोद से उतर जाती और अपनी सहेलियों को अपनी मिठाई और खिलौने दिखाने के लिए भाग जाती... यही गुड़िया सी लड़की जब आठ बरस की हुई, तो एक दिन मचल कर अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा हम तो डाची लेंगे, अब्बा हमें डाची ले दो!
भोली मासूम लड़की! उसे क्या मालूम कि वो एक मुफ़्लिस और क़ल्लाश मज़दूर की लड़की है जिसके लिये सांडनी ख़रीदना तो कुजा उसका तसव्वुर करना भी गुनाह है। रूखी हंसी के साथ बाक़र ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, रोजू तू तो ख़ुद डाची है। पर रज़िया न मानी।
उस दिन मुशीर माल अपनी सांडनी पर चढ़ कर अपनी छोटी सी लड़की को आगे बिठाए इस काट (बीस पच्चीस झुग्गियों का गांव) में कुछ मज़दूर लेने आये थे। तभी रज़िया के नन्हे से दिल में डाची पर सवार होने की ज़बरदस्त ख़्वाहिश पैदा हो उठी थी और उसी दिन से बाक़र की रही सही ग़फ़लत भी दूर हो गई।
उसने रज़िया को टाल तो दिया था पर दिल ही दिल में उसने अह्द कर लिया था कि चाहे जो हो वो रज़िया के लिए एक ख़ूबसूरत डाची ज़रूर मोल लेगा और तब उसी इलाक़े में जहां उसकी आमदनी की औसत महीना भर में तीन आना रोज़ाना भी न होती थी वहीं अब आठ दस आने हो गई। दूर दूर के देहात में अब वो मज़दूरी के लिए जाता। कटाई और बिजाई के दिनों में दिन रात जान लड़ाता। फ़सल काटता, दाने निकालता, खलियानों में अनाज भरता, नीरा डाल कर कप बनाता, बिजाई के दिनों में हल चलता, पीलियां बनाता, निराई करता। उन दिनों में उसे पाँच आने से आठ आने तक रोज़ाना मज़दूरी मिल जाती। जब कोई काम न होता तो अलस्सुबह उठकर, आठ कोस की मंज़िल मार कर मंडी जा पहुंचता और आठ दस आने की मज़दूरी कर के ही वापस लौटता। उन दिनों में वो रोज़ छः आने बचाता आ रहा था। इस मामूल में उसने किसी तरह की ढील न आने दी थी। उसे जैसे जुनून सा हो गया था। बहन कहती, बाक़र, अब तो तुम बिल्कुल ही बदल गये हो, पहले तो कभी तुमने इस तरह जी तोड़ कर मेहनत न की थी।
बाक़र हँसता और कहता, तुम चाहती हो, मैं तमाम उम्र इसी तरह निठल्ला बैठा रहूं।
बहन कहती, निकम्मा बैठने को तो मैं नहीं कहती, लेकिन सेहत गंवा कर धन जमा करने की सलाह भी मैं नहीं दे सकती।
ऐसे वक़्त हमेशा बाक़र के सामने उसकी मरहूम बीवी की तस्वीर खिंच जाती। उसकी आख़िरी आरज़ू उसके कानों में गूंज जाती और वो सेहन में खेलती हुई रज़िया पर एक प्यार की नज़र डाल कर होंटों पर पुरसोज़ मुस्कुराहट लिए हुए फिर अपने काम में लग जाता और आज... आज डेढ़ साल की कड़ी मशक़्क़त के बाद वो मुद्दत से पाली हुई अपनी इस आरज़ू को पूरी कर सका था। सांडनी की रस्सी उसके हाथ में थी और सरकारी खाले (नहर की छोटी शाख़) के किनारे किनारे वो चला जा रहा था।
शाम का वक़्त था और मग़रिब में ग़ुरूब होते हुए आफ़ताब की किरनें धरती को सोने का आख़िरी दान दे रही थीं। हवा में कुछ ख़ुनकी आ गई थी और कहीं दूर... खेतों में टीटहरी टियाऊं टियाऊं कर के उड़ रही थी। बाक़र की निगाह तसव्वुर के सामने माज़ी के तमाम वाक़ियात एक एक कर के आ रहे थे। इधर-उधर से कोई किसान अपने ऊंट पर सवार जैसे फुदकता हुआ निकल जाता और कभी कभी खेतों से वापस आने वाले किसानों के लड़के छकड़े पर रखे हुए घास के गठों पर बैठे, बैलों को पुचकारते, किसी देहाती गीत का एक-आध बंद गाते या छकड़े के पीछे बंधे हुए ख़ामोशी से चले आने वाले ऊंटों की थूथनियों से खेलते चले आते थे।
बाक़र ने जैसे ख़्वाब से बेदार हो कर मग़रिब की तरफ़ ग़ुरूब हुए आफ़ताब को देखा और फिर सामने की तरफ़ वीराने में नज़र दौड़ाई। उसका गांव अभी बड़ी दूर था। मसर्रत से पीछे की तरफ़ देख और चुप-चाप चली आने वाली सांडनी को प्यार से पुचकार कर वो और भी तेज़ी से चलने लगा। कहीं उसके पहुंचने से पहले रज़िया सो न जाये इसी ख़्याल से।
मुशीर माल की काट नज़र आने लगी। यहां से उसका गांव नज़दीक ही था। यही कोई दो कोस! बाक़र की चाल धीमी हो गई और इसके साथ ही तसव्वुर की देवी अपनी रंग-बिरंगी कूची से उसके दिमाग़ के क़िरतास पर तरह तरह की तस्वीरें बनाने लगी। बाक़र ने देखा, उसके घर पहुंचते ही नन्ही रज़िया मसर्रत से नाच कर उसकी टांगों से लिपट गई है और फिर डाची को देखकर उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैरत और मसर्रत से भर गई हैं, फिर उसने देखा वो रज़िया को अपने आगे बिठाये सरकारी खाले के किनारे किनारे डाची पर भागा जा रहा है। शाम का वक़्त है। मस्त, ठंडी हवा चल रही है और कभी कभी कोई पहाड़ी कव्वा अपने बड़े बड़े परों को फैलाए अपनी मोटी आवाज़ से एक दोबार काएं काएं कर के ऊपर से उड़ता चला जाता है। रज़िया की ख़ुशी का वार-पार नहीं, वो जैसे हवाई जहाज़ में उड़ी जा रही है! फिर उस के सामने आया... वो रज़िया को ले बहावल नगर की मंडी में खड़ा है। नन्ही रज़िया जैसे भौंचक्की सी है। हैरान सी खड़ी वो हर तरफ़ अनाज के उन बड़े बड़े ढेरों को, ला-इंतिहा छकड़ों को और कार-ए-हैरत में गुम कर देने वाली उन बेशुमार चीज़ों को देख रही है। एक दूकान पर ग्रामोफोन बजने लगता है। लकड़ी के उस डिब्बे से किस तरह गाना निकल रहा है? कौन उसमें छुपा गा रहा है? ये सब बातें रज़िया की समझ में नहीं आतीं और ये सब जानने के लिए उसके दिल में जो इश्तियाक़ है, वो उस की आँखों से टपका पड़ता है।
अपने तसव्वुर की दुनिया में मह्व वह काट के पास गुज़रा जा रहा था कि अचानक कुछ ख़याल आ जाने से वो रुका और काट में दाख़िल हो गया। मुशीर माल की काट भी कोई बड़ा गांव न था। उधर के सब गांव ऐसे ही हैं। ज़्यादा हुए तो तीस छप्पर होंगे। कड़ियों की छत, क्या पक्की ईंटों का मकान अभी इस इलाक़े में नहीं। ख़ुद बाक़र की काट में पंद्रह घर थे। घर कहाँ सरकण्डों की झुग्गियां थीं। मुशीर माल की काट भी ऐसी ही बीस पच्चीस झुग्गियों की बस्ती थी। सिर्फ़ मुशीर माल का मकान कच्ची ईंटों से बना था। लेकिन छत उस पर भी सरकण्डों ही की थी। नानक बढ़ई की झुग्गी के सामने वो रुका। मंडी जाने से पहले वो उसके हाँ डाची का गदरा बनने के लिए दे गया था। उसे ख़याल आया कि अगर रज़िया ने डाची पर चढ़ने की ज़िद की तो वो उसे कैसे टाल सकेगा। इसी ख़याल से वो पीछे मुड़ आया था। उसने नानक को दो एक आवाज़ें दीं। अंदर से शायद उसकी बीवी ने जवाब दिया,
घर में नहीं मंडी गये हैं!
बाक़र की आधी ख़ुशी जाती रही। वो क्या करे? ये न सोच सका। नानक अगर मंडी गया है तो गदरा क्या ख़ाक बना कर गया होगा। लेकिन फिर उसने सोचा शायद बना कर रख गया हो। उसने फिर आवाज़ दी, मैं डाची का पालान बनाने दे गया था।
जवाब मिला, हमें नहीं मालूम!
बाक़र की सब ख़ुशी जाती रही। गदरे के बग़ैर वो डाची लेकर क्या जाये? नानक होता तो उसका पालान चाहे न बना सही, कोई दूसरा ही उससे मांग कर ले जाता। इस ख़याल के आते ही उसने सोचा चलो मुशीर माल से मांग लें। उनके तो इतने ऊंट रहते हैं कोई न कोई पुराना पालान होगा ही, अभी उसी से काम चला लेंगे। तब तक नानक नया गदरा तैयार कर देगा। ये सोच कर वो मुशीर माल के घर की तरफ़ चल पड़ा।
अपनी मुलाज़िमत के दौरान में मुशीर माल साहब ने काफ़ी दौलत जमा कर ली थी और जब इधर नहर निकली तो अपने असर-ओ-रसूख़ से रियासत ही की ज़मीन में कौड़ियों के मोल कई मुरब्बे ज़मीन हासिल कर ली थी। अब रिटायर हो कर यहीं आ रहे थे। राहक (मुज़ारे) रखे हुए थे। आमदनी ख़ूब थी और मज़े से बसर हो रही थी। अपनी चौपाल पर एक तख़्त पर बैठे हुक़्क़ा पी रहे थे। सर पर सफ़ेद साफा, गले में सफ़ेद क़मीस, उस पर सफ़ेद जाकिट, और कमर में दूध जैसा सफ़ेद तह बंद। गर्द से अटे हुए बाक़र को सांडनी की रस्सी थामे आते देखकर उन्होंने पूछा, कहो बाक़र, किधर से आ रहे हो?
बाक़र ने झुक कर सलाम करते हुए कहा, मंडी से आ रहा हूँ मालिक!
ये डाची किस की है?
मेरी ही है मालिक, अभी मंडी से ला रहा हूँ।
कितने को लाए हो?
बाक़र ने चाहा, कह दे, आठ बीसी को लाया हूँ, उसके ख़याल में ऐसी ख़ूबसूरत डाची दो सौ में भी सस्ती थी, पर दिल न माना। बोला, हुज़ूर मांगता तो 160 था। पर सात बीसी ही को ले आया हूँ।
मुशीर माल ने एक नज़र डाची पर डाली। वो ख़ुद देर से एक ख़ूबसूरत सी डाची अपनी सवारी के लिए लेना चाहते थे। उनके डाची तो थी पर गुज़श्ता साल उसे सीमक हो गया था और अगरचे नील- वगैरह देने से उसका रोग तो दूर हो गया था। पर उसकी चाल में वो मस्ती वो लचक न रही थी। ये डाची उनकी नज़र में जच गई। क्या सुडौल और मुतनासिब आज़ा हैं, क्या सफ़ेदी माइल भूरा भूरा रंग है, क्या लचलचाती लंबी गर्दन है! बोले, चलो हमसे आठ बीसी ले लो। हमें एक डाची की ज़रूरत भी है। दस तुम्हारी मेहनत के रहे।
बाक़र ने फीकी हंसी के साथ कहा, हुज़ूर अभी तो मेरा चाव भी पूरा नहीं हुआ।
मुशीर माल उठकर डाची की गर्दन पर हाथ फेरने लगे थे। वाह क्या असील जानवर है! बज़ाहिर बोले, चलो पाँच और ले लेना। और उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, नूरे, अबे ओ नूरे!
नौकर नौहरे में बैठा भैंसों के लिए पट्ठे कुतर रहा था। गडासा हाथ ही में लिये हुए भागा आया। मुशीर माल ने कहा, ये डाची ले जाकर बांध दो! 165 में, कहो कैसी है?
नूरे ने हैरान से खड़े बाक़र के हाथ से रस्सी ले ली और सर से पांव तक एक नज़र डाची पर डाल कर बोला, ख़ूब जानवर है। और ये कह कर नौहरे की तरफ़ चल पड़ा।
तब मुशीर माल ने अंटी से साठ रुपये के नोट निकाल कर बाक़र के हाथ में देते हुए मुस्कुरा कर कहा, अभी ये रखो, बाक़ी भी एक दो महीने तक पहुंचा दूँगा। हो सकता है तुम्हारी क़िस्मत के पहले ही आ जाएं। और बग़ैर कोई जवाब सुने वो नोहरे की तरफ़ चल पड़े। नूरा फिर चारा कतरने लगा था। दूर ही से आवाज़ देकर उन्होंने कहा, भैंस का चारा रहने दे, पहले डाची के लिए ग्वारे का नीरा कर डाल, भूकी मालूम होती है।
और पास जा कर सांडनी की गर्दन सहलाने लगे।
कृष्ण पक्ष का चांद अभी तुलू’ नहीं हुआ था। वीराने में चारों तरफ़ कुहासा छाया हुआ था। सर पर दो एक तारे झाँकने लगे थे। बबूल और उकान्हा के दरख़्त बड़े बड़े स्याह धब्बे बन रहे थे। साठ रुपये के नोटों को हाथ में लटकाए अपने घर से ज़रा फ़ासिले पर एक झाड़ी की ओट में बैठा बाक़र उस मद्धम टिमटिमाती रौशनी की शुआ को देख रहा था जो सरकण्डों से छनछन कर उसके घर के आँगन से आ रही थी। जानता था रज़िया जाग रही होगी। उस का इंतिज़ार कर रही होगी और वो ये सोच रहा था कि रौशनी बुझ जाये, रज़िया सो जाये तो वो चुप-चाप घर में दाख़िल हो!
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.