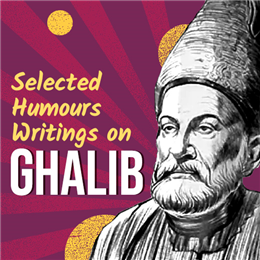ग़ालिब फिर इस दुनिया में
जब मैं इस दुनिया में था तो मैंने बेचैन हो कर एक बार कहा था,
मौत का एक दिन मुअय्यन है
नींद क्यों रात-भर नहीं आती
आज मौत की नींद फिर उचट गई। क्या नींद, क्या मौत, दोनों में किसी का एितबार नहीं, जब ज़िन्दा थे तो ज़िन्दगी का रोना था और मौत की तमन्ना थी, मैंने कहा था,
क़ैद-ए-हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज
शम्अ हर रंग में जलती है सहर होते तक
शम्मा और सहर का क्या ज़िक्र है, मैंने तो खुली खुली बात कह दी थी। हाँ एक और शेर याद आ गया,
किससे महरूमी-ए-क़िस्मत की शिकायत कीजे
हमने चाहा था कि मर जाएँ सो वो भी न हुआ
लेकिन ज़ौक़ ने इससे भी लगती हुई बात कही थी। वो न जाने ये शेर कैसे कह गए थे,
अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएँगे
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएँगे
हाँ, तो मैं कहाँ हूँ, अभी मेरे हवास दुरुस्त नहीं, लेकिन ये ज़मीन और ये आसमान तो कुछ जाने बूझे मालूम होते हैं। लोगों को एक तरफ़ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मैं भी उन्हीं के साथ हो लूँ... “पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं...” अब इन रास्तों पर पालकियाँ जाती हुई नज़र नहीं आतीं, घोड़ा गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन उनकी शक्ल-ओ-सूरत बिल्कुल बदली हुई है। आँखों के सामने से बीसियों ऐसी गाड़ियाँ भी गुज़र गईं, जिनमें कोई जानवर जुता हुआ नहीं था। सुन रहा हूँ कि लोग उन्हें मोटर कार कहते हैं। इन कल पुर्ज़ों से चलने वाली गाड़ियों में तेज़ी और भड़क तो बहुत है लेकिन पुरानी सवारियों की सी बात उनमें कहाँ?
ख़ैर ये तो होना था। आज से न जाने कितने बरस पहले जब मैं इस दुनिया में था, तब ही ज़माना करवट बदल चुका था। ये काया पलट आँखों के लिए नई चीज़ है और दिल-ओ-दिमाग़ को भी हैरत में डाल दे लेकिन मेरी आँखों ने तो उस वक़्त पिछली ज़िन्दगी पाई थी। वो इंक़िलाबात देखे थे कि अब क्या कहूँ, हैरत क्या करूँ और किस बात पर करूँ। बचपन और जवानी में क़िला के रंग-ढंग को देखा था। मुग़ल दरबार की झिलमिलाती हुई शम्अ “दाग़-ए-फ़िराक़ सोहबत-ए-शब की जली हुई” फिर भी एक नया रंग पैदा कर रही थी। शह्र के शरीफ़ों और रईसों की ज़िंदगियाँ देखी थीं। दूर दूर तक का सफ़र घोड़ों पर, बहेलियों पर, पालकियों पर और डाक गाड़ियों पर तय किया था। फिर 1857 का ग़दर हुआ, ग़दर क्या हुआ क़यामत आ गई। इसके बाद पिछली ही ज़िन्दगी में रेल की सवारी पर दिल्ली से कलकत्ता का लम्बा सफ़र पूरा किया, मालूम नहीं कलकत्ता की शान अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी। उस वक़्त ये शह्र दुल्हन बना हुआ था जिसकी याद से अब भी तड़प उठता हूँ।
कलकत्ते का जो ज़िक्र किया तूने हमनशीं
इक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय
और यूँ तो न कुछ रौनक़ में रखा है न उजड़ी हालत में रखा है। न आबादी में न वीराने में फिर भी जो कुछ है और जैसा कुछ है ग़नीमत है।
नग़मा हाय ग़म को भी ऐ दिल ग़नीमत जानिए
बेसदा हो जाएगा ये साज़-ए-हस्ती एक दिन
इंसान जब ज़िन्दगी की मुसीबतों से परेशान हो जाता है तो उसे दुनिया छोड़ने की सूझती है। अपने को धोका देने और ग़लत रास्ते पर चलने को अक्सर लोग ख़ुदा की तलाश या सच्चाई का पा जाना समझते हैं। लेकिन इस सच्चाई की भी सच्चाई मुझे मालूम है।
हाँ अह्ल-ए-तलब कौन सुने ताना-ए-ना याफ़्त
जब पा न सके उसको तो आप अपने को खो आए
दुनिया को छोड़कर तो पैग़म्बरी भी कुछ नहीं होता।
वो ज़िन्दा हम हैं कि हैं रू-शनास-ए-ख़ल्क़ ऐ ख़िज़्र
न तुम कि चोर बने उम्र-ए-जावेदाँ के लिए
मैं अपने ख़यालात की धुन में कहाँ निकल आया। ये तमाम चीज़ें, ये मकानात और ये आबादी नई भी मालूम होती है और पुरानी भी, अजनबी भी और मानूस भी। वो सामने धुँदलके में लाल क़िला नज़र आ रहा है, कुछ दूर पर जामा मस्जिद के बुर्ज और मीनार नज़र आ रहे हैं। मैं दिल्ली ही में हूँ। हाय दिल्ली वाय दिल्ली! इस बाज़ार की शान तो देखने की चीज़ है। चाँदनी चौक अच्छा ये वही पुराना चाँदनी चौक है जो बार-बार लुटा और बार-बार आबाद हुआ। उजड़ा और बसा। इसका नाम तक नहीं बदला। यहाँ तो नई ज़िन्दगी के शोर-ओ-पुकार में भी, यहाँ की नई आवाज़ों में भी पुराने नाम कान में पड़ रहे हैं, कूचा चेलाँ, कूचा-ए-बल्लीमारान, इन दो मोहल्लों में बरसों मेरा क़याम रहा है। बहार आती है और चली जाती है लेकिन बाग़ वही रहता है। इस बाज़ार में इस दूसरी दुनिया से पलट कर क्या ख़रीदें। जब ज़िन्दा थे तभी ये हाल था कि,
दिरम-ओ-दाम अपने पास कहाँ
चील के घोंसले में मास कहाँ
लेकिन इस तरफ़ कुछ किताबें बेचने वालों की दुकानें हैं। किताबों की दुनिया मुर्दों और ज़िंदों दोनों के बीच की दुनिया है। यहाँ हर शख़्स कह सकता है कि “हम भी इक अपनी हवा बाँधते हैं।” चलें ज़रा किताबों की इस ख़याली दुनिया की सैर करें। वो एक तरफ़ अलमारी में कोई निहायत अच्छी और क़ीमती किताब रखी हुई है। जिल्द तो देखो कैसी ख़ूबसूरत है। सुनहरे हर्फ़ों से कुछ लिखा हुआ भी है। उसके बराबर छोटी छोटी किताबें देखने में कैसी भली मालूम होती हैं। अरे भई ज़रा ये सामने लगी हुई किताबें तो उठा देना, वही जो सामने के तख़्ते पर अलमारी में लगी हुई हैं। छपाई और लिखाई के ये खेल पहले कभी नहीं देखे थे, दीवान-ए-ग़ालिब, दीवान-ए-ग़ालिब, दीवान-ए-ग़ालिब, मुरक़्क़ा-ए-चुग़ताई! मेरी आँखें ये क्या देख रही हैं। बर्लिन और हिन्दोस्तान के कई शह्रों से ये किताबें निकली हैं।
क्यों भई, ज़ौक़ और मोमिन, नासिख़ और आतिश, मीर और सौदा ये सब के सब ग़ालिब से ज़ियादा मशहूर थे। उनके कलाम तो और ठाट से छपे होंगे ज़रा उन्हें भी देखूँ। क्या कहा? सिर्फ़ ग़ालिब के दीवान इस एहतिमाम से निकले हैं। फिर क्या कहा? आज ग़ालिब की कही हुई बातों का सारे हिन्दोस्तान में शोर है, ग़ालिब पर किताबें और ग़ालिब पर मज़ामीन कसरत से निकल रहे हैं। अच्छा ये कहना भी किसी डॉक्टर बिजनौरी का मुल्क में मशहूर है कि हिन्दोस्तान की दो बड़ी किताबें हैं एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान-ए- ग़ालिब, तो सिर्फ़ रहना सहना ही इस मुल्क का नहीं बदला बल्कि मज़ाक़-ए-शाइरी की भी काया पलट गई है। हाँ, अब आप दूसरे ग्राहकों की तरफ़ मुतवज्जाे हों। शुक्रिया, अब मैं अपने इस शेर को क्या कहूँ,
हूँ ख़िफ़ाई के मुक़ाबिल मैं ज़ुहूरी ग़ालिब
मेरे दावे पे ये हुज्जत है कि मशहूर नहीं
पहली ज़िन्दगी में दूसरों की शोहरत के खेल देखे थे। मरने के बाद अपनी शोहरत के खेल देख रहा हूँ। वो ज़िन्दगी की छेड़ थी ये मौत की है।
पूछते हैं वो कि ग़ालिब कौन है
कोई बतलाओ कि हम बतलाएँ क्या
हमने माना कि कुछ नहीं ग़ालिब
मुफ़्त हाथ आए तो बुरा क्या है
इस मुरक़्क़ा-ए-चुग़ताई को क्या कहूँ ,अगर मेरे अशआर तस्वीर के नीचे न लिखे होते तो मैं भी उन तस्वीरों को न समझता। ख़ैर, तो उन लकीरों और रंगों से मेरे शेरों का मतलब समझाया गया है। न दीवान-ए-ग़ालिब होता न तस्वीर बनाने वाला अपना यह कमाल दिखा सकता।
खुलता किसी पे क्यों िमरे दिल का मुआमला
शेरों के इन्तिख़ाब ने रुसवा किया मुझे
बहर-हाल ग़ज़ल के मतलब को तस्वीर के पर्दों से ज़ाहिर करने की अदा को मैं कुछ समझा कुछ नहीं समझा। ज़ियादा-तर तस्वीरें बेलिबास हैं।
शौक़ हर रंग रक़ीब-ए-सर-ओ-सामाँ निकला
क़ैस तस्वीर के पर्दे में भी उर्यां निकला
ख़ैर इतना तो हुआ कि “चन्द तस्वीर-ए-बुताँ चन्द हसीनों के ख़ुतूत” एक जगह कर दिए गए। हसीनों के ख़त यानी उनकी शोख़ तबीअत, उनके चंचल मिज़ाज की वो तस्वीरें जो मेरे अक्सर अशआर में अक्सर दिखाई देती हैं, और यूँ तो हसीनों के ख़ुतूत भी मालूम।
क़ासिद के आते आते ख़त इक और लिख रखूँ
मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में
ख़ैर मशहूर हुए तो क्या और न हुए तो क्या। मेरा वो फ़ारसी कलाम जिसका हिन्दोस्तान में जवाब नहीं था वो इस दुकान में नज़र नहीं आता। मेरे चन्द अशआर से अगले वक़्तों के लोगों को और मुमकिन है आजकल के लोगों को भी ये धोका हो कि मैंने अपनी शोहरत की सारी वज्ह अपने फ़ारसी कलाम को जानता था और उर्दू की बड़ाई को मैं नहीं समझा था। ये एक मज़ेदार धोका है। उर्दू आगे बढ़कर क्या कुछ होने वाली थी उसकी झलक मैं देख चुका था। मेरे उर्दू कलाम के चन्द शेर जिनमें फ़ारसी ज़ियादा थी, लोग ले उड़े थे और ये न देख सके थे कि मैंने ग़ज़ल को कितनी चंचल, कितनी टकसाली, कितनी चुटीली, कितनी जीती-जागती, बोलती-चालती चीज़ बना दिया था। अगर मैं उर्दू की अहमियत को न समझता तो अपने उन ख़ुतूत को जिनमें मैंने चिट्ठी को बातचीत बना दिया था, इस एहतियात और इस एहतिमाम से बचाकर न रखता, क़रीब क़रीब सबसे छोटा उर्दू दीवान मैंने छोड़ा था और मुझे यक़ीन था कि सबसे ज़ियादा मेरे ही अशआर लोगों की ज़बान पर होंगे।
अब यहाँ मुझे बहुत देर हो चुकी। किताब बेचने वाला भी अपने दिल में क्या कहता होगा। ये एक अख़बार रखा हुआ है। क्यों भई इस पर आज ही की तारीख़ है ना? अच्छा तो आज 23 जून 38 ई. है मुझे कुछ याद आता है कि मैं 1869 तक ज़िन्दा था। उसके बाद दूसरी दुनिया की ज़िन्दगी थी और उसमें माह-ओ-साल कहाँ, आज इस दुनिया से गए हुए सत्तर बरस होने को आए। इतने बड़े और तवील अरसे में महज़ अपनी शोहरत और कामयाबी का हाल जान कर ख़ैर, एक तरह ख़ुश तो हूँ लेकिन ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि हिन्दोस्तान में अब कैसी शाइरी हो रही है। कोई कुतुबख़ाना तो पास होगा। लोग किसी हार्डिंग लाइब्रेरी का पता दे रहे हैं। अच्छा देखूँ, यहाँ क्या दाग़, अमीर, हाली, अकबर, इक़बाल, हसरत मोहानी, जिगर, असग़र, शाद अज़ीम आबादी, अज़ीज़, जोश और दूसरे शोअरा के मजमूए नज़र आ रहे हैं। उनमें दाग़ और अमीर को तो मैं पिछली ज़िन्दगी ही में जानता था। हाली तो मेरे सबसे होनहार शागिर्दों में थे।
अकबर से बीसियों बरस पहले उस दूसरी दुनिया में मिला था जहाँ से ख़ुद आया हूँ और जहाँ तमाम मरे हुए शोअरा के साथ ये सब बज़्म-ए-सुख़न की रौनक़ बन गए हैं। वहाँ अकबर का साथ छोड़ने को तो जी नहीं चाहता था और इक़बाल तो अभी अभी वहाँ पहुँचे हैं। उस शख़्स की शोहरत वहाँ बरसों पहले पहुँच चुकी थी और फ़रिश्तों की ज़बान पर इक़बाल के नग़मे बरसों पहले से थे। मैंने उर्दू में जिस तरह की शाइरी की दाग़ बेल डाली थी, शाइरी को जो अज़मत देना चाही थी, मेरी ये कोशिश इक़बाल ही के हाथों परवान चढ़ी। हसरत मोहानी का कलाम देखा। मोमिन, जुरअत, मुसहफ़ी का नाम उस कलाम से चमक गया। जिगर, असग़र, शाद, अज़ीज़, चकबस्त और सुरूर जहानाबादी उन सबकी शाइरी अपनी अपनी जगह ऊँची है लेकिन कहीं कहीं रोक-थाम और गहरी नज़र की ज़रूरत मालूम होती है। देखूँ ये यास यगाना कौन शख़्स है और इसकी आयात-ए-विज्दानी में क्या है। शेर तो जानदार हैं। बयान का तरीक़ा भी कहीं कहीं उस्तादाना है। आतिश की गर्मागर्मी और तेज़ी भी मिल जाती है लेकिन ग़ालिब का नाम उस शख़्स पर भूत की तरह सवार है। ख़ैर... “वो कहें और सुना करे कोई”... मिर्ज़ा क़तील की याद ताज़ा हो गई। ग़ालिब न जाने कितने शाइरों की दुखती हुई रग है। मैं उर्दू में मुसलसल नज़्म की तरक़्क़ी देखकर ख़ुश हूँ।
ब-क़द्र-ए-शौक़ नहीं ज़र्फ़-ए-तंगना-ए-ग़ज़ल
कुछ और चाहिए वुसअत मिरे बयाँ के लिए
ग़ज़ल हो या नज़्म, संजीदगी, मज़ाक़ की पाकीज़गी और गिरी हुई बातों से बचना भी वो खूबियाँ हैं जो शाइरी को पैग़म्बरी का दर्जा दे देती हैं। हाँ, कुछ अजीब और ग़लत बातें भी मेरे बाद की शाइरी में नज़र आती हैं। एक साहब ग़ालिब की जा-नशीनी का दावा यूँ करते हैं कि जिस तरह मीर के सत्तासी बरस के बाद ग़ालिब का ज़माना आया, उसी तरह ग़ालिब के सत्तासी बरस बाद वो पैदा हुए हालाँकि हर वक़्त और मेरे ज़माने के सत्तासी बरस के बाद भी बेवक़ूफ़ दुनिया में पैदा हो सकते हैं। अपने कुछ अच्छे कुछ बुरे अशआर को लोग इल्हाम भी बताने लगे हैं। अपनी ग़लत और बेढंगी नक़्क़ाली भी देखता हूँ, बहुत हो रही है। मोहमल फ़ारसी तरकीबें, एक रस्मी क़िस्म की मुश्किल-पसन्दी, लफ़्ज़-परस्ती और शेरियत से मुअर्रा बुलन्द-आहंगी और इज़हार-ए-इल्मियत यहाँ तक कि ग़ैर मौज़ूँ कलाम को भी शाइरी बताना ये सब बातें भी आजकल के शोअरा में आ गई हैं।
मैं उर्दू नस्र और उर्दू रिसालों और अख़बारों की कसरत और आब-ओ-ताब को देखकर भी ख़ुश हूँ। रुक़आत-ए-ग़ालिब गोया इस बात की पेशेनगोई थे। ये सब सही लेकिन दिल्ली की पिछली सोहबतें याद आ गईं और दिल को तड़पा गईं। अब न ज़ौक़ हैं न मोमिन, न शेफ़्ता न दाग़, न हाली न मजरूह, न अनवर। ख़ैर, शेर-ओ-शाइरी ही तो सारी ज़िन्दगी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि ये मुल्क फिर जाग रहा है। इसकी तमाम क़ौमें मिलकर एक नई ज़िन्दगी पैदा करने की कोशिश में हैं। अपना शेर मुझे याद आया।
हम मुवह्हिद हैं हमारा केश है तर्क-ए-रूसूम
मिल्लतें जब मिट गईं अज्ज़ा-ए-ईमाँ हो गईं
मेरी नज़रें ये भी देख कर ख़ुश हैं कि अंग्रेज़ों की तहज़ीब, उनके इल्म-ओ-फ़न से फ़ायदा उठाते हुए भी हिन्दोस्तान अपनी तहज़ीब को फिर से ज़िन्दा करना चाहता है।
लाज़िम नहीं कि ख़िज़्र की हम पैरवी करें
माना कि इक बुज़ुर्ग हमें हम सफ़र मिले
अब शाम हो रही है। मैं सिर्फ़ एक पल के लिए इस दुनिया में आया था। शायद मुझे आए अभी कुछ वक़्त नहीं हुआ, और पल मारते मैंने सब कुछ देख लिया। दूसरी दुनिया का एक पल इस दुनिया की एक सदी के बराबर होता है। हम अह्ले अदम एक पल में जो कुछ देख लेते हैं दुनिया में उसके लिए एक उम्र चाहिए। अब न वो दिल्ली है न सत्तर बरस पहले का ज़माना, न मिर्ज़ा हरगोपाल तफ़्ता हैं कि इस बेसर-ओ-सामआनी में मेरी प्यास बुझाएँ। अब तो क़र्ज़ की भी नहीं पी सकते। अख़बारों से ये भी मालूम हुआ कि अब शराब इस मुल्क में बन्द होने वाली है।
मय ब-ज़ुहाद मकुन अर्ज़ कि ईं जौहर-ए-नाब
पेश-ए-ईं क़ौम ब-शोराबा-ए-ज़मज़म न रसद
हिन्दुस्तान बहुत बदल चुका है लेकिन अगले वक़्तों के लोग, मालूम होता है अभी बाक़ी हैं।
अगले वक़्तों के हैं ये लोग उन्हें कुछ न कहो
जो मय-ओ-नग़मा को अन्दोह-रुबा कहते हैं
ख़ैर शराब से निशात और ख़ुशी किस काफ़िर को दरकार है।
“यक-गोना बेख़ुदी मुझे दिन रात चाहिए।” और वो बेख़ुदी मुझ पर छा चुकी है। दुनिया के हुस्न के करिश्मे देख चुका। मैं इस तमाशे को क़यामत कहता हूँ। मैं ख़ाक हो चुका था।
ब-जुज़ परवाज़-ए-शौक़-ए-नाज़ क्या बाक़ी रहा होगा
क़यामत एक हवा-ए-तुन्द है ख़ाक-ए-शहीदाँ पर
फिर आँख खुल गई।
हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी
कुछ हमारी ख़बर नहीं आती
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.