सिब्ग़े एंड संस (सोदागरान-ओ-नाशिरान-ए-कुतुब)
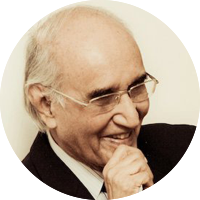
सिब्ग़े एंड संस (सोदागरान-ओ-नाशिरान-ए-कुतुब)
मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी
MORE BYमुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी
यह उस पुरउम्मीद ज़माने का ज़िक्र है जब उन्हें किताबों की दुकान खोले और डेल कार्नेगी पढ़े दो-तीन महीने हुए होंगे और जब उनके होंटों पर हर वक़्त वो धुली मंझी मुस्कुराहट खेलती रहती थी, जो आजकल सिर्फ़ टूथपेस्ट के इश्तिहारों में नज़र आती है। उस ज़माने में उनकी बातों में वो उड़ कर लगने वाला जोश और वलवला था जो बिलउमूम अंजाम से बेख़बर सट्टे बाज़ों और नौ मुस्लिमों से मंसूब किया है।
दुकान क्या थी, किसी बिगड़े हुए रईस की लाइब्रेरी थी। मालूम होता था कि उन्होंने चुन-चुन कर वही किताबें दुकान में रखी हैं, जो ख़ुद उनको पसंद थीं और जिनके मुताल्लिक़ उन्होंने हर तरह अपना इत्मीनान कर लिया था कि बाज़ार में उनकी कोई मांग है न खपत।
हमारे दोस्त मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने दुकान में क़दम रखते ही अपनी तमाम नापसंदीदा किताबें इस ख़ुशसलीक़गी से यकजा देखीं तो एक दफ़ा अपनी पुरानी ऐनक पर एतबार नहीं आया और जब एतबार आगया तो उल्टा प्यार आने लगा। अपने मख़सूस खट मिट्ठे लहजे में बोले, “यार! अगर आम पसंद की भी दो-चार किताबें रख लेते तो गाहक दुकान से इस तरह न जाते जैसे सिकन्दर दुनिया से गया था दोनों हाथ ख़ाली!”
ताजिराना तबस्सुम के बाद फ़रमाया, “मैं सिर्फ़ मेयारी किताबें बेचता हूँ।”
पूछा, “मेयारी की क्या पहचान?”
इरशाद हुआ, “सुनो, मेरे एक क़रीबी हमसाये हैं। प्रोफ़ेसर क़ाज़ी अबदुल क़ुद्दूस, चौबीस घंटे किताबों में जुटे रहते हैं। लिहाज़ा मैंने किया ये कि दुकान खोलने से पहले उनसे उनकी अपनी पसंदीदा किताबों की मुकम्मल फ़ेहरिस्त बनवा ली। फिर उन किताबों को छोड़कर उर्दू की बक़ीया तमाम किताबें ख़रीद के दुकान में सजा दीं। इससे बेहतर इंतिख़ाब कोई कर के दिखा दे।”
फिर एका एकी ताजिराना लहजा बना कर सेग़-ए-जमा में हुंकारे, “हमारी किताबें उर्दू अदब की आबरू हैं।”
“और हम ये बहुत अर्ज़ां बेचते हैं!” मिर्ज़ा ने उसी लहजे में जुमला पूरा किया।
मुसीबत ये थी कि हर किताब, हर मुसन्निफ़ के मुताल्लिक़ उनकी अपनी राय थी। बेलाग और अटल, जिसका इज़हार-ओ-ऐलान बिलजब्र-ओ-बमंज़िला दीनी फ़र्ज़ समझते थे। चुनांचे बारहा ऐसा हुआ कि उन्होंने गाहक को किताब ख़रीदने से जबरन बाज़ रखा कि इससे उसका अदबी ज़ौक़ ख़राब तर होने का अंदेशा था। सच तो ये है कि वो कुतुबफ़रोश कम और कुतुबनुमा ज़्यादा थे।
कभी कोई ख़रीदार हल्की फुल्की किताब मांग बैठता तो बड़ी शफ़क़त से जवाब देते, “यहां से दो गलियाँ छोड़कर सीधे हाथ को मुड़ जाईए। परले नुक्कड़ पर चूड़ियों की दुकान के पास एक लेटरबाक्स नज़र आएगा। उसके ठीक सामने जो ऊंची सी दुकान है बच्चों की किताबें वहीं मिलती हैं।”
एक मर्तबा का वाक़िया अब तक याद है कि एक साहिब कुल्लियात-ए-मोमिन पूछते हुए आए और चंद मिनट बाद मौलवी मुहम्मद इस्माईल मेरठी मरहूम की नज़्मों का गुलदस्ता हाथ में लिए उनकी दुकान से निकले।
एक दिन मैंने पूछा, अख़तर शीरानी की किताबें क्यों नहीं रखते?
मुस्कुराए, फ़रमाया, वो नाबालिग़ शायर है। मैं समझा शायद Minor poet का वो यही मतलब समझते हैं। मेरी हैरानी देखकर ख़ुद ही वज़ाहत फ़रमा दी कि वो वस्ल की इस तौर पर फ़र्माइश करता है गोया कोई बच्चा टॉफ़ी मांग रहा है।
इस पर मैंने अपने एक महबूब शायर का नाम लेकर कहा कि बेचारे होश ख़लीज आबादी ने क्या ख़ता की है? उनके मजमुए भी नज़र नहीं आते।
इरशाद हुआ कि उस ज़ालिम के तकाज़ाए वस्ल के ये तेवर हैं गोया कोई काबुली पठान डाँट डाँट कर डूबी हुई रक़म वसूल कर रहा है।
मैंने कहा मगर वो ज़बान के बादशाह हैं।
बोले, ठीक कहते हो। ज़बान उनके घर की लौंडी है और वो उसके साथ वैसा ही सुलूक करते हैं!
आजिज़ हो कर मैंने कहा अच्छा यूँही सही, मगर फ़ानी बदायूनी क्यों ग़ायब हैं? फ़रमाया, हश! वो निरे मुसव्विर-ए-ग़म हैं।
मैंने कहा, बजा मगर मेहदी-उल-अफ़ादी तो कामिल इंशा पर्दाज़ हैं।
बोले, छोड़ो भी फ़ानी मुसव्विर-ए-ग़म हैं तो मेहदी मुसव्विर-ए-बिंत-ए-ग़म। वल्लाह वो इन्शाईया नहीं, निसाईया लिखते हैं।
बिलआख़िर मैंने एक जाने-पहचाने प्रोफ़ेसर नक़्क़ाद का नाम लिया, मगर पता चला कि उन्होंने अपने कानों से फ़ाज़िल प्रोफ़ेसर के वालिद बुजु़र्गवार को लखनऊ को नखलऊ और मिज़ाजे शरीफ़ को मजाज़ शरीफ़ कहते सुना था। चुनांचे इस पिदराना नाअहली की बिना पर उनके तन्क़ीदी मज़ामीन दुकान में कभी बार न पा सके। यही नहीं ख़ुद प्रोफ़ेसर मौसूफ़ ने एक महफ़िल में उनके सामने ग़ालिब का एक मशहूर शे’र ग़लत पढ़ा और दोहरे हो हो कर दाद वसूल की, सो अलग!
मैंने कहा, इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है? बोले, फ़र्क़ की एक ही रही मीरन साहिब का क़िस्सा भूल गए? किसी ने उनके सामने ग़ालिब का शे’र ग़लत पढ़ दिया, तेवरियाँ चढ़ा कर बोले, मियां ये कोई क़ुरआन-ओ-हदीस है। जैसे चाहा पढ़ दिया।
आपने मुलाहिज़ा फ़रमा लिया कि बहुत सी किताबें वो इसलिए नहीं रखते थे कि उनको सख़्त नापसंद थीं और उनके मुसन्निफ़ीन से वो किसी न किसी मौज़ू पर ज़ाती इख़्तिलाफ़ रखते थे लेकिन मादूद-ए-चंद मुसन्निफ़ीन जो उस मातूब-ओ-मग़ज़ूब ज़ुमरे से ख़ारिज थे, उनकी किताबें दुकान में रखते ज़रूर थे, मगर कोशिश यही होती कि किसी तरह बिकने न पाएं, क्योंकि वो उन्हें बेहद पसंद थीं और उन्हें संगवा संगवा कर रखने में अजीब रुहानी लज़्ज़त महसूस करते थे। पसंद-ओ-नापसंद की इस ग़ैर ताजिराना कशाकश का नतीजा ये निकला कि, कुतुब अज़ जा न जज़्बा।
सुनी-सुनाई नहीं कहता। मैंने अपनी आँखों से देखा कि दीवान-ए-ग़ालिब (मुसव्विर) दुकान में महीनों पड़ा रहा। महज़ इस वजह से कि उनका ख़्याल था कि दुकान उसके बग़ैर सूनी सूनी मालूम होगी। मिर्ज़ा कहा करते थे कि उनकी मिसाल उस बदनसीब क़स्साब की सी है, जिसे बकरों से इश्क़ हो जाये।
किताबों से इशक़ का ये हाल था कि ऐन बोहनी और बिक्री के औक़ात में भी मुताले में कमर कमर ग़र्क़ रहते। ये कमर कमर की क़ैद इसलिए लगाना पड़ी कि हमने आज तक उन्हें कोई किताब पूरी पढ़ते नहीं देखा।
मिर्ज़ा इसी बात को यूं कहते थे कि बहुत कम किताबें ऐसी है जो अपने को उनसे पढ़वा सकी हैं। यही नहीं, अपने मुताले की तकनीक के मुताबिक़ रुमानवी और जासूसी उनको हमेशा उल्टा यानी आख़िर से पढ़ते ताकि हीरोइन का हश्र और क़ातिल का नाम फ़ौरन मालूम हो जाये।
उनका क़ौल है कि मेयारी नॉवेल वही है जो इस तरह पढ़ने पर भी आख़िर से शुरू तक दिलचस्प हो। हर कहीं से दो तीन सफ़े उलट-पलट कर पूरी किताब के मुताल्लिक़ बेदरेग़ राय क़ायम कर लेना और फिर उसे मनवाना उनके बाएं हाथ का खेल था।
बाज़-औक़ात तो लिखाई छपाई देखकर ही सारी किताब का मज़मून भाँप लेते। मुझे याद है कि उर्दू की एक ताज़ा छपी हुई किताब का काग़ज़ और रोशनाई सूंघ कर न सिर्फ़ उसे पढ़ने बल्कि दुकान में रखने से भी इनकार कर दिया। उनके दुश्मनों ने उड़ा रखी थी कि वो किताब का सर-ए-वर्क़ पढ़ते पढ़ते ऊँघने लगते हैं और इस आलम-ए-कशफ़ में जो कुछ दिमाग़ में आता है, उसको मुसन्निफ़ से मंसूब करके हमेशा हमेशा के लिए उससे बेज़ार होजाते हैं।
और मुसन्निफ़ ग़रीब किस शुमार-क़तार में हैं। अपने अदबी क़ियास-ओ-कियाफ़े का ज़िक्र करते हुए एक दिन यहां तक डिंग मारने लगे कि मैं आदमी की चाल से बता सकता हूँ कि वो किस क़िस्म की किताबें पढ़ता रहा है।
इत्तफ़ाक़ से उस वक़्त एक भरे भरे पछाए वाली लड़की दुकान के सामने से गुज़री। चीनी क़मीज़ उसके बदन पर चुस्त फ़िक़रे की तरह कसी हुई थी। सर पर एक रिबन सलीक़े से ओढ़े हुए जिसे मैं ही क्या, कोई भी शरीफ़ आदमी, दुपट्टा नहीं कह सकता, इसलिए कि दुपट्टा कभी इतना भला मालूम नहीं होता।
तंग मोरी और तंग तर घेर की शलवार। चाल अगरचे कड़ी कमान का तीर न थी, लेकिन कहीं ज़्यादा महक। कमान कितनी भी उतरी हुई क्यों न हो, तीर ला-मुहाला सीधा ही आएगा। ठुमक ठुमक कर नहीं, लेकिन वो क़त्ताला-ए-आलम क़दम आगे बढ़ाने से पहले एक दफ़ा जिस्म के दरमियानी हिस्से को घंटे के पेंडुलम की तरह दाएं-बाएं यूं हिलाती कि बस छुरी सी चल जाती।
नतीजा ये कि मुतज़क्किरा हिस्सा-ए-जिस्म ने जितनी मुसाफ़त जुनूब से शुमाल तक तय की, उतनी ही मशरिक़ से मग़रिब तक। मुख़्तसर यूं समझिए कि हर गाम पर एक क़दम आदम सलीब बनाती हुई आगे बढ़ थी।
“अच्छा, बताओ, उसकी चौमुखी चाल से क्या टपकता है?” मैंने पूछा।
“उसकी चाल से तो बस उसका चाल-चलन टपके है।” मुझे आँख-मार कर लहकते हुए बोले।
“फिर वही बात, चाल से बताओ कैसी किताबें पढ़ती है?” मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा।
“पगले, ये तो ख़ुद एक किताब है!” उन्होंने शहादत की उंगली से सड़क पर उन ख़्वांदगान की तरफ़ इशारा किया जो एक फ़र्लांग से उसके पीछे पीछे फे़हरिस्त-ए- मज़मीन का मुताला करते चले आरहे थे।
देखा गया है कि वही कुतुबफ़रोश कामयाब होते हैं जो किताब के नाम और क़ीमत के इलावा और कुछ जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनकी नावाक़फ़ियत-ए- आम्मा जिस क़दर वसीअ होगी, जिस क़दर अमीक़ और मुतनव्वे होगी, उतनी ही भरपूर ख़ुद-एतिमादी और मासूम गुमराही के साथ वो बुरी किताब को अच्छा कर के बेच सकेंगे। इसके बरअकस किताबें पढ़ते पढ़ते(अधूरी ही सही) हमारे हीरो को इस्लामी नाविलों के जोशीले मकालमे हिफ़्ज़ हो गए थे और बग़दादी जिमख़ाने में कभी वैसी व्हिस्की की ज़्यादती से मौसूफ़ पर हिज़यानी कैफ़ियत तारी हो जाती तो दुश्मनान-ए-इस्लाम पर घूँसे तान तान कर तड़ाक पड़ाक ऐसे डायलॉग बोलते, जिनसे शौक़-ए-शहादत इस तरह टपका पड़ता था कि पैरों तक ईमान ताज़ा हो जाता।
मुसलसल वर्क़ गरदानी के सबब नई-नवेली किताबें अपनी कुँवारी करारी महक और जिल्द की कसावट खो चुकी थीं। बेशतर सफ़हात के कोने कुत्ते के कानों की तरह मुड़ गए थे और बाज़ पसंदीदा औराक़ की ये कैफ़ियत थी कि
जाना जाता है कि इस राह से लश्कर गुज़रा और लश्कर भी वो जो ख़ून की बजाय पीक की छींटें उड़ाता हुआ गुज़र जाये।
एक मर्तबा उनको भरे दुकान में अपने ही साइज़ के एक इस्लामी नॉवेल का इतर निकालते देखा तो मिर्ज़ा ने टोका, “लोग अगर किसी हलवाई को मिठाई चखते देख लें तो उससे मिठाई ख़रीदनी छोड़ देते हैं और एक तुम हो कि हर आए गए के सामने कुतुब चशी करते रहते हो!”
फिर क्या था, पहले ही भरे बैठे थे, फट पड़े, “कुतुबफ़रोशी एक इल्म है, बरख़ुरदार, हमारे हाँ नीम जाहिल किताबें लिख सकते हैं, मगर बेचने के लिए बाख़बर होना ज़रूरी है। बईना उसी तरह जैसे एक अंधा सुर्मा बना सकता है मगर बीच बाज़ार में खड़े हो कर बेच नहीं सकता।
मियां, तुम क्या जानो! कैसे कैसे जय्यद जाहिल से पाला पड़ता है (अपनी अज़ीज़ तरीन किताब की जानिब इशारा करते हुए) जी में आती है, दीवान-ए-ग़ालिब (मअ मुक़द्दमा मौलाना इमतियाज़ अली अर्शी) उनके सर पर दे मारूं।
तुम्हें यक़ीन नहीं आएगा। दो हफ़्ते होने को आए, एक मज़लूम सूरत क्लर्क यहां आया और मुझे उस कोने में ले जा कर कुछ शरमाते-लजाते हुए कहने लगा कि कृश्न चंदर एम.ए की वो किताब चाहिए, जिसमें “तेरे माँ के दूध में हुक्म का इक्का” वाली गाली है।
ख़ैर, उसे जाने दो कि उस बेचारे को देखकर वाक़ई महसूस होता था कि ये गाली सामने रखकर ही उस की सूरत बनाई गई है। मगर उन साहिब को क्या कहोगे जो नए नए उर्दू के लेक्चरर मुक़र्रर हुए हैं। मेरे वाक़िफ़ कार हैं। इसी महीने की पहली तारीख़ को कॉलेज में पहली तनख़्वाह वसूल कर के सीधे यहां आए और फूली हुई साँसों के साथ लगे पूछने, साहिब, आपके हाँ मंटो की वो किताब भी है जिसमें “धरन तख़्ता” के मानी हों?
और अभी परसों का ज़िक्र है, एक मुहतरमा तशरीफ़ लाईं, सिन यही अठारह- उन्नीस का, निकलता हुआ फ़र्बा बदन। अपनी गुड़िया की चोली पहने हुए थीं। दोनों हथेलियों की रेहल बना कर उस पर अपनी किताबी चेहरा रखा और लगीं किताबों को टुकुर टुकुर देखने। इसी जगह जहां तुम खड़े हो। फिर दरयाफ़्त किया, कोई नॉवेल है?
मैंने रातों की नींद हराम करने वाला एक नॉवेल पेश किया। रेहल पर से बोलीं, ये नहीं कोई ऐसा दिलचस्प नॉवेल दीजिए कि रात को पढ़ते ही नींद आजाए।
मैंने एक ऐसा ही ग़शी आवर नॉवेल निकाल कर दिया, मगर वो भी नहीं जचा। दर असल उन्हें किसी गहरे सब्ज़ गर्द पोश वाली किताब की तलाश थी, जो उनकी ख़्वाबगाह के सुर्ख़ पर्दों से “मैच” हो जाये। उस सख़्त मेयार पर सिर्फ़ एक किताब पूरी उतरी, वो थी “उस्ताद मोटर ड्राइवरी” (मंजूम) जिसको दर असल उर्दू ज़बान में ख़ुदकुशी की आसान तरकीबों का पहला मंजूम हिदायतनामा कहना चाहिए।
मैंने नौख़ेज़ ख़ातून की हिमायत की, “हमारे हाँ उर्दू में ऐसी किताबें बहुत कम हैं जो बग़ैर गर्द पोश के भी अच्छी लगें, गर्द पोश तो ऐसा ही है जैसे औरत के लिए कपड़े।”
“मगर हालीवुड में आजकल ज़्यादातर एक्ट्रेसें ऐसी हैं जो अगर कपड़े पहन लें तो ज़रा भी अच्छी न लगें।” मिर्ज़ा ने बात को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया।
लेकिन नया नया शौक़ था और अभी ये नौबत नहीं आई थी कि ऐसे वाक़ियात से उनकी तबीयत सचमुच मुकद्दर हो जाये। डेल कार्नेगी के मश्वरे के मुताबिक़ वो हर वक़्त मुस्कुराते रहते और हमने सोते में भी उनकी बाछें बतौर ख़ैर सगाली खुली हुई देखीं। उस ज़माने में बक़ौल मिर्ज़ा वो छोटा देखते न बड़ा हर कस-ओ-नाकस के साथ डेल कार्नेगी किया करते थे।
हद ये कि डाकिया अगर बैरंग ख़त भी लाता तो इनाम-ओ-इकराम देकर रुख़सत करते। ग्राहकों को तो ज़ाती मेहमान समझ कर बिछ बिछ जाते और अक्सर मता-ए-सुख़न के साथ (और कभी उसके बग़ैर ही) ख़ुद भी बिक जाते।
सच है ख़ुश ख़लक़ी कभी रायगां नहीं जाती, चुनांचे चंद ही दिनों में दुकान चल निकली, मगर दुकानदारी ठप हो गई। ये सूरत-ए-तज़ाद इस तरह पैदा हुई कि दुकान पर अब उन क़दरदानों की रेल-पेल रहने लगी जो असल में उनसे कोका-कोला पीने या फ़ोन करने आते और रोकन में एक-आध किताब आरियतन लेकर टलते।
जिस गाहक से ख़ुसूसियत बरतते, उसकी पेशवाई को बेतहाशा दौड़ते हुए सड़क के उस पार जाते। फिर उसे अपने ऊंचे से स्टूल पर बिठा कर फ़ौरन दूसरे गाहक को चालीस क़दम तक रुख़सत करने चले जाते। हर दो रसूम की पुर तकल्लुफ़ अदायगी के दौरान दुकान किसी एक गाहक या गिरोह की इज्तिमाई तहवील में रहती। नतीजा? किताबों की क़तारों में जा-ब-जा खांचे पड़ गए। जैसे दाँत टूट गए हों।
उनके अपने बयान के मुताबिक़ एक नए गाहक को(जिसने अभी अभी “ग़ुबार-ए-ख़ातिर” का एक नुस्ख़ा उधार ख़रीदा था।) पास वाले रेस्तोराँ में मुसन्निफ़ की मन भाती चीनी चाय पिलाने ले गए। हलफ़िया कहते कि मुश्किल से एक घंटा वहां बैठा हूँगा, मगर वापस आकर देखा तो नूर-उल-लुग़ात की चौथी जिल्द की जगह ख़ाली थी। ज़ाहिर है कि किसी बेईमान ने मौक़ा पाते ही हाथ साफ़ कर दिया। उन्हें उसकी जगह फ़साना-ए-आज़ाद की चौथी जिल्द रखना पड़ी और आख़िर को यही सेट चाकसू कॉलेज लाइब्रेरी को बज़रिया वी.पी किया।
चोरियां बढ़ती देखकर एक बुजु़र्गवार ने जो यौम-ए-इफ़्तिताह से दुकान पर उठते बैठते थे (बल्कि ये कहना चाहिए कि सिर्फ़ बैठते थे, इसलिए हमने उनको कभी उठते नहीं देखा) माल की नाजायज़ ‘निकासी’ रोकने के लिए ये तजवीज़ पेश की कि एक तालीम-याफ़्ता मगर ईमानदार मैनेजर रख लिया जाये।
हर-चंद कि उनका रू-ए-सुख़न अपनी ही तरफ़ था, लेकिन एक दूसरे साहिब ने (जो ख़ैर से साहब-ए-दीवान थे और रोज़ाना अपने दीवान की बिक्री का हाल पूछने आते और उर्दू के मुस्तक़बिल से मायूस हो कर लौटते थे।) ख़ुद को इस असामी के लिए पेश ही नहीं कि बल्कि शाम को अपने घर वापस जाने से भी इनकार कर दिया।
यही साहिब दूसरे दिन से ख़ज़ानची जी कहलाए जाने लगे। सूरत से सज़ायाफ़्ता मालूम होते थे और अगर वाक़ई सज़ायाफ़्ता नहीं थे तो ये पुलिस की ऐन भलमंसाहट थी।
बहरहाल यहां उनकी ज़ात से ख़ियानत-ए-मुजरिमाना का कोई ख़दशा न था, क्योंकि दुकान की सारी बिक्री मुद्दतों से उधार पर हो रही थी। यूं तो दुकान में पहले ही दिन से “आज नक़द कल उधार” की एक छोड़ तीन तीन तख़्तियाँ लगी थीं मगर हम देखते चले आए थे कि वो कल का काम आज ही कर डालने के क़ाइल हैं।
फिर ये कि क़र्ज़ पर किताबें बेचने पर ही इकतिफ़ा करते तो सब्र आ जाता। लेकिन आख़िर आख़िर में यहां तक सुनने में आया कि बा’ज़ गाहक उनसे नक़द रुपये क़र्ज़ लेकर पास वाली दुकान से किताबें ख़रीदने लगे हैं।
मैं मौक़े की तलाश में था, लिहाज़ा एक दिन तख़लिया पा कर उन्हें समझाया कि बंदा-ए-ख़ुदा अगर क़र्ज़ ही देना है तो बड़ी रक़म क़र्ज़ दो ताकि लेने वाले को याद रहे और तुम्हें तक़ाज़ा करने में शर्म न आए। ये छोटे छोटे कर्जे़ देकर ख़ल्क़-ए-ख़ुदा के ईमान और अपने अख़लाक़ की आज़माईश काहे को करते हो?
मेरी बात उनके दिल को लगी। दूसरे ही दिन ख़ज़ानची जी से नादेहंद ख़रीदारों की मुकम्मल फ़ेहरिस्त हरूफ़-ए-तहज्जी के एतबार से मुरत्तब कराई और फिर ख़ुद उसी तर्तीब से उधार वसूल करने का पंच रोज़ा मन्सूबा बना डाला, लेकिन अलिफ ही की रदीफ़ में एक ऐसा ना हंजार आन पड़ा कि छः महीने तक ‘बे’ से शुरू होने वाले नामों की बारी ही नहीं आई।
मैंने ये नक़्शा देखा तो फिर समझाया कि जब ये हज़रात तुम्हारे पास हरूफ़-ए-तहज्जी की तर्तीब से क़र्ज़ लेने आए तो तुम इस तर्तीब से वसूल करने पर क्यों अड़े हुए हो? सीधी सी बात थी मगर वो मंतिक़ पर उतर आए। कहने लगे, अगर दूसरे बेउसूल हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बेउसूला हो जाऊं। देखते नहीं, स्कूल में हाज़िरी के वक़्त बच्चों के नाम हरूफ़-ए-तहज्जी की तर्तीब से पुकारे जाते हैं। मगर बच्चों को इसी तर्तीब से पैदा या पास होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, बोलते क्यों नहीं?
इसके बावजूद मेरी नसीहत का इतना असर ज़रूर हुआ कि अब किताब उधार नहीं बेचते थे ‘तोहफ़तन’ दे दिया करते थे। कहते थे जब रक़म डूबनी ही है तो फिर सवाब से भी क्यों महरूम रहूं? इधर कुछ अर्से से उन्होंने बही खाते लिखना भी छोड़ दिया था। जिसका ये माक़ूल जवाज़ पेश करते कि मैं नुक़्सान माया में जान के ज़ियाँ का इज़ाफ़ा नहीं करना चाहता।
मिर्ज़ा ने ये लुट्टस मचती देखी तो एक दिन पूछा, “आजकल तुम हुकूमत के फ़राइज़ क्यों अंजाम दे रहे हो?”
“क्या मतलब?”
“तुमने क़ौम की मुफ़्त तालीम का ज़िम्मा क्यों ले रखा है?”
अब उनके चेहरे पर दानाई की वो छूट पड़ने लगी जो उमूमन दिवाला निकलने के बाद तुलूअ होती है।
मिर्ज़ा का ख़्याल है कि जब तक दो-तीन दफ़ा दिवाला न निकले आदमी को दुकानदारी का सलीक़ा नहीं आता, चुनांचे इस मुबारक बर्बादी के बाद वो बुझ से गए और हर शय में अपनी कमी महसूस करने लगे।
वो दाइमी (Built-in) मुस्कुराहट भी ग़ायब हो गई और अब वो भूल कर किसी गाहक से सीधे मुँह बात नहीं करते थे, मबादा वो उधार मांग बैठे। अक्सर देखा कि जूं ही गाहक ने दुकान में क़दम रखा और उन्होंने घुड़क कर पूछा, “क्या चाहिए?”
एक दिन मैंने दड़ बढ़ाया, “अंधे को भी नज़र आता है कि किताबों की दुकान है, फिर तुम क्यों पूछते हो, क्या चाहिए? क्या चाहिए?”
फ़रमाया, “क्या करूँ, बाज़े बाज़े की सूरत ऐसी होती है कि ये पूछना पड़ता है।”
किताबें रखने के गुनाहगार ज़रूर थे, तौअन व करहन बेच भी लेते थे।
लेकिन अय्यार तबा ख़रीदार देखकर
उनके नक चढ़ेपन का अंदाज़ा इस वाक़े से हो सकता है कि एक दफ़ा एक शख़्स पूछता हुआ आया, “लुग्त है?”
“लुग़त का तलफ़्फ़ुज़ उसने ‘लुत्फ़’ के वज़न पर किया। उन्होंने नथुने फुला कर जवाब दिया, “स्टाक में नहीं है।”
वो चला गया तो मैंने कहा, “ये सामने रखी तो है, तुमने इनकार क्यूँ कर दिया?” कहने लगे, “ये लुग़त है। फिर ये भी कि उस बेचारे का काम एक लुग़त से थोड़ा ही चलेगा।”
हाँ तलफ़्फ़ुज़ पर याद आया कि इस दौर-ए-इब्तेला में उन्होंने दुकान में अज़कार-ए- रफ़्ता रेडियो रख लिया था। उसी को गोद में लिए घंटों गड़ गड़ाहट सुना करते थे, जिसे वो मुख़्तलिफ़ मुल्कों के मौसम का हाल कहा करते थे। बाद में मिर्ज़ा की ज़बानी ग़ायत-ए-समा ख़राशी ये मालूम हुई कि उस रेडियाई दमे की बदौलत कम अज़ कम ग्राहकों की ग़लत उर्दू तो सुनाई नहीं देती।
ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि कुतुब फ़रोशों को हर किताब पर औसतन तीस चालीस फ़ीसद कमीशन मिलता है। बिला कद्द-ओ-काविश। जिस पेशे में मुनाफ़े की ये शरह आम हो, उसमें दिवाला निकालने के लिए ग़ैरमामूली दिल-ओ-दिमाग़ दरकार हैं। और वो ऐसे ही दिल-ओ-दिमाग़ के मालिक निकलते अपनी हिसाबी सलाहियतों का दस्तावेज़ी सबूत वो उस ज़माने ही में दे चुके थे जब सह माही इम्तिहान की कापी में वो अपना नाम शेख़ सिब्ग़तुल्लाह लिखते और ग़ैर सरकारी तौर पर महज़ सिबग़े कहलाते थे।
उसी ज़माने से वो अपने इस अक़ीदे पर सख़्ती से क़ायम हैं कि इल्म-उल-हिसाब दर-हक़ीक़त किसी मुतअस्सिब काफ़िर ने मुसलमानों को आज़ार पहुंचाने के लिए ईजाद किया था। चुनांचे एक दिन ये ख़बर सुनकर बड़ी हैरत हुई कि रात उन पर इल्म-उल-हिसाब ही के किसी क़ाएदे की रू से ये मुनकशिफ़ हुआ है कि अगर वो किताबें न बेचें (दुकान ही में पड़ी सड़ने दें) तो नव्वे फ़ीसद मुनाफ़ा होगा।
मुनाफ़े की ये अंधाधुंद शरह सुनकर मिर्ज़ा के भी मुँह में पानी भर आया। लिहाज़ा नज़दीक तरीन गली से सिबग़े के पास वो गुर मालूम करने पहुंचे, जिसकी मदद से वो भी अपनी पुराने कोटों की दुकान में ताला ठोक कर फ़िलफ़ौर अपने दलिद्दर दूर करलें।
सिबग़े ने कान में लगी हुई पेंसिल की मदद से अपने फॉमूले की जो तशरीह की उसका लुब्ब-ए-लुबाब सलीस उर्दू में ये है कि अब तक उनका ये मामूल रहा कि जिस दिन नई किताबें ख़रीद कर दुकान में लगाते, उसी दिन उन पर मिलने वाले चालीस फ़ीसद मुनाफ़े का हिसाब (क़रीब तरीन पाई तक) लगा कर ख़र्च कर डालते।
लेकिन जब ये किताबें साल भर तक दुकान में पड़ी भिनकती रहतीं तो ‘क्रिस्मस सेल’ में इन गंज हाय गिरांमाया को पच्चास फ़ीसद रिआयत पर फ़रोख़्त कर डालते और इस तरह अपने हिसाब की रू से हर किताब पर नव्वे फ़ीसद नाजायज़ नुक़्सान उठाते। लेकिन नया फ़ार्मूला दरयाफ़्त होने के बाद अब वो किताबें यकसर फ़रोख़्त ही नहीं करेंगे, लिहाज़ा अपनी इस हिक्मत-ए-बेअमली से नव्वे फ़ीसद नुक़्सान से साफ़ बच जाऐंगे और ये मुनाफ़ा नहीं तो और क्या है?
कुतुबफ़रोशी के आख़री दौर में जब उन पर पयंबरी वक़्त पड़ा तो हर एक गाहक को अपना माली दुश्मन तसव्वुर करते और दुकान से उसके ख़ाली हाथ जाने को अपने हक़ में बाइस-ए-ख़ैर-ओ-बरकत गरदानते। हफ़्ते को मेरा दफ़्तर एक बजे बंद हो जाता है। वापसी में यूँ ही ख़्याल आया कि चलो आज सिबग़े की दुकान में झाँकता चलूं।
देखा कि वो ऊंचे स्टूल पर पैर लटकाए अपने क़र्ज़दारों की फ़ेहरिस्तों से टेक लगाए सो रहे हैं। मैंने खंकार कर कहा, “क़ैलूला...?”
“स्टाक में नहीं है!” आँखें बंद किए किए बोले।
ये कह कर ज़रा गर्दन उठाई। चिन्धयाई हुई आँखों से अपनी दाहिनी हथेली देखी और फिर सो गए।
दाहिनी हथेली देखना उनकी पुरानी आदत है, जिसे ज़माना-ए-तालिब इल्मी की याद गार कहना चाहिए। होता ये था कि दिन-भर ख़ार-ओ-ख़स्ता होने के बाद वो रात को होस्टल में ही न किसी के सर हो जाते कि सुबह तुम्हारा मुँह देखा था। चुनांचे उनके कमरे के साथी अपनी बदनामी के ख़ौफ़ से सुबह दस बजे तक लिहाफ़ ओढ़े पड़े रहते और कछुवे की तरह गर्दन निकाल निकाल कर देखते रहते कि सिबग़े दफ़ान हुए या नहीं।
जब अपने बेगाने सब आए दिन की नहूसतों की ज़िम्मेदारी लेने से यूं मुँह छुपाने लगे तो सिबग़े ने एक हिंदू नजूमी के मश्वरे से ये आदत डाली कि सुबह आँख खुलते ही शगुन के लिए अपनी दाएं हथेली देखते और दिन-भर अपने आप पर लानत भेजते रहते।
फिर तो ये आदत सी हो गई कि नाज़ुक-ओ-फ़ैसलाकुन लमहात में मसलन अख़बार में अपना रोल नंबर तलाश करते वक़्त, ताश फेंटने के बाद और क्रिकेट की गेंद पर हिट लगाने से पहले, एक दफ़ा अपनी दाहिनी हथेली ज़रूर देख लेते थे। जिस ज़माने का ये ज़िक्र है, उन दिनों उनको अपनी हथेली में एक हसीना साफ़ नज़र आ रही थी जिसका जहेज़ बमुश्किल उनकी हथेली में समा सकता था।
अलमारियों के अनगिनत ख़ाने जो कभी ठसाठस भरे रहते थे, अब ख़ाली हो चुके थे,जैसे किसी ने भुट्टे के दाने निकाल लिए हों। मगर सिबग़े हाथ पर हाथ धर कर बैठने वाले नहीं थे, चुनांचे अक्सर देखा कि ज़ुहर से अस्र तक शीशे के शो केस की फ़र्ज़ी ओट में अपने ख़लेरे-चचेरे भाईयों के साथ सर जोड़े फ्लश खेलते रहते।
उनका ख़्याल था कि जो अगर क़रीबी रिश्तेदारों के साथ खेला जाये तो कम गुनाह होता है। रही दुकानदारी तो वो इन हॉलों को पहुंच गई थी कि ताश के पत्तों के सिवा अब दुकान में काग़ज़ की कोई चीज़ नहीं बची थी। ग्राहकों की तादाद अगरचे तिगुनी चौगुनी हो गई, मगर मोल-तोल की नौईयत क़दरे मुख़्तलिफ़ होते होते जब ये नौबत आ गई कि राह चलने वाले भी भाव-ताव करने लगे तो ख़ज़ानची जी ने ख़ाकी गत्ते पर एक नोटिस निहायत पाकीज़ा ख़त में आवेज़ां कर दिया, “ये फ़र्नीचर की दुकान नहीं है।”
याद रहे कि उनकी निस्फ़ ज़िंदगी उन लोगों ने तल्ख़ कर दी जो क़र्ज़ पर किताबें ले जाते थे और बक़ीया निस्फ़ ज़िंदगी उन हज़रात ने तल्ख़ कर रखी थी जिनसे वो ख़ुद क़र्ज़ लिए बैठे थे।
इस में शुबहा नहीं कि उनकी तबाही में कुछ शाइबा ख़ूबी-ए-तक़दीर भी था। क़ुदरत ने उनके हाथ में कुछ ऐसा जस दिया था कि सोने के हाथ लगाऐं तो मिट्टी हो जाये लेकिन इन्साफ़ से देखा जाये तो उनकी बर्बादी का सेहरा क़ुदरत के इलावा उन मेहरबानों के सर था जो इंतहाई ख़ुलूस और मुस्तक़िल मिज़ाजी के साथ दामे, दरमे, क़दमे, सुख़ने उनको नुक़्सान पहुंचाते रहे।
दूसरी वजह जैसा कि ऊपर इशारा कर चुका हूँ ये थी कि वो अपने ख़ास दोस्तों से अपनी हाजत और उनकी हैसियत के मुताबिक़ क़र्ज़ा लेते हैं और कर्जे़ को मुनाफ़ा समझ कर खा गए। बक़ौल मिर्ज़ा उनका दिल बड़ा था और क़र्ज़ लेने में उन्होंने कभी बुख़ल से काम नहीं लिया।
क़र्ज़ लेन-देन उनके मिज़ाज में इस हद तक रच बस चुका था कि मिर्ज़ा का ख़्याल था कि सिबग़े दरअसल सुह्रवर्दी हुकूमत को खुख करने की ग़रज़ से अपनी आमदनी नहीं बढ़ाते। इसलिए कि आमदनी बढ़ेगी तो ला-मुहाला इन्कम टैक्स भी बढ़ेगा। अब तो उनकी ये तमन्ना है कि बक़ीया उम्र-ए-अज़ीज़ ‘बंक ओवर ड्राफ़्ट’ पर गोशा-ए-बदनामी में गुज़ार दें लेकिन उनकी नीयत बुरी नहीं थी। ये और बात है कि हालात ने उनकी नेक नीयती को उभरने न दिया।
गुज़िश्ता रमज़ान में मुलाक़ात हुई तो बहुत उदास और फ़िक्रमंद पाया। बार-बार पतलून की जेब से यद-ए-बैज़ा निकाल कर देख रहे थे। पूछा सिबग़े क्या बात है? बोले, कुछ नहीं। प्रोफ़ेसर अबदुल क़ुद्दूस से क़र्ज़ लिए तेरह साल होने को आए। आज यूंही बैठे-बैठे ख़्याल आया कि अब वापसी की सबील करनी चाहिए वर्ना वो भी दिल में सोचेंगे कि शायद में ना देहंद हूँ।
जवानी में ख़ुदा के क़ाइल नहीं थे, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ईमान पुख़्ता होता गया। यहां तक कि अब वो अपनी तमाम नालायक़ियों को सच्चे दिल से मिन जानिब अल्लाह समझने लगे थे। तबीयत ही ऐसी पाई थी कि जब तक छोटी से छोटी बात पर बड़ी से बड़ी क़ुर्बानी न दे देते, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। बक़ौल मिर्ज़ा, वो अनल-हक़ कहे बग़ैर सूली पर चढ़ना चाहते थे। तिजारत को उन्होंने वसीला-ए-मआश नहीं हुल्या-ए-जिहाद समझा और बहुत जल्द शहादत का दर्जा पाया।
दुकान की दीवार का प्लास्टर एक जगह से उखड़ गया था। उस मुक़ाम पर (जो तक़रीबन दो मुरब्बा गज़ था।) उन्होंने एक सुर्ख़ तख़्ती जिस पर उनका फ़लसफ़ा-ए हयात ब ख़ते नस्तालीक़ कुंदा था, टांग दी।
बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं
इसमें क़तई कोई तअल्ली नहीं थी, बल्कि देखा जाये तो उन्होंने कसर-ए-नफ़सी ही से काम लिया क्योंकि बातिल तो बातिल, वो हक़ से भी दबने वाले नहीं थे मिर्ज़ा अक्सर नसीहत करते कि मियां कामयाबी चाहते हो तो कामयाब कुतुब फ़रोशों की तरह बक़दर-ए-ज़रूरत सच बोलो और हर किताब के हुस्न-ओ-क़ुबह पर ज़िद्दम ज़िद्दा करने के बजाय ग्राहकों को उन्ही की पसंद की किताबों से बर्बाद होने दो जो बेचारा तरबूज़ से बहल जाये उसे ज़बरदस्ती अंगूर क्यों खिलाते हो? लेकिन सिबग़े का कहना था कि बीसवीं सदी में जीत उन्ही की है जिनके एक हाथ में दीन है और दूसरे में दुनिया।
और दाएं हाथ को ख़बर नहीं कि बाएं में क्या है, तिजारत और नजात में संजोग मुम्किन नहीं। तिजारत में फ़ौरी नाकामी उनके नज़दीक मिक़्यास-उल-शराफ़त थी। उन्ही का मक़ूला है कि अगर कोई शख़्स तिजारत में बहुत जल्द नाकाम न हो सके तो समझ लो कि उसके हसब नसब में फ़ी है। इस एतबार से उन्होंने क़दम क़दम पर बल्कि हर सौदे में अपनी नसबी शराफ़त का वाफ़र सबूत दिया।
हस्सास आदमी थे। उस पर बदकिस्मती ये कि एक नाकाम कुतुबफ़रोश की हैसियत से उन्हें इंसानों की फ़ित्रत का बहुत क़रीब से मुताला करने का मौक़ा मिला। इसीलिए बहुत जल्द इंसानियत से मायूस हो गए। उन्होंने तमाम उम्र तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें उठाईं। शायद इसी वजह से उन्हें यक़ीन हो चला था कि वो हक़ पर हैं। ज़िंदगी से कब के बेज़ार हो चुके थे और उनकी बातों से ऐसा लगता था कि गोया अब महज़ अपने क़र्ज़-ख़्वाहों की तालीफ़-ए-क़लूब के लिए जी रहे हैं। अब हम जैल में वो तास्सुरात-ओ-तअस्सुबात मुख़्तसिरन बयान करते हैं जो उनकी चालीस साला नातजुर्बाकारी का निचोड़ हैं।
दुकान खोलने से चार-पाँच महीने पहले एक अदबी ख़ैर सगाली वफ़द (इदारा बराए तरक़्क़ी अंजुमन पसंद मुसन्निफ़ीन) के साथ सीलोन हो आए थे जिसे हासिद लंका के नाम से याद करते थे। उस जज़ीरे की सह रोज़ा सयाहत के बाद उठते-बैठते “तरक़्क़ी याफ़्ता ममालिक” की अदब नवाज़ी व इल्म दोस्ती के चर्चे रहने लगे।
एक दफ़ा बिरादरान-ए-वतन की नाकद़री का गिला करते हुए फ़रमाया, “आपके हाँ तो अभी तक जहालत की ख़राबियां दूर करने पर किताबें लिखी जा रही हैं मगर तरक़्क़ी याफ़्ता ममालिक में तो अब मारा मार ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं, जिनका मक़सद उन ख़राबियों को दूर करना है जो महज़ जहालत दूर होने से पैदा हो गई हैं। साहिब वहां इल्म की ऐसी क़दर है कि किताब लिखना, किताब छापना, किताब बेचना, किताब ख़रीदना, हद ये कि किताब चुराना भी सवाब में दाख़िल है। यक़ीन मानिए तरक़्क़ी याफ़्ता ममालिक में तो जाहिल आदमी ठीक से जुर्म भी नहीं कर सकता।”
शामत-ए-आमाल मेरे मुँह से निकल गया, “ये सब कहने की बातें हैं। तरक़्क़ी याफ़्ता ममालिक में कोई किताब उस वक़्त तक अच्छी ख़्याल नहीं की जाती जब तक कि उसकी फ़िल्म न बन जाये और फ़िल्म बनने के बाद किताब पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।”
उन्हें ग़ुस्सा आगया, ‘तीन पैसे की छोकरी” का कोना मोड़ कर वापस अलमारी में रखी और मेरे लब-ओ-लहजे की हू-ब-हू नक़ल उतारते हुए बोले, “और आपके हाँ ये कैफ़ियत है कि नौजवान उस वक़्त तक उर्दू की कोई किताब पढ़ने की हाजत महसूस नहीं करते, जब तक पुलिस उसे फ़ुहश क़रार न दे दे और फ़ुहश क़रार पाने के बाद उसके बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता।”
उनके तंज़ में ताने का रंग आ चला था, इसलिए मैंने झट से हामी भर ली कि पुलिस अगर दिल से चाहे तो तमाम अच्छी अच्छी किताबों को फ़ुहश क़रार देकर नौजवानों में उर्दू अदब से गहरे दिलचस्पी पैदा कर सकती है।
मेरे लहजे का नोटिस लेते हुए उल्टे मुझी से उलझने लगे कि आप बात की तह तक नहीं पहुंचे। आप धड़ा धड़ किताबें छाप सकते हैं। मगर ज़बरदस्ती पढ़वा नहीं सकते।
मैंने कहा, क्यों नहीं? उठा के निसाब में दाख़िल कर दीजिए।
वो भला हार मानने वाले थे। कहने लगे अगर ये पूरी की पूरी नस्ल को हमेशा के लिए किसी अच्छी किताब से बेज़ार करना हो तो सीधी तरकीब ये है कि उसे निसाब में दाख़िल कर दीजिए।
कुतुबफ़रोशी की बदौलत सिबग़े का साबिक़ा ऐसे ऐसे पढ़ने और ना पढ़ने वालों से पड़ा,
हज़ारों साल नर्गिस जिनकी बेनूरी पे रोती है
उनमें ख़य्याम के वो दिलदादा भी शामिल थे जो असल रुबाइयों में तर्जुमे की खूबियां तलाश करते फिरते थे। उनमें वो साल ख़ूर्दा किताबख़्वाँ भी थे जो कजलाए हुए कोयलों को दहकाने के लिए बक़ौल मिर्ज़ा उरियां नाविलों से मुँह काला करते और समझते कि हम उर्दू की इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं। (ये क़ौल उन ही का है कि फ़ुहश किताब में दीमक नहीं लग सकती क्योंकि दीमक ऐसा काग़ज़ खा कर अफ़्ज़ाइश-ए-नस्ल के क़ाबिल नहीं रहती।) उनमें वो ख़ुशनसीब भी थे जिनके लिए किताब बेहतरीन रफ़ीक़ है और वो कम नसीब भी जिनके लिए वाहिद रफ़ीक़।
और उस बेनाम क़बीले में वो जिद्दत पसंद पढ़ने वाले भी शामिल थे जो लहज़ा ताज़ा बह ताज़ा, नौ ब नौ के तलबगार थे। हालाँकि उन जैसों को मालूम होना चाहिए कि फ़क़त डिक्शनरी ही एक ऐसी किताब है जिसे वो जब भी देखें, इंशाअल्लाह नई मालूम होगी। लेकिन एक हद तक सिबग़े की भी ज़्यादती थी कि नई उर्दू किताबों को अपने दिल और दुकान में जगह देना तो बड़ी बात है, चिमटे से पकड़ कर भी बेचने के लिए तैयार न थे।
एक दिन ख़ाक़ानी-ए-हिंद उस्ताद ज़ौक़ के क़साइद की गर्द हफ़्तावार टाइम से झाड़ते हुए गट गटा कर कहने लगे कि आजकल लोग ये चाहते हैं कि अदब एक “कैप्सूल” मैं बंद करके उनके हवाले कर दिया जाये, जिसे वो कोका-कोला के घूँट के साथ गटक से हलक़ से उतार लें। इंसानी तहज़ीब पत्थर और भोजपत्र के अह्द से गुज़र कर अब रीडर्स डाइजेस्ट के दौर तक आगई है। समझे? ये मुसन्निफ़ों का दौर नहीं, सहाफ़ियों का दौर है सहाफ़ियों का।
मैंने डरते डरते पूछा, “मगर सहाफ़त में क्या क़बाहत है?”
बोले, “कुछ नहीं। बड़ा मुसन्निफ़ अपनी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाता है, मगर बड़ा सहाफ़ी पब्लिक की आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाता है!”
मुसन्निफ़ों का ज़िक्र छिड़ गया तो एक वारदात और सुनते चलिए। सात-आठ महीने तक वो उर्दू अफ़सानों का एक मजमूआ बेचते रहे, जिसके सर वर्क़ पर मुसन्निफ़ के दस्तख़त बक़लम ख़ुद सब्त थे और ऊपर ये इबारत, “जिस किताब पर मुसन्निफ़ के दस्तख़त न हों वो जाली तसव्वुर की जाये।”
एक रोज़ उन्हें रजिस्ट्री से मुसन्निफ़ के वकील की मार्फ़त नोटिस मिला कि हमें मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि आप हमारे मुवक्किल की किताब का एक मुसद्दिक़ा एडिशन अर्सा आठ माह से मुबय्यना तौर पर फ़रोख़्त कर रहे हैं, जिस पर मुसन्निफ़ मज़कूर के दस्तख़त बक़ैद तारीख़ सब्त हैं। आपको बज़रिये नोटिस हज़ा मुतला-ओ-मुतनब्बा किया जाता है कि महूला बाला किताब और दस्तख़त दोनों जाली हैं।
असल एडिशन में मुसन्निफ़ के दस्तख़त सिरे से हैं ही नहीं। इस वाक़ए से उन्होंने ऐसी इबरत पकड़ी कि आइन्दा कोई ऐसी किताब दुकान में नहीं रखी, जिस पर किसी के भी दस्तख़त हों बल्कि जहां तक बन पड़ता, उन्ही किताबों को तर्जीह देते जिन पर मुसन्निफ़ का नाम तक दर्ज नहीं होता, मसलन! अलिफ़ लैला, ज़ाबता फ़ौजदारी, रेलवे टाइम टेबल, इंजील।
तबाही के जो तबाज़ाद राह बल्कि शाहराह उन्होंने अपने लिए निकाली, उस पर वो तो क्या, क़ारून भी ज़्यादा देर गामज़न नहीं रह सकता था, क्योंकि मंज़िल बहुत दूर नहीं थी। आख़िर वो दिन आही गया, जिसका दुश्मनों को इंतज़ार था और दोस्तों को अंदेशा, दुकान बंद हो गई।
ख़ज़ानची जी की तनख़्वाह ढाई महीने से चढ़ी हुई थी। लिहाज़ा ख़ाली अलमारियां, एक अदद गोलक चोबी जो ना देहंदों की फ़ेहरिस्तों से मुँह तक भरी थी। चांदी का ख़ूबसूरत सिगरेट केस, जिसे खोलते ही महसूस होता था, गोया बीड़ी का बंडल खुल गया। नसीनी जिसकी सिर्फ़ ऊपर की तीन सीढ़ियां बाक़ी रह गई थीं, ख़्वाब-आवर गोलियों की शीशी, कराची रेस में दौड़ने वाले घोड़ों के शिजरा हाय नसब, नवंबर से दिसंबर तक का मुकम्मल कलेंडर कील समेत।
ये सब ख़ज़ानची जी ने सिबग़े की अव्वलीन ग़फ़लत में हथिया लिये और रातों रात अपनी तनख़्वाह की एक एक पाई गधा गाड़ी में ढो ढो कर ले गए।
दूसरे दिन दुकान का मालिक बक़ाया किराए की मद में जो जायदाद मनक़ूला व ग़ैर मनक़ूला उठा कर या उखाड़ कर ले गया, उसकी तफ़सील की यहां न गुंजाइश है न ज़रूरत।
हमारे पढ़ने वालों को बस इतना इशारा काफ़ी होगा कि उनमें सबसे क़ीमती चीज़ बग़ैर चाबी के बंद होने वाला एक क़ुफ़ुल फ़ौलादी साख़्ता जर्मनी था। पुराना ज़रूर था मगर एक ख़ूबी उसमें ऐसी पैदा हो गई थी जो हमने नए से नए जर्मन तालों में भी नहीं देखी। यानी बग़ैर चाबी के बंद होना और इसी तरह खुलना!
सिबग़े ग़रीब के हिस्से में सिर्फ़ अपने नाम (मअ फ़र्ज़ी फ़रज़ंदान) का साइनबोर्ड आया, जिसको सात रुपये मज़दूरी देकर घर उठवा लाए और दूसरे दिन सवा रुपये में महल्ले के कबाड़ी के हाथ फ़रोख़्त कर डाला। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दो महीने तक अपनी हथेली का शबाना रोज़ मुताला करने के बाद एक ट्रेनिंग कॉलेज में स्कूल मास्टरों को पढ़ाना शुरू कर दिया।
मिर्ज़ा के अलफ़ाज़ में सिबग़े की कुतुबफ़रोशान ज़िंदगी के बाब का अंजाम निहायत अफ़सानवी रहा। जिस अफ़साने की तरफ़ यहां मिर्ज़ा का इशारा है, वो दर असल काईलिंग की एक मशहूर चीनी कहानी है, जिसका हीरो एक आर्टिस्ट है। एक दिन वो अपनी एक मॉडल लड़की की ख़ूबसूरती से इस क़दर मुतास्सिर हुआ कि उसी वक़्त अपने सारे ब्रश और कैनवस समेट समाट कर जला डाले और एक सर्कस में हाथियों को सधाने का काम करने लगा।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.
